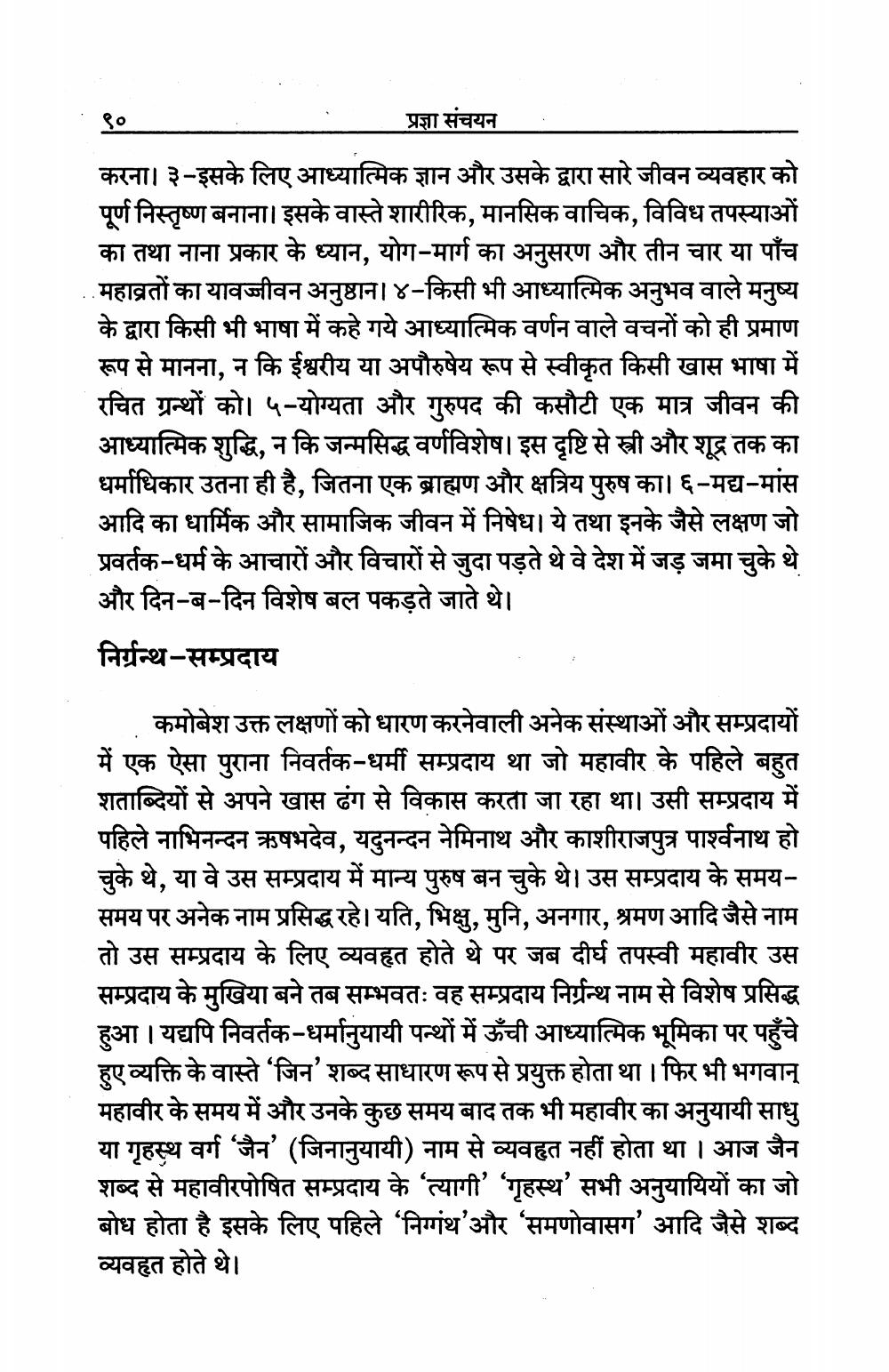________________
प्रज्ञा संचयन
करना। ३-इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और उसके द्वारा सारे जीवन व्यवहार को पूर्ण निस्तृष्ण बनाना। इसके वास्ते शारीरिक, मानसिक वाचिक, विविध तपस्याओं
का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग-मार्ग का अनुसरण और तीन चार या पाँच ..महाव्रतों का यावज्जीवन अनुष्ठान। ४-किसी भी आध्यात्मिक अनुभव वाले मनुष्य
के द्वारा किसी भी भाषा में कहे गये आध्यात्मिक वर्णन वाले वचनों को ही प्रमाण रूप से मानना, न कि ईश्वरीय या अपौरुषेय रूप से स्वीकृत किसी खास भाषा में रचित ग्रन्थों को। ५-योग्यता और गुरुपद की कसौटी एक मात्र जीवन की
आध्यात्मिक शुद्धि, न कि जन्मसिद्ध वर्णविशेष। इस दृष्टि से स्त्री और शूद्र तक का धर्माधिकार उतना ही है, जितना एक ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुष का। ६-मद्य-मांस आदि का धार्मिक और सामाजिक जीवन में निषेध। ये तथा इनके जैसे लक्षण जो प्रवर्तक-धर्म के आचारों और विचारों से जुदा पड़ते थे वे देश में जड़ जमा चुके थे
और दिन-ब-दिन विशेष बल पकड़ते जाते थे। निर्ग्रन्थ-सम्प्रदाय
कमोबेश उक्त लक्षणों को धारण करनेवाली अनेक संस्थाओं और सम्प्रदायों में एक ऐसा पुराना निवर्तक-धर्मी सम्प्रदाय था जो महावीर के पहिले बहुत शताब्दियों से अपने खास ढंग से विकास करता जा रहा था। उसी सम्प्रदाय में पहिले नाभिनन्दन ऋषभदेव, यदुनन्दन नेमिनाथ और काशीराजपुत्र पार्श्वनाथ हो चुके थे, या वे उस सम्प्रदाय में मान्य पुरुष बन चुके थे। उस सम्प्रदाय के समयसमय पर अनेक नाम प्रसिद्ध रहे। यति, भिक्षु, मुनि, अनगार, श्रमण आदि जैसे नाम तो उस सम्प्रदाय के लिए व्यवहृत होते थे पर जब दीर्घ तपस्वी महावीर उस सम्प्रदाय के मुखिया बने तब सम्भवतः वह सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि निवर्तक-धर्मानुयायी पन्थों में ऊँची आध्यात्मिक भूमिका पर पहुंचे हुए व्यक्ति के वास्ते 'जिन' शब्द साधारण रूप से प्रयुक्त होता था। फिर भी भगवान् महावीर के समय में और उनके कुछ समय बाद तक भी महावीर का अनुयायी साधु या गृहस्थ वर्ग 'जैन' (जिनानुयायी) नाम से व्यवहृत नहीं होता था । आज जैन शब्द से महावीरपोषित सम्प्रदाय के 'त्यागी' 'गृहस्थ' सभी अनुयायियों का जो बोध होता है इसके लिए पहिले 'निग्गंथ'और 'समणोवासग' आदि जैसे शब्द व्यवहृत होते थे।