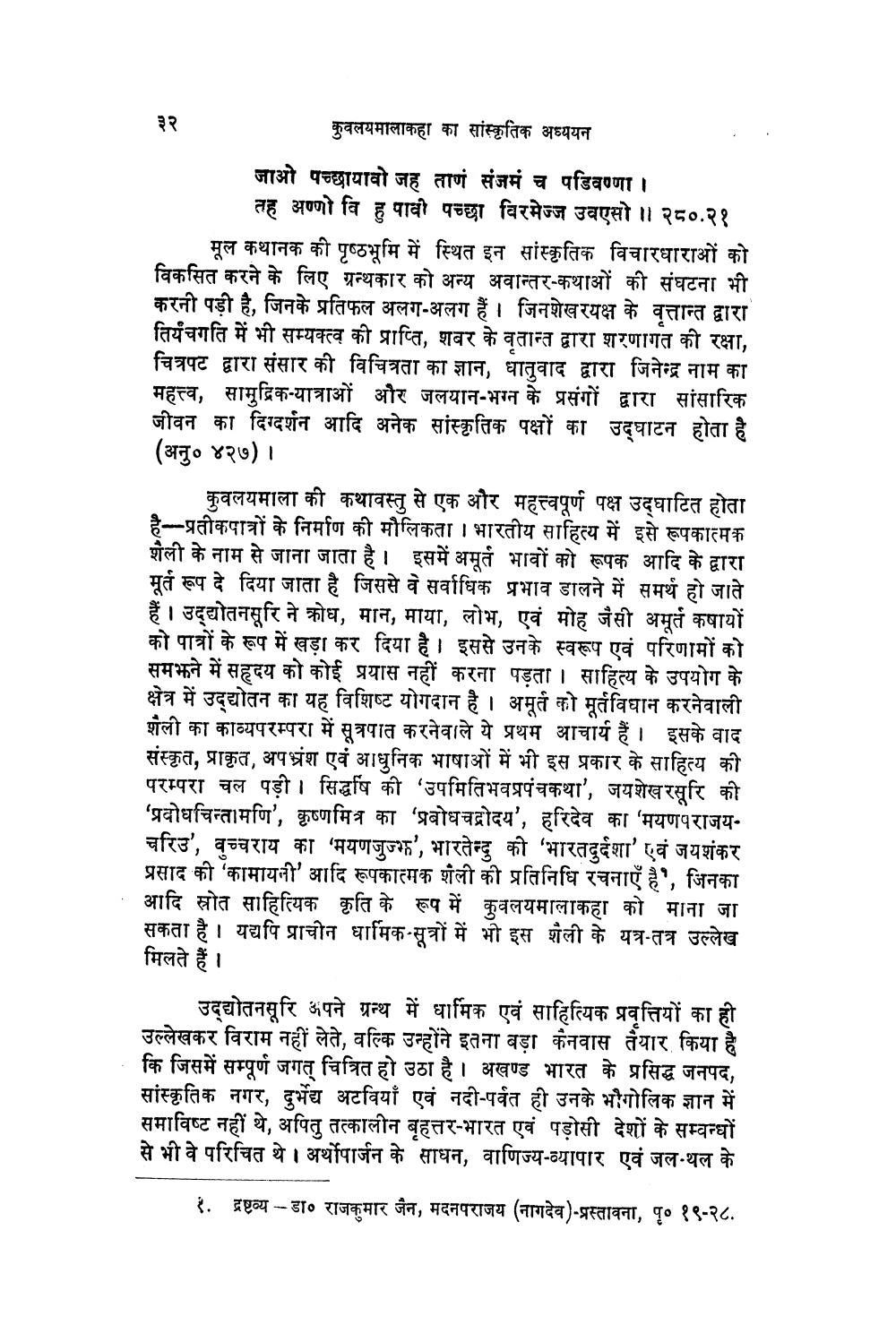________________
३२
कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन
जाओ पच्छायावो जह ताणं संजमं च पडिवण्णा । तह अण्णो वि हु पावी पच्छा विरमेज्ज उवएसो ॥। २८०.२१
मूल कथानक की पृष्ठभूमि में स्थित इन सांस्कृतिक विचारधाराओं को विकसित करने के लिए ग्रन्थकार को अन्य अवान्तर - कथाओं की संघटना भी करनी पड़ी है, जिनके प्रतिफल अलग-अलग हैं । जिनशेखरयक्ष के वृत्तान्त द्वारा तियंचगति में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति, शवर के वृतान्त द्वारा शरणागत की रक्षा, चित्रपट द्वारा संसार की विचित्रता का ज्ञान, धातुवाद द्वारा जिनेन्द्र नाम का महत्त्व, सामुद्रिक यात्राओं और जलयान - भग्न के प्रसंगों द्वारा सांसारिक जीवन का दिग्दर्शन आदि अनेक सांस्कृतिक पक्षों का उद्घाटन होता है ( अनु० ४२७ ) ।
कुवलयमाला की कथावस्तु से एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष उद्घाटित होता है -- प्रतीकपात्रों के निर्माण की मौलिकता । भारतीय साहित्य में इसे रूपकात्मक शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें अमूर्त भावों को रूपक आदि के द्वारा मूर्त रूप दे दिया जाता है जिससे वे सर्वाधिक प्रभाव डालने में समर्थ हो जाते हैं | उद्योतनसूरि ने क्रोध, मान, माया, लोभ, एवं मोह जैसी अमूर्त कषायों को पात्रों के रूप में खड़ा कर दिया है। इससे उनके स्वरूप एवं परिणामों को समझने में सहृदय को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । साहित्य के उपयोग के क्षेत्र में उद्योतन का यह विशिष्ट योगदान है । अमूर्त को मूर्तविधान करनेवाली शैली का काव्यपरम्परा में सूत्रपात करनेवाले ये प्रथम आचार्य हैं । इसके वाद संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाओं में भी इस प्रकार के साहित्य की परम्परा चल पड़ी । सिद्धर्षि की 'उपमितिभवप्रपंचकथा', जयशेखरसूरि की 'प्रबोधचिन्तामणि', कृष्णमित्र का 'प्रबोधचद्रोदय', हरिदेव का 'मयणपराजयचरिउ', वुच्चराय का 'मयणजुज्भ', भारतेन्दु की 'भारतदुर्दशा' एवं जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' आदि रूपकात्मक शैली की प्रतिनिधि रचनाएँ है', जिनका आदि स्रोत साहित्यिक कृति के रूप में कुवलयमालाकहा को माना जा सकता है । यद्यपि प्राचीन धार्मिक सूत्रों में भी इस शैली के यत्र-तत्र उल्लेख मिलते हैं ।
उद्योतनसूरि अपने ग्रन्थ में धार्मिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों का ही उल्लेखकर विराम नहीं लेते, वल्कि उन्होंने इतना बड़ा कैनवास तैयार किया है कि जिसमें सम्पूर्ण जगत् चित्रित हो उठा है । अखण्ड भारत के प्रसिद्ध जनपद, सांस्कृतिक नगर, दुर्भेद्य अटवियाँ एवं नदी- पर्वत ही उनके भौगोलिक ज्ञान में समाविष्ट नहीं थे, अपितु तत्कालीन बृहत्तर भारत एवं पड़ोसी देशों के सम्वन्धों से भी वे परिचित थे । अर्थोपार्जन के साधन, वाणिज्य व्यापार एवं जल-थल के
१. द्रष्टव्य - डा० राजकुमार जैन, मदनपराजय (नागदेव ) - प्रस्तावना, पृ० १९-२८.