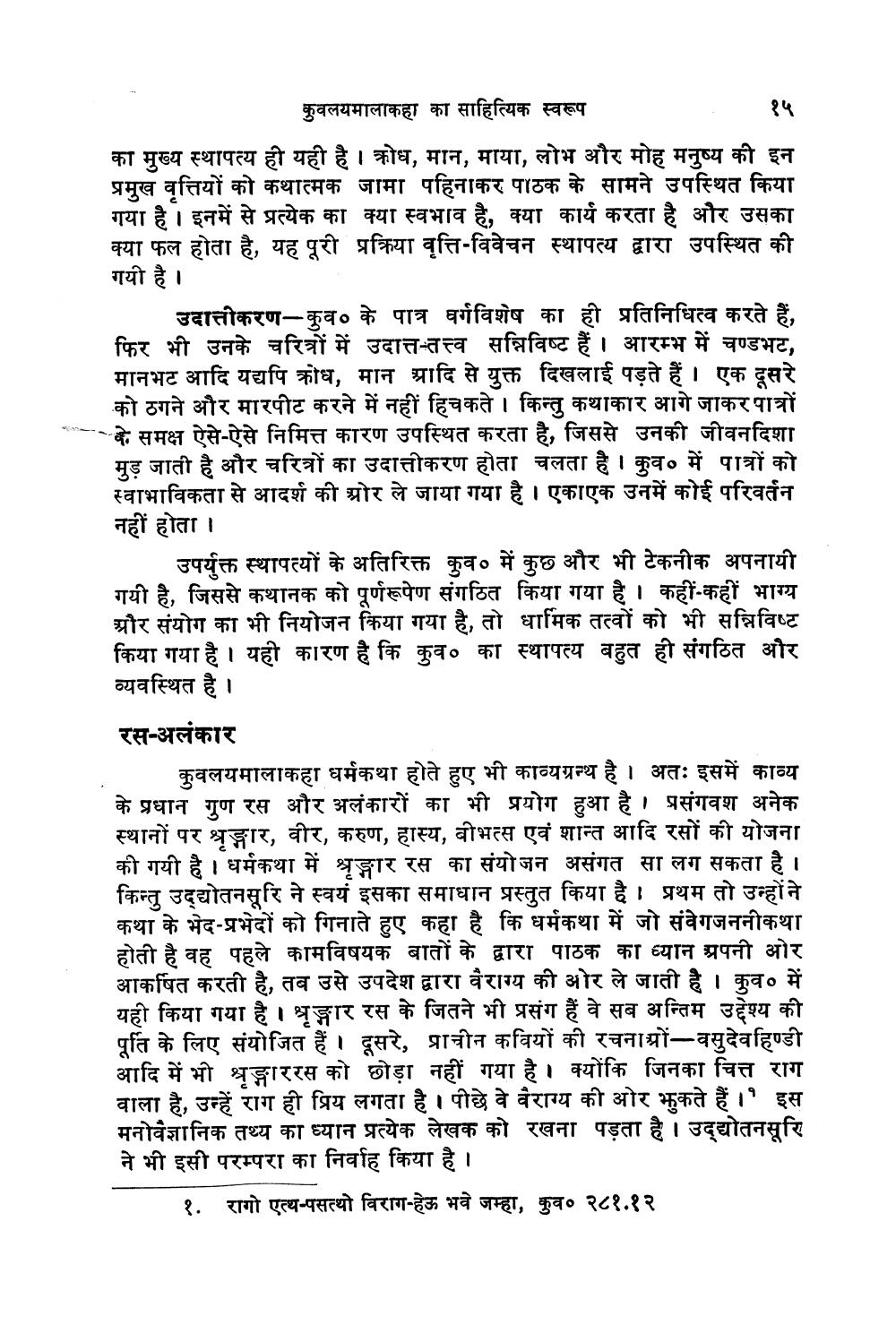________________
कुवलयमालाकहा का साहित्यिक स्वरूप
१५
का मुख्य स्थापत्य ही यही है । क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह मनुष्य की इन प्रमुख वृत्तियों को कथात्मक जामा पहिनाकर पाठक के सामने उपस्थित किया गया है । इनमें से प्रत्येक का क्या स्वभाव है, क्या कार्य करता है और उसका क्या फल होता है, यह पूरी प्रक्रिया वृत्ति-विवेचन स्थापत्य द्वारा उपस्थित की गयी है।
उदात्तीकरण-कुव० के पात्र घर्गविशेष का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनके चरित्रों में उदात्त-तत्त्व सन्निविष्ट हैं। आरम्भ में चण्डभट, मानभट आदि यद्यपि क्रोध, मान आदि से युक्त दिखलाई पड़ते हैं। एक दूसरे को ठगने और मारपीट करने में नहीं हिचकते। किन्तु कथाकार आगे जाकर पात्रों के समक्ष ऐसे-ऐसे निमित्त कारण उपस्थित करता है, जिससे उनकी जीवनदिशा मुड़ जाती है और चरित्रों का उदात्तीकरण होता चलता है । कुव० में पात्रों को स्वाभाविकता से आदर्श की ओर ले जाया गया है । एकाएक उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
उपर्युक्त स्थापत्यों के अतिरिक्त कुव० में कुछ और भी टेकनीक अपनायी गयी है, जिससे कथानक को पूर्णरूपेण संगठित किया गया है। कहीं-कहीं भाग्य
और संयोग का भी नियोजन किया गया है, तो धार्मिक तत्वों को भी सन्निविष्ट किया गया है । यही कारण है कि कुव० का स्थापत्य बहुत ही संगठित और व्यवस्थित है। रस-अलंकार
कुवलयमालाकहा धर्मकथा होते हुए भी काव्यग्रन्थ है। अतः इसमें काव्य के प्रधान गुण रस और अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। प्रसंगवश अनेक स्थानों पर श्रृङ्गार, वीर, करुण, हास्य, वीभत्स एवं शान्त आदि रसों की योजना की गयी है। धर्मकथा में श्रृङ्गार रस का संयोजन असंगत सा लग सकता है। किन्तु उद्योतनसूरि ने स्वयं इसका समाधान प्रस्तुत किया है। प्रथम तो उन्होंने कथा के भेद-प्रभेदों को गिनाते हुए कहा है कि धर्मकथा में जो संवेगजननीकथा होती है वह पहले कामविषयक बातों के द्वारा पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, तब उसे उपदेश द्वारा वैराग्य की ओर ले जाती है । कुव० में यही किया गया है। श्रृङ्गार रस के जितने भी प्रसंग हैं वे सब अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयोजित हैं। दूसरे, प्राचीन कवियों की रचनाओं-वसुदेवहिण्डी आदि में भी श्रृङ्गाररस को छोड़ा नहीं गया है। क्योंकि जिनका चित्त राग वाला है, उन्हें राग ही प्रिय लगता है। पीछे वे वैराग्य की ओर झुकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का ध्यान प्रत्येक लेखक को रखना पड़ता है । उद्द्योतनसूरि ने भी इसी परम्परा का निर्वाह किया है।
१. रागो एत्थ-पसत्थो विराग-हेऊ भवे जम्हा, कुव० २८१.१२