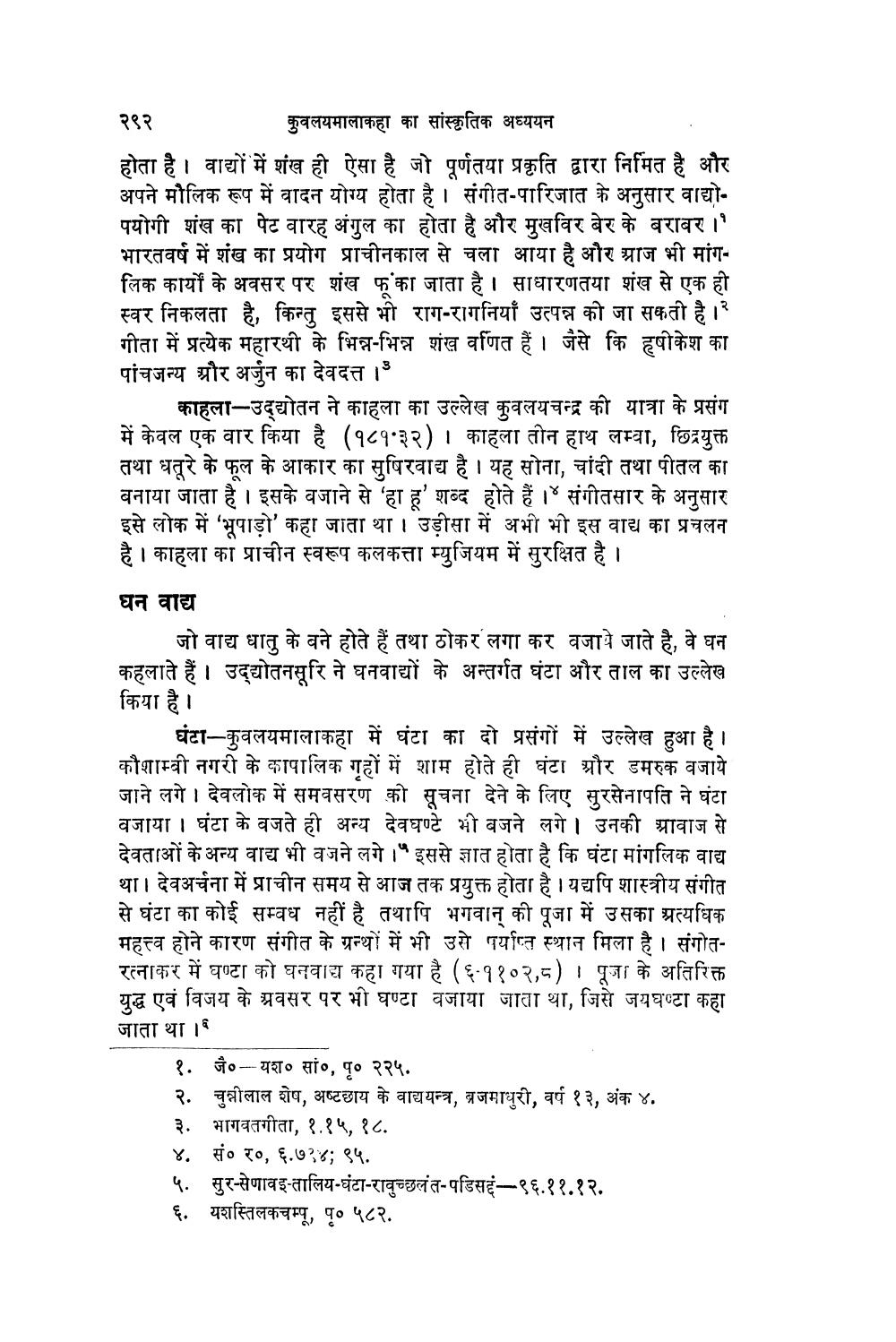________________
२९२
कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन होता है। वाद्यों में शंख ही ऐसा है जो पूर्णतया प्रकृति द्वारा निर्मित है और अपने मौलिक रूप में वादन योग्य होता है। संगीत-पारिजात के अनुसार वाद्योपयोगी शंख का पेट वारह अंगुल का होता है और मुखविर बेर के बराबर ।' भारतवर्ष में शंख का प्रयोग प्राचीनकाल से चला आया है और आज भी मांगलिक कार्यों के अवसर पर शंख फूका जाता है। साधारणतया शंख से एक ही स्वर निकलता है, किन्तु इससे भी राग-रागनियाँ उत्पन्न की जा सकती है। गीता में प्रत्येक महारथी के भिन्न-भिन्न शंख वणित हैं। जैसे कि हृषीकेश का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त ।।
___ काहला-उद्योतन ने काहला का उल्लेख कुवलयचन्द्र की यात्रा के प्रसंग में केवल एक वार किया है (१८१.३२) । काहला तीन हाथ लम्बा, छिद्रयुक्त तथा धतूरे के फूल के आकार का सुषिरवाद्य है । यह सोना, चांदी तथा पीतल का बनाया जाता है । इसके बजाने से 'हा हूँ' शब्द होते हैं। संगीतसार के अनुसार इसे लोक में 'भूपाड़ो' कहा जाता था। उड़ीसा में अभी भी इस वाद्य का प्रचलन है। काहला का प्राचीन स्वरूप कलकत्ता म्युजियम में सुरक्षित है।
घन वाद्य
जो वाद्य धातु के बने होते हैं तथा ठोकर लगा कर वजाये जाते है, वे धन कहलाते हैं। उद्द्योतनसूरि ने घनवाद्यों के अन्तर्गत घंटा और ताल का उल्लेख किया है।
घंटा-कुवलयमालाकहा में घंटा का दो प्रसंगों में उल्लेख हुआ है। कौशाम्बी नगरी के कापालिक गृहों में शाम होते ही घंटा और डमरुक वजाये जाने लगे। देवलोक में समवसरण को सूचना देने के लिए सुरसेनापति ने घंटा वजाया। घंटा के बजते ही अन्य देवघण्टे भी बजने लगे। उनकी आवाज से देवताओं के अन्य वाद्य भी वजने लगे। इससे ज्ञात होता है कि घंटा मांगलिक वाद्य था। देवअर्चना में प्राचीन समय से आज तक प्रयुक्त होता है । यद्यपि शास्त्रीय संगीत से घंटा का कोई सम्बध नहीं है तथापि भगवान की पूजा में उसका अत्यधिक महत्त्व होने कारण संगीत के ग्रन्थों में भी उसे पर्याप्त स्थान मिला है। संगोतरत्नाकर में घण्टा को घनवाद्य कहा गया है (६.११०२,८) । पूजा के अतिरिक्त युद्ध एवं विजय के अवसर पर भी घण्टा बजाया जाता था, जिसे जयघण्टा कहा जाता था।
१. जै०-- यश० सां०, पृ० २२५. २. चुन्नीलाल शेष, अष्टछाय के वाद्ययन्त्र, ब्रजमाधुरी, वर्ष १३, अंक ४. ३. भागवतगीता, १.१५, १८. ४. सं० र०, ६.७९४, ९५. ५. सुर-सेणावइ-तालिय-घंटा-रावुच्छलंत-पडिसइं-९६.११.१२. ६. यशस्तिलकचम्पू, पृ० ५८२.