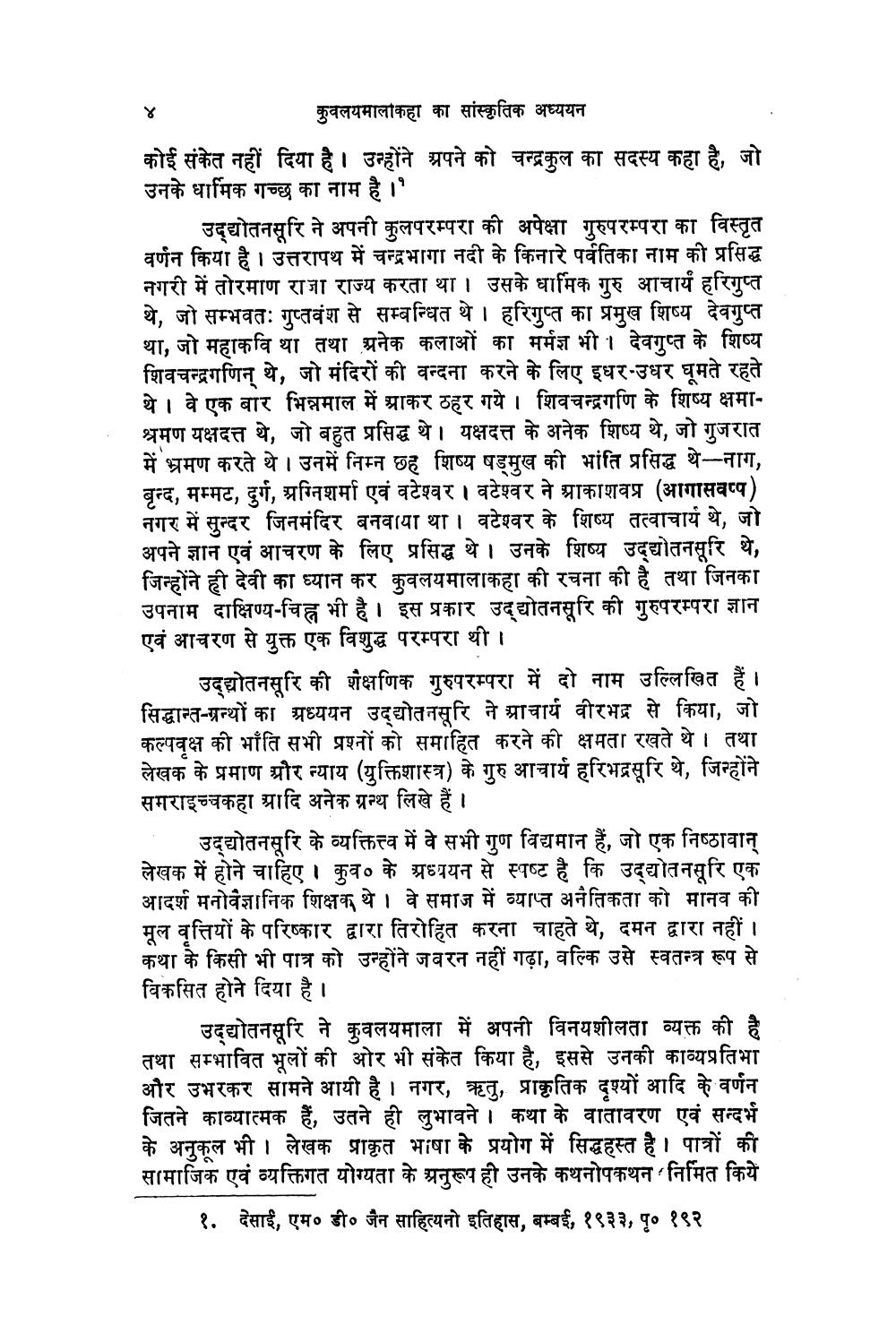________________
कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन
कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने अपने को चन्द्रकुल का सदस्य कहा है, जो उनके धार्मिक गच्छ का नाम है।'
उद्द्योतनसूरि ने अपनी कुलपरम्परा की अपेक्षा गुरुपरम्परा का विस्तृत वर्णन किया है। उत्तरापथ में चन्द्रभागा नदी के किनारे पर्वतिका नाम की प्रसिद्ध नगरी में तोरमाण राजा राज्य करता था। उसके धार्मिक गुरु आचार्य हरिगुप्त थे, जो सम्भवतः गुप्तवंश से सम्बन्धित थे। हरिगुप्त का प्रमुख शिष्य देवगुप्त था, जो महाकवि था तथा अनेक कलाओं का मर्मज्ञ भी। देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्रगणिन् थे, जो मंदिरों की वन्दना करने के लिए इधर-उधर घूमते रहते थे। वे एक बार भिन्नमाल में आकर ठहर गये । शिवचन्द्रगणि के शिष्य क्षमाश्रमण यक्षदत्त थे, जो बहुत प्रसिद्ध थे। यक्षदत्त के अनेक शिष्य थे, जो गुजरात में भ्रमण करते थे। उनमें निम्न छह शिष्य षड्मुख की भांति प्रसिद्ध थे-नाग, बृन्द, मम्मट, दुर्ग, अग्निशर्मा एवं वटेश्वर । वटेश्वर ने आकाशवप्र (आगासवप्प) नगर में सुन्दर जिनमंदिर बनवाया था। वटेश्वर के शिष्य तत्वाचार्य थे, जो अपने ज्ञान एवं आचरण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य उद्द्योतनसूरि थे, जिन्होंने ही देवी का ध्यान कर कुवलयमालाकहा की रचना की है तथा जिनका उपनाम दाक्षिण्य-चिह्न भी है। इस प्रकार उद्योतनसूरि की गुरुपरम्परा ज्ञान एवं आचरण से युक्त एक विशुद्ध परम्परा थी।
उद्योतनसूरि की शैक्षणिक गुरुपरम्परा में दो नाम उल्लिखित हैं। सिद्धान्त-ग्रन्थों का अध्ययन उद्द्योतनसूरि ने आचार्य वीरभद्र से किया, जो कल्पवृक्ष की भाँति सभी प्रश्नों को समाहित करने की क्षमता रखते थे। तथा लेखक के प्रमाण और न्याय (युक्तिशास्त्र) के गुरु आचार्य हरिभद्रसूरि थे, जिन्होंने समराइच्चकहा आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं।
उद्द्योतनसूरि के व्यक्तित्व में वे सभी गुण विद्यमान हैं, जो एक निष्ठावान् लेखक में होने चाहिए। कुव० के अध्ययन से स्पष्ट है कि उद्द्योतनसूरि एक आदर्श मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। वे समाज में व्याप्त अनैतिकता को मानव की मूल वृत्तियों के परिष्कार द्वारा तिरोहित करना चाहते थे, दमन द्वारा नहीं। कथा के किसी भी पात्र को उन्होंने जवरन नहीं गढ़ा, वल्कि उसे स्वतन्त्र रूप से विकसित होने दिया है।
उद्योतनसूरि ने कुवलयमाला में अपनी विनयशीलता व्यक्त की है तथा सम्भावित भूलों की ओर भी संकेत किया है, इससे उनकी काव्यप्रतिभा और उभरकर सामने आयी है। नगर, ऋतु, प्राकृतिक दृश्यों आदि के वर्णन जितने काव्यात्मक हैं, उतने ही लुभावने। कथा के वातावरण एवं सन्दर्भ के अनुकूल भी। लेखक प्राकृत भाषा के प्रयोग में सिद्धहस्त है। पात्रों की सामाजिक एवं व्यक्तिगत योग्यता के अनुरूप ही उनके कथनोपकथन निर्मित किये
१. देसाई, एम० डी० जैन साहित्यनो इतिहास, बम्बई, १९३३, पृ० १९२