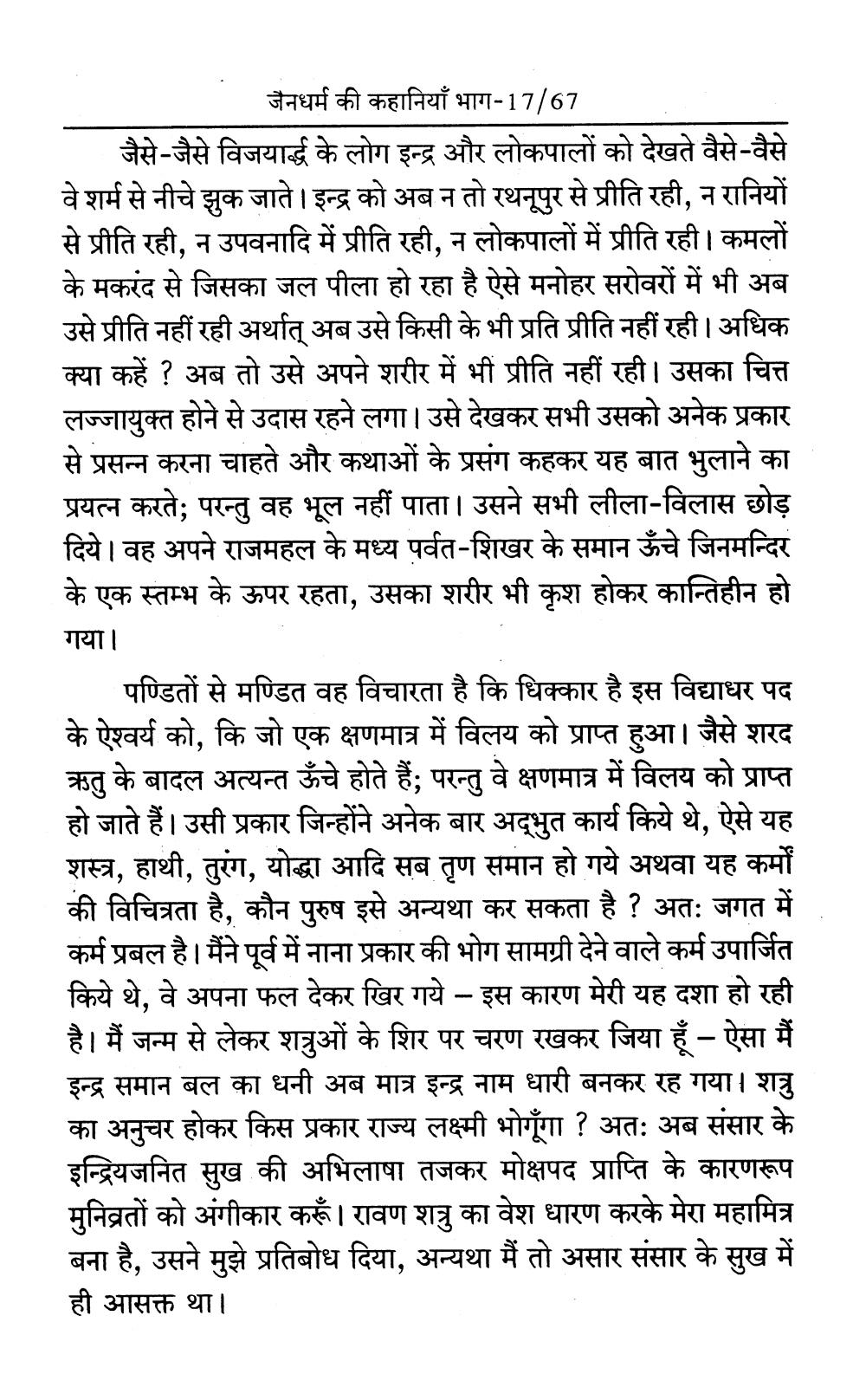________________
_जैनधर्म की कहानियाँ भाग-17/67 जैसे-जैसे विजयार्द्ध के लोग इन्द्र और लोकपालों को देखते वैसे-वैसे वे शर्म से नीचे झुक जाते। इन्द्र को अब न तो रथनूपुर से प्रीति रही, न रानियों से प्रीति रही, न उपवनादि में प्रीति रही, न लोकपालों में प्रीति रही। कमलों के मकरंद से जिसका जल पीला हो रहा है ऐसे मनोहर सरोवरों में भी अब उसे प्रीति नहीं रही अर्थात् अब उसे किसी के भी प्रति प्रीति नहीं रही। अधिक क्या कहें ? अब तो उसे अपने शरीर में भी प्रीति नहीं रही। उसका चित्त लज्जायुक्त होने से उदास रहने लगा। उसे देखकर सभी उसको अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहते और कथाओं के प्रसंग कहकर यह बात भुलाने का प्रयत्न करते; परन्तु वह भूल नहीं पाता। उसने सभी लीला-विलास छोड़ दिये। वह अपने राजमहल के मध्य पर्वत-शिखर के समान ऊँचे जिनमन्दिर के एक स्तम्भ के ऊपर रहता, उसका शरीर भी कृश होकर कान्तिहीन हो गया।
पण्डितों से मण्डित वह विचारता है कि धिक्कार है इस विद्याधर पद के ऐश्वर्य को, कि जो एक क्षणमात्र में विलय को प्राप्त हुआ। जैसे शरद ऋतु के बादल अत्यन्त ऊँचे होते हैं; परन्तु वे क्षणमात्र में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने अनेक बार अद्भुत कार्य किये थे, ऐसे यह शस्त्र, हाथी, तुरंग, योद्धा आदि सब तृण समान हो गये अथवा यह कर्मों की विचित्रता है, कौन पुरुष इसे अन्यथा कर सकता है ? अत: जगत में कर्म प्रबल है। मैंने पूर्व में नाना प्रकार की भोग सामग्री देने वाले कर्म उपार्जित किये थे, वे अपना फल देकर खिर गये – इस कारण मेरी यह दशा हो रही है। मैं जन्म से लेकर शत्रुओं के शिर पर चरण रखकर जिया हूँ – ऐसा मैं इन्द्र समान बल का धनी अब मात्र इन्द्र नाम धारी बनकर रह गया। शत्रु का अनुचर होकर किस प्रकार राज्य लक्ष्मी भोगूंगा ? अतः अब संसार के इन्द्रियजनित सुख की अभिलाषा तजकर मोक्षपद प्राप्ति के कारणरूप मुनिव्रतों को अंगीकार करूँ। रावण शत्रु का वेश धारण करके मेरा महामित्र बना है, उसने मुझे प्रतिबोध दिया, अन्यथा मैं तो असार संसार के सुख में ही आसक्त था।