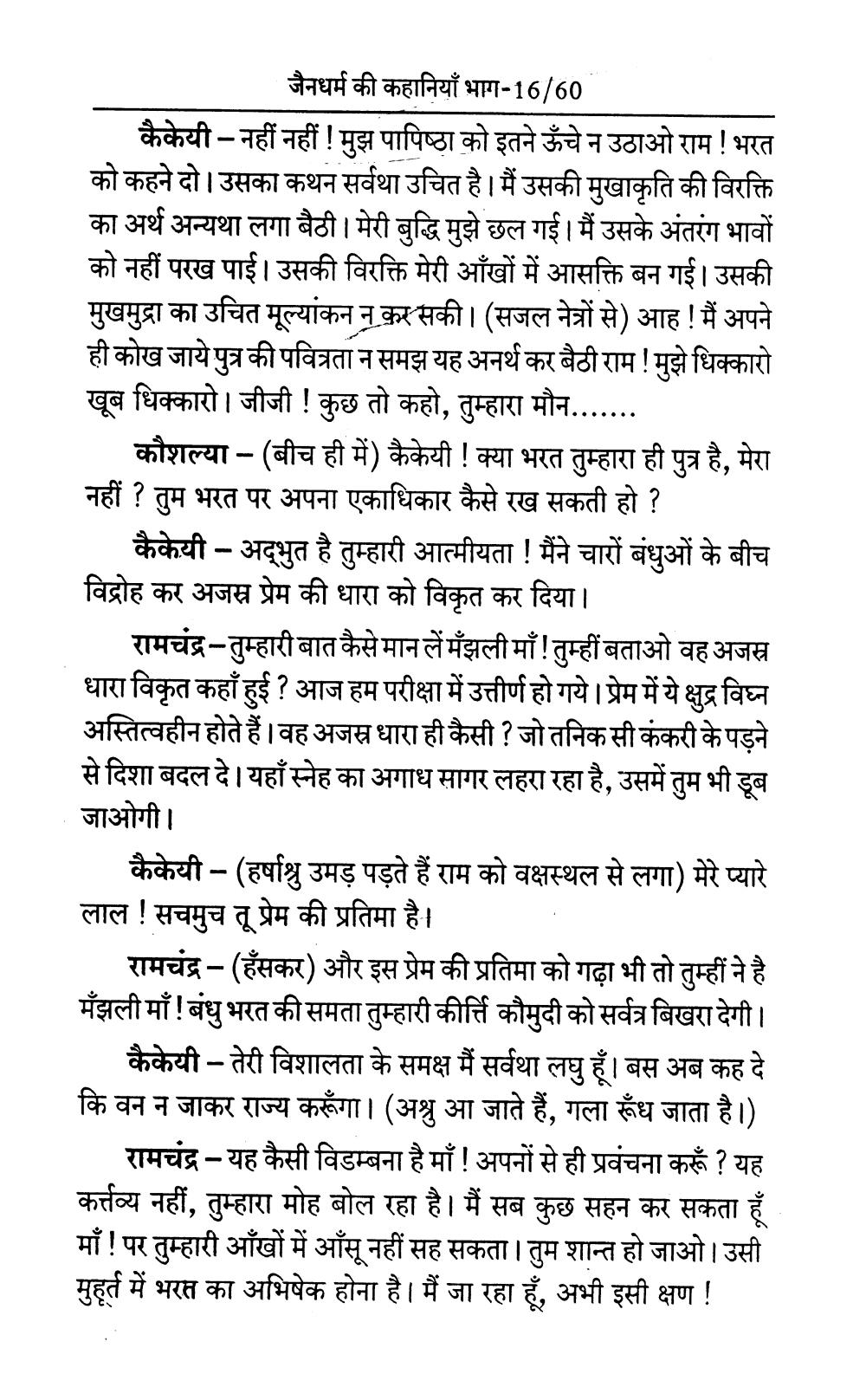________________
जैनधर्म की कहानियाँ भाग-16/60 __ कैकेयी- नहीं नहीं ! मुझ पापिष्ठा को इतने ऊँचे न उठाओ राम ! भरत को कहने दो। उसका कथन सर्वथा उचित है। मैं उसकी मुखाकृति की विरक्ति का अर्थ अन्यथा लगा बैठी। मेरी बुद्धि मुझे छल गई। मैं उसके अंतरंग भावों को नहीं परख पाई। उसकी विरक्ति मेरी आँखों में आसक्ति बन गई। उसकी मुखमुद्रा का उचित मूल्यांकन न कर सकी। (सजल नेत्रों से) आह ! मैं अपने ही कोख जाये पुत्र की पवित्रता न समझ यह अनर्थ कर बैठी राम ! मुझे धिक्कारो खूब धिक्कारो। जीजी ! कुछ तो कहो, तुम्हारा मौन.......
कौशल्या - (बीच ही में) कैकेयी ! क्या भरत तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा नहीं ? तुम भरत पर अपना एकाधिकार कैसे रख सकती हो ? ___ कैकेयी - अद्भुत है तुम्हारी आत्मीयता ! मैंने चारों बंधुओं के बीच विद्रोह कर अजस्र प्रेम की धारा को विकृत कर दिया।
रामचंद्र-तुम्हारी बात कैसे मान लें मँझली माँ! तुम्हीं बताओ वह अजस्र धारा विकृत कहाँ हुई ? आज हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये। प्रेम में ये क्षुद्र विघ्न अस्तित्वहीन होते हैं। वह अजस्र धारा ही कैसी ? जो तनिक सी कंकरी के पड़ने से दिशा बदल दे। यहाँ स्नेह का अगाध सागर लहरा रहा है, उसमें तुम भी डूब जाओगी।
कैकेयी – (हर्षाश्रु उमड़ पड़ते हैं राम को वक्षस्थल से लगा) मेरे प्यारे लाल ! सचमुच तू प्रेम की प्रतिमा है।
रामचंद्र - (हँसकर) और इस प्रेम की प्रतिमा को गढ़ा भी तो तुम्हीं ने है मँझली माँ! बंधु भरत की समता तुम्हारी कीर्ति कौमुदी को सर्वत्र बिखरा देगी।
कैकेयी- तेरी विशालता के समक्ष मैं सर्वथा लघु हूँ। बस अब कह दे कि वन न जाकर राज्य करूँगा। (अश्रु आ जाते हैं, गला रूंध जाता है।)
रामचंद्र - यह कैसी विडम्बना है माँ ! अपनों से ही प्रवंचना करूँ ? यह कर्तव्य नहीं, तुम्हारा मोह बोल रहा है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ माँ ! पर तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं सह सकता। तुम शान्त हो जाओ। उसी मुहूर्त में भरत का अभिषेक होना है। मैं जा रहा हूँ, अभी इसी क्षण !