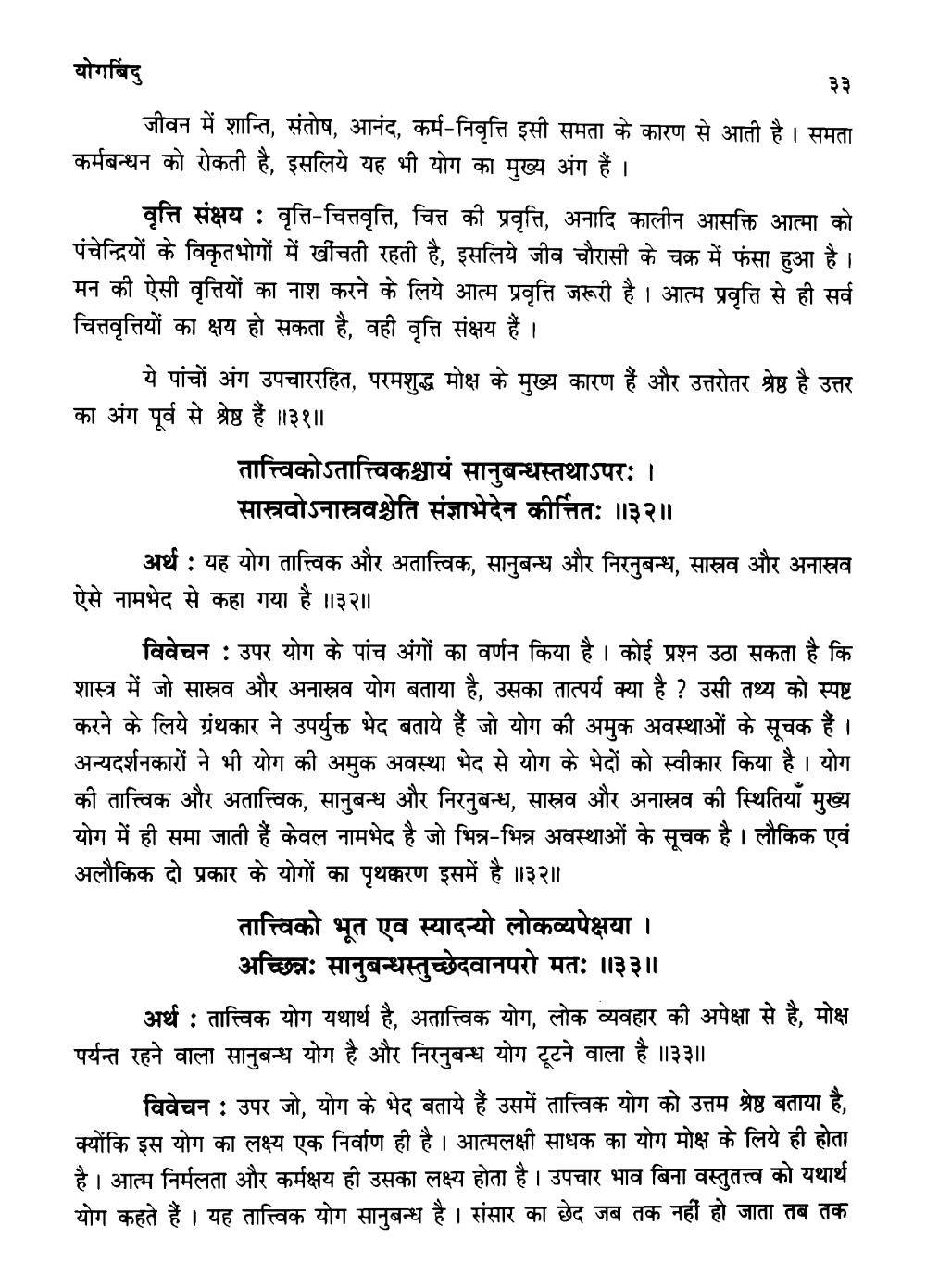________________
योगबिंदु
३३ जीवन में शान्ति, संतोष, आनंद, कर्म-निवृत्ति इसी समता के कारण से आती है । समता कर्मबन्धन को रोकती है, इसलिये यह भी योग का मुख्य अंग हैं ।
वृत्ति संक्षय : वृत्ति-चित्तवृत्ति, चित्त की प्रवृत्ति, अनादि कालीन आसक्ति आत्मा को पंचेन्द्रियों के विकृतभोगों में खींचती रहती है, इसलिये जीव चौरासी के चक्र में फंसा हुआ है। मन की ऐसी वृत्तियों का नाश करने के लिये आत्म प्रवृत्ति जरूरी है। आत्म प्रवृत्ति से ही सर्व चित्तवृत्तियों का क्षय हो सकता है, वही वृत्ति संक्षय हैं ।
ये पांचों अंग उपचाररहित, परमशुद्ध मोक्ष के मुख्य कारण हैं और उत्तरोतर श्रेष्ठ है उत्तर का अंग पूर्व से श्रेष्ठ हैं ॥३१॥
तात्त्विकोऽतात्त्विकश्चायं सानुबन्धस्तथाऽपरः ।
सास्रवोऽनास्रवश्चेति संज्ञाभेदेन कीर्तितः ॥३२॥ अर्थ : यह योग तात्त्विक और अतात्त्विक, सानुबन्ध और निरनुबन्ध, सास्रव और अनास्रव ऐसे नामभेद से कहा गया है ॥३२॥
विवेचन : उपर योग के पांच अंगों का वर्णन किया है । कोई प्रश्न उठा सकता है कि शास्त्र में जो सास्रव और अनास्रव योग बताया है, उसका तात्पर्य क्या है ? उसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिये ग्रंथकार ने उपर्युक्त भेद बताये हैं जो योग की अमुक अवस्थाओं के सूचक हैं । अन्यदर्शनकारों ने भी योग की अमुक अवस्था भेद से योग के भेदों को स्वीकार किया है । योग की तात्त्विक और अतात्त्विक, सानुबन्ध और निरनुबन्ध, सास्रव और अनास्रव की स्थितियाँ मुख्य योग में ही समा जाती हैं केवल नामभेद है जो भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के सूचक है । लौकिक एवं अलौकिक दो प्रकार के योगों का पृथक्करण इसमें है ॥३२॥
तात्त्विको भूत एव स्यादन्यो लोकव्यपेक्षया ।
अच्छिन्नः सानुबन्धस्तुच्छेदवानपरो मतः ॥३३॥ अर्थ : तात्त्विक योग यथार्थ है, अतात्त्विक योग, लोक व्यवहार की अपेक्षा से है, मोक्ष पर्यन्त रहने वाला सानुबन्ध योग है और निरनुबन्ध योग टूटने वाला है ॥३३॥
विवेचन : उपर जो, योग के भेद बताये हैं उसमें तात्त्विक योग को उत्तम श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि इस योग का लक्ष्य एक निर्वाण ही है । आत्मलक्षी साधक का योग मोक्ष के लिये ही होता है। आत्म निर्मलता और कर्मक्षय ही उसका लक्ष्य होता है । उपचार भाव बिना वस्तुतत्त्व को यथार्थ योग कहते हैं । यह तात्त्विक योग सानुबन्ध है । संसार का छेद जब तक नहीं हो जाता तब तक