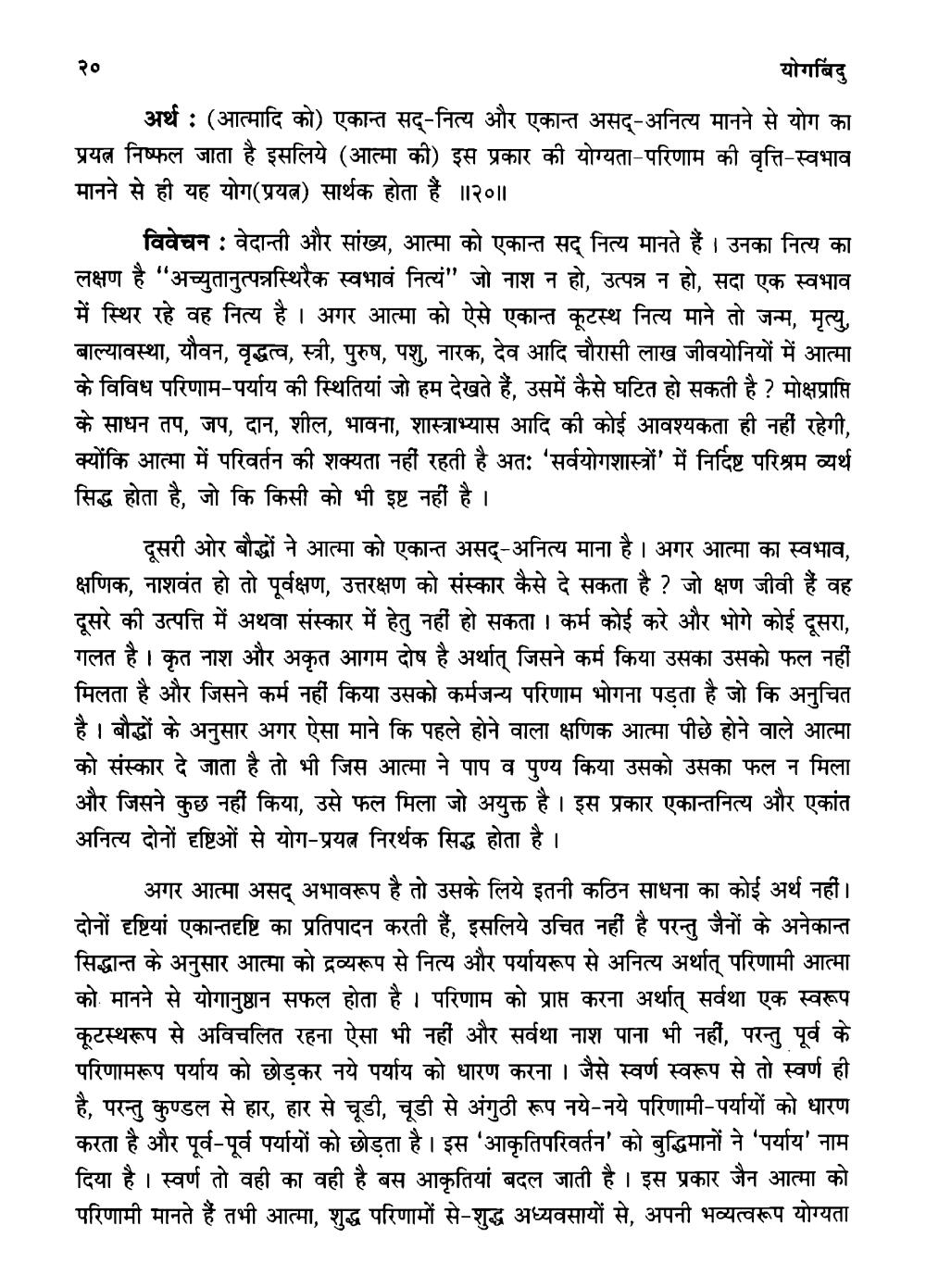________________
योगबिंदु अर्थ : (आत्मादि को) एकान्त सद्-नित्य और एकान्त असद्-अनित्य मानने से योग का प्रयत्न निष्फल जाता है इसलिये (आत्मा की) इस प्रकार की योग्यता-परिणाम की वृत्ति-स्वभाव मानने से ही यह योग(प्रयत्न) सार्थक होता हैं ॥२०॥
विवेचन : वेदान्ती और सांख्य, आत्मा को एकान्त सद् नित्य मानते हैं । उनका नित्य का लक्षण है "अच्युतानुत्पन्नस्थिरैक स्वभावं नित्यं" जो नाश न हो, उत्पन्न न हो, सदा एक स्वभाव में स्थिर रहे वह नित्य है । अगर आत्मा को ऐसे एकान्त कूटस्थ नित्य माने तो जन्म, मृत्यु, बाल्यावस्था, यौवन, वृद्धत्व, स्त्री, पुरुष, पशु, नारक, देव आदि चौरासी लाख जीवयोनियों में आत्मा के विविध परिणाम-पर्याय की स्थितियां जो हम देखते हैं, उसमें कैसे घटित हो सकती है ? मोक्षप्राप्ति के साधन तप, जप, दान, शील, भावना, शास्त्राभ्यास आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा में परिवर्तन की शक्यता नहीं रहती है अत: 'सर्वयोगशास्त्रों में निर्दिष्ट परिश्रम व्यर्थ सिद्ध होता है, जो कि किसी को भी इष्ट नहीं है।
दूसरी ओर बौद्धों ने आत्मा को एकान्त असद्-अनित्य माना है। अगर आत्मा का स्वभाव, क्षणिक, नाशवंत हो तो पूर्वक्षण, उत्तरक्षण को संस्कार कैसे दे सकता है ? जो क्षण जीवी हैं वह दूसरे की उत्पत्ति में अथवा संस्कार में हेतु नहीं हो सकता । कर्म कोई करे और भोगे कोई दूसरा, गलत है । कृत नाश और अकृत आगम दोष है अर्थात् जिसने कर्म किया उसका उसको फल नहीं मिलता है और जिसने कर्म नहीं किया उसको कर्मजन्य परिणाम भोगना पड़ता है जो कि अनुचित है । बौद्धों के अनुसार अगर ऐसा माने कि पहले होने वाला क्षणिक आत्मा पीछे होने वाले आत्मा को संस्कार दे जाता है तो भी जिस आत्मा ने पाप व पुण्य किया उसको उसका फल न मिला और जिसने कुछ नहीं किया, उसे फल मिला जो अयुक्त है। इस प्रकार एकान्तनित्य और एकांत अनित्य दोनों दृष्टिओं से योग-प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होता है ।
अगर आत्मा असद् अभावरूप है तो उसके लिये इतनी कठिन साधना का कोई अर्थ नहीं। दोनों दृष्टियां एकान्तदृष्टि का प्रतिपादन करती हैं, इसलिये उचित नहीं है परन्तु जैनों के अनेकान्त सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को द्रव्यरूप से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य अर्थात् परिणामी आत्मा को मानने से योगानुष्ठान सफल होता है । परिणाम को प्राप्त करना अर्थात् सर्वथा एक स्वरूप कूटस्थरूप से अविचलित रहना ऐसा भी नहीं और सर्वथा नाश पाना भी नहीं, परन्तु पूर्व के परिणामरूप पर्याय को छोड़कर नये पर्याय को धारण करना । जैसे स्वर्ण स्वरूप से तो स्वर्ण ही है, परन्तु कुण्डल से हार, हार से चूडी, चूडी से अंगुठी रूप नये-नये परिणामी-पर्यायों को धारण करता है और पूर्व-पूर्व पर्यायों को छोड़ता है। इस ‘आकृतिपरिवर्तन' को बुद्धिमानों ने 'पर्याय' नाम दिया है । स्वर्ण तो वही का वही है बस आकृतियां बदल जाती है । इस प्रकार जैन आत्मा को परिणामी मानते हैं तभी आत्मा, शुद्ध परिणामों से-शुद्ध अध्यवसायों से, अपनी भव्यत्वरूप योग्यता