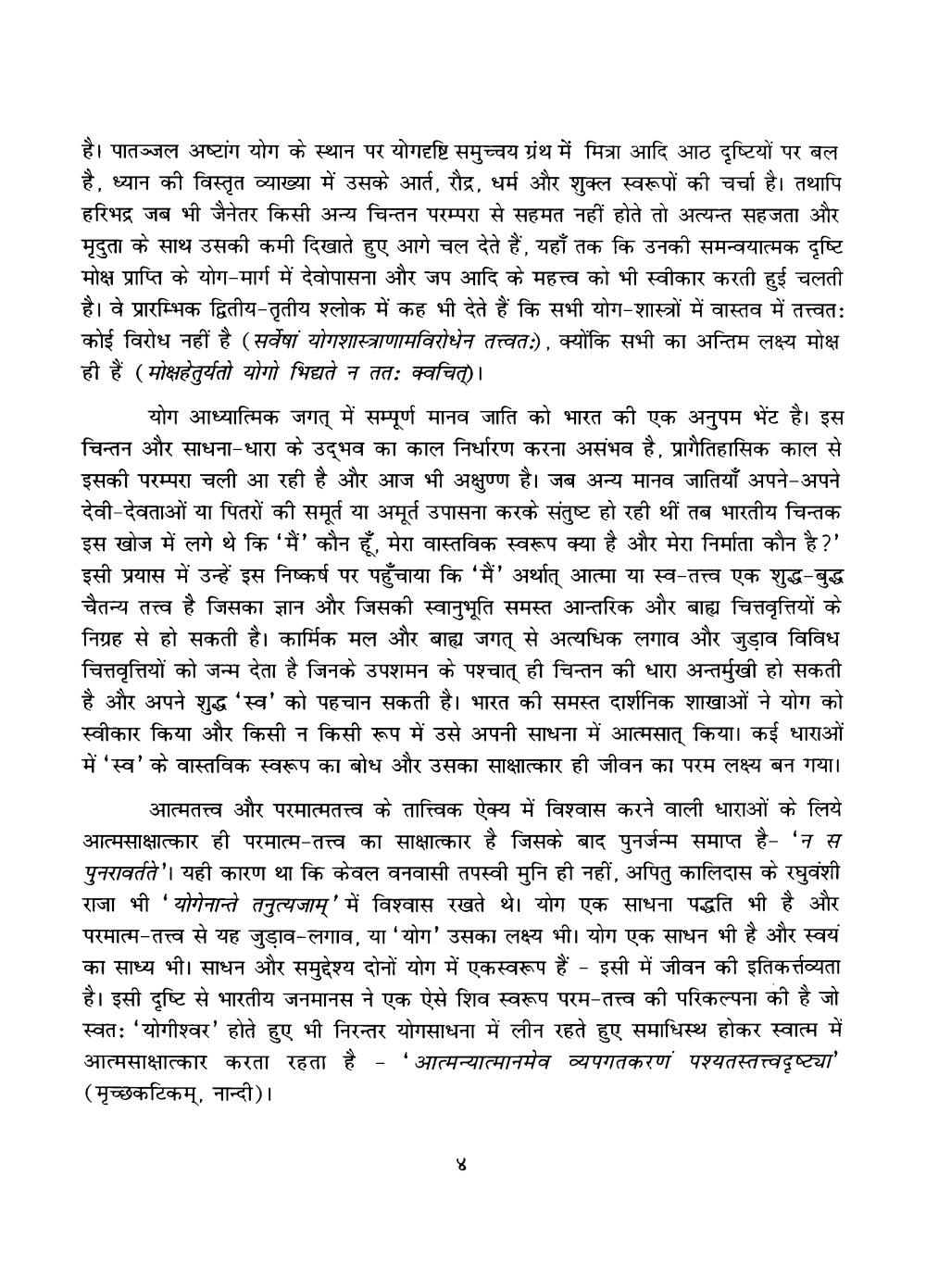________________
पातञ्जल अष्टांग योग के स्थान पर योगदृष्टि समुच्चय ग्रंथ में मित्रा आदि आठ दृष्टियों पर बल है, ध्यान की विस्तृत व्याख्या में उसके आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल स्वरूपों की चर्चा है। तथापि हरिभद्र जब भी जैनेतर किसी अन्य चिन्तन परम्परा से सहमत नहीं होते तो अत्यन्त सहजता और मृदुता के साथ उसकी कमी दिखाते हुए आगे चल देते हैं, यहाँ तक कि उनकी समन्वयात्मक दृष्टि मोक्ष प्राप्ति के योग मार्ग में देवोपासना और जप आदि के महत्त्व को भी स्वीकार करती हुई चलती है। वे प्रारम्भिक द्वितीय तृतीय श्लोक में कह भी देते हैं कि सभी योग- शास्त्रों में वास्तव में तत्त्वतः कोई विरोध नहीं है (सर्वेषां योगशास्त्राणामविरोधेन तत्त्वतः), क्योंकि सभी का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष ही हैं (मोक्षहेतुर्यतो योगो भिद्यते न ततः क्वचित्) ।
योग आध्यात्मिक जगत् में सम्पूर्ण मानव जाति को भारत की एक अनुपम भेंट है। इस चिन्तन और साधना - धारा के उद्भव का काल निर्धारण करना असंभव है, प्रागैतिहासिक काल से इसकी परम्परा चली आ रही है और आज भी अक्षुण्ण है। जब अन्य मानव जातियाँ अपने-अपने देवी-देवताओं या पितरों की समूर्त या अमूर्त उपासना करके संतुष्ट हो रही थीं तब भारतीय चिन्तक इस खोज में लगे थे कि 'मैं' कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मेरा निर्माता कौन है ?" इसी प्रयास में उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि 'मैं' अर्थात् आत्मा या स्व-तत्त्व एक शुद्ध-बुद्ध चैतन्य तत्त्व है जिसका ज्ञान और जिसकी स्वानुभूति समस्त आन्तरिक और बाह्य चित्तवृत्तियों के निग्रह से हो सकती है। कार्मिक मल और बाह्य जगत् से अत्यधिक लगाव और जुड़ाव विविध चित्तवृत्तियों को जन्म देता है जिनके उपशमन के पश्चात् ही चिन्तन की धारा अन्तर्मुखी हो सकती है और अपने शुद्ध 'स्व' को पहचान सकती है। भारत की समस्त दार्शनिक शाखाओं ने योग को स्वीकार किया और किसी न किसी रूप में उसे अपनी साधना में आत्मसात् किया। कई धाराओं में 'स्व' के वास्तविक स्वरूप का बोध और उसका साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य बन गया।
आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्व के तात्त्विक ऐक्य में विश्वास करने वाली धाराओं के लिये आत्मसाक्षात्कार ही परमात्म-तत्त्व का साक्षात्कार है जिसके बाद पुनर्जन्म समाप्त है- 'न स पुनरावर्तते' । यही कारण था कि केवल वनवासी तपस्वी मुनि ही नहीं, अपितु कालिदास के रघुवंशी राजा भी ' योगेनान्ते तनुत्यजाम्' में विश्वास रखते थे। योग एक साधना पद्धति भी है और परमात्म-तत्त्व से यह जुड़ाव लगाव, या 'योग' उसका लक्ष्य भी । योग एक साधन भी है और स्वयं का साध्य भी। साधन और समुद्देश्य दोनों योग में एकस्वरूप हैं - इसी में जीवन की इतिकर्त्तव्यता है । इसी दृष्टि से भारतीय जनमानस ने एक ऐसे शिव स्वरूप परम-तत्त्व की परिकल्पना की है जो स्वतः 'योगीश्वर' होते हुए भी निरन्तर योगसाधना में लीन रहते हुए समाधिस्थ होकर स्वात्म में आत्मसाक्षात्कार करता रहता है ' आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या ' (मृच्छकटिकम्, नान्दी) ।
४