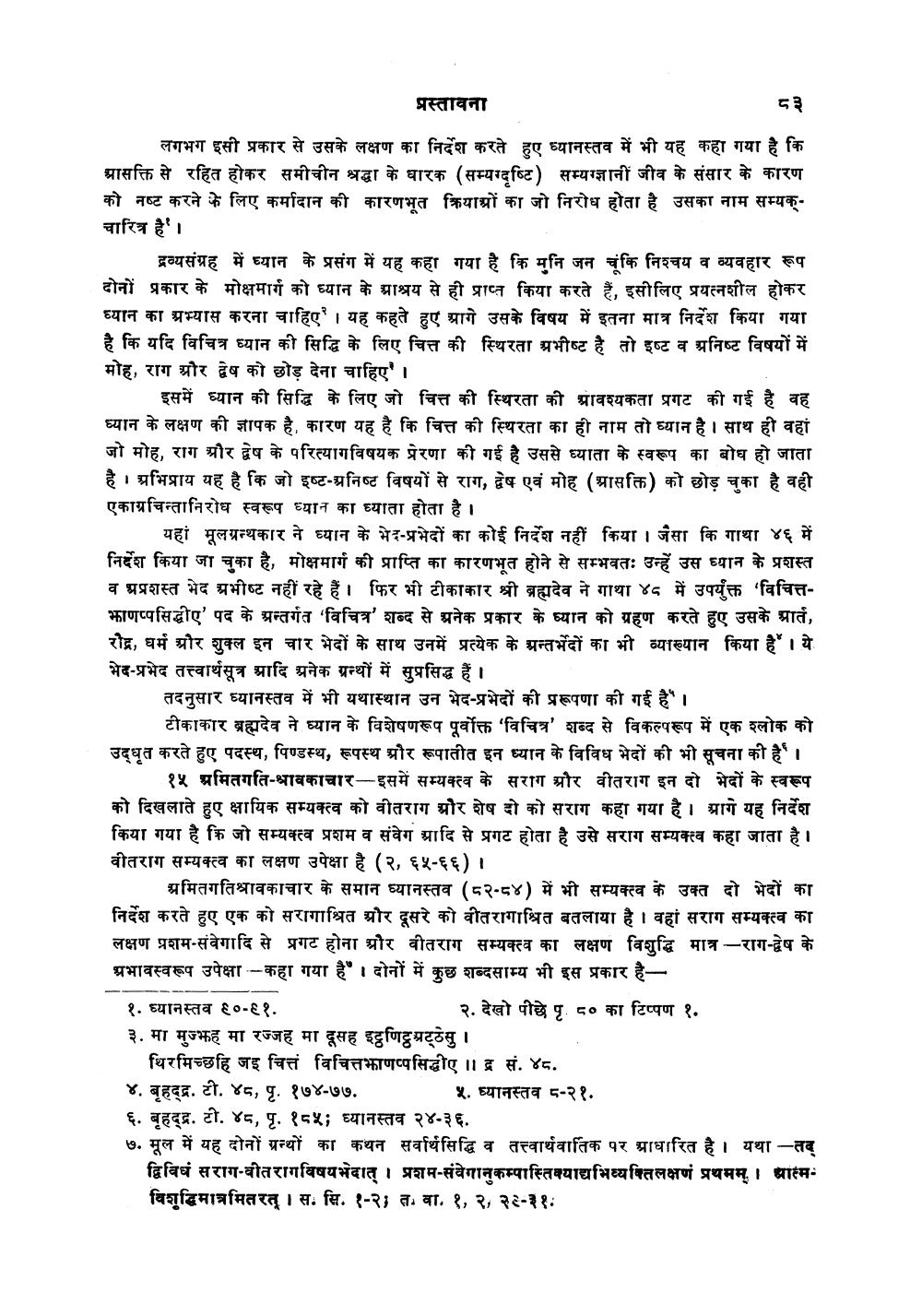________________
प्रस्तावना
८३
लगभग इसी प्रकार से उसके लक्षण का निर्देश करते हुए ध्यानस्तव में भी यह कहा गया है कि आसक्ति से रहित होकर समीचीन श्रद्धा के धारक ( सम्यग्दृष्टि ) सम्यग्ज्ञानी जीव के संसार के कारण को नष्ट करने के लिए कर्मादान की कारणभूत क्रियाओं का जो निरोध होता है उसका नाम सम्यक्चारित्र है' ।
द्रव्यसंग्रह में ध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि मुनि जन चूंकि निश्चय व व्यवहार रूप दोनों प्रकार के मोक्षमार्ग को ध्यान के आश्रय से ही प्राप्त किया करते हैं, इसीलिए प्रयत्नशील होकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए । यह कहते हुए आगे उसके विषय में इतना मात्र निर्देश किया गया है कि यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता अभीष्ट है तो इष्ट व अनिष्ट विषयों में मोह, राग और द्वेष को छोड़ देना चाहिए' ।
इसमें ध्यान की सिद्धि के लिए जो चित्त की स्थिरता की श्रावश्यकता प्रगट की गई है वह ध्यान के लक्षण की ज्ञापक है, कारण यह है कि चित्त की स्थिरता का ही नाम तो ध्यान है। साथ ही वहां जो मोह, राग और द्वेष के परित्यागविषयक प्रेरणा की गई है उससे ध्याता के स्वरूप का बोध हो जाता है | अभिप्राय यह है कि जो इष्ट-अनिष्ट विषयों से राग, द्वेष एवं मोह ( श्रासक्ति) को छोड़ चुका है वही एकाग्रचिन्तानिरोध स्वरूप ध्यान का ध्याता होता है ।
यहां मूलग्रन्थकार ने ध्यान के भेद-प्रभेदों का कोई निर्देश नहीं किया । जैसा कि गाथा ४६ में निर्देश किया जा चुका है, मोक्षमार्ग की प्राप्ति का कारणभूत होने से सम्भवतः उन्हें उस ध्यान के प्रशस्त व अप्रशस्त भेद अभीष्ट नहीं रहे हैं । फिर भी टीकाकार श्री ब्रह्मदेव ने गाथा ४८ में उपर्युक्त ' विचित्तझापसिद्धी' पद के अन्तर्गत 'विचित्र' शब्द से अनेक प्रकार के ध्यान को ग्रहण करते हुए उसके प्रार्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल इन चार भेदों के साथ उनमें प्रत्येक के अन्तर्भेदों का भी व्याख्यान किया है । ये भेद-प्रभेद तत्त्वार्थ सूत्र आदि अनेक ग्रन्थों में सुप्रसिद्ध हैं ।
तदनुसार ध्यानस्तव में भी यथास्थान उन भेद-प्रभेदों की प्ररूपणा की गई है । टीकाकार ब्रह्मदेव ने ध्यान के विशेषणरूप पूर्वोक्त 'विचित्र' शब्द से विकल्परूप में एक श्लोक को उद्धृत करते हुए पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन ध्यान के विविध भेदों की भी सूचना की है । १५ श्रमितगति - श्रावकाचार — इसमें सम्यक्त्व के सराग और वीतराग इन दो भेदों के स्वरूप को दिखलाते हुए क्षायिक सम्यक्त्व को वीतराग और शेष दो को सराग कहा गया है। आगे यह निर्देश किया गया है कि जो सम्यक्त्व प्रशम व संवेग आदि से प्रगट होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहा जाता है । वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण उपेक्षा है (२, ६५-६६ ) ।
श्रमितगतिश्रावकाचार के समान ध्यानस्तव ( ८२-८४ ) में भी सम्यक्त्व के उक्त दो भेदों का निर्देश करते हुए एक को सरागाश्रित और दूसरे को वीतरागाश्रित बतलाया है। वहां सराग सम्यक्त्व का लक्षण प्रशम-संवेगादि से प्रगट होना और वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण विशुद्धि मात्र - राग-द्वेष के प्रभावस्वरूप उपेक्षा कहा गया है। दोनों में कुछ शब्दसाम्य भी इस प्रकार है
२. देखो पीछे पृ. ८० का टिप्पण १.
१. ध्यानस्तव ६०-६१.
३. मा मुज्झह मा रज्जह मा दूसह इट्ठणिट्ठट्ठेसु ।
थिरमिच्छहि जई चित्तं विचित्तभाणप्पसिद्धीए ।। द्र सं. ४८.
४. बृहद्र. टी. ४८, पृ. १७४-७७.
५. ध्यानस्तव ८- २१.
६. बृहद्र. टी. ४८, पृ. १८५; ध्यानस्तव २४-३६.
७. मूल में यह दोनों ग्रन्थों का कथन सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वार्थवार्तिक पर आधारित है । यथा - तद् द्विविधं सराग- वीतरागविषयभेदात् । प्रशम-संवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिव्यक्तिलक्षणं प्रथमम् । आत्मविशुद्धिमात्र मितरत् । स. सि. १ २३ त. वा. १, २, २६-३१: