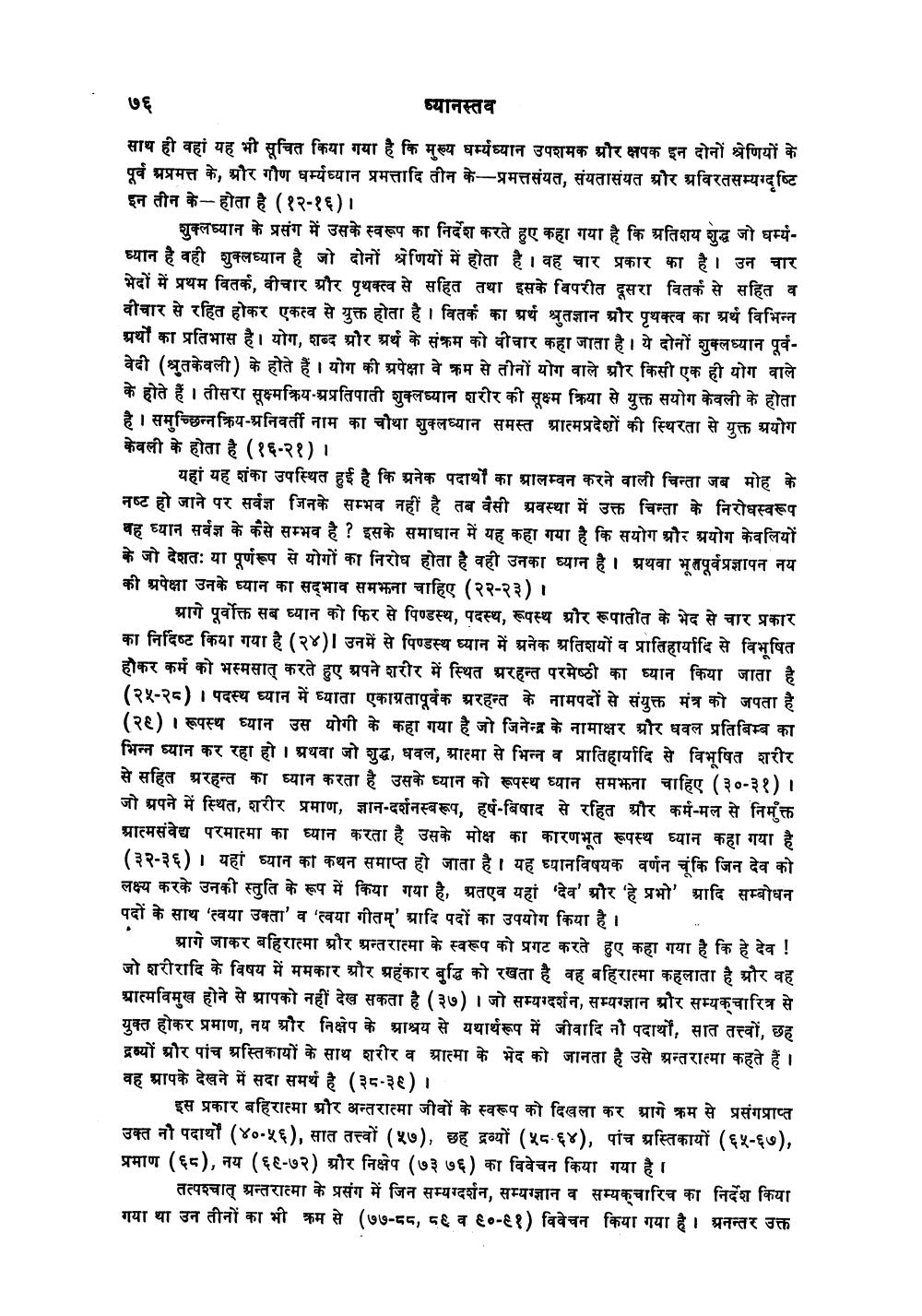________________
७६
ध्यानस्तव
साथ ही वहां यह भी सूचित किया गया है कि मुख्य धर्म्यध्यान उपशमक और क्षपक इन दोनों श्रेणियों के पूर्व अप्रमत्त के, और गौण धर्म्यध्यान प्रमत्तादि तीन के-प्रमत्तसंयत, संयतासंयत और अविरतसम्यग्दृष्टि इन तीन के-होता है (१२-१६)।
___ शुक्लध्यान के प्रसंग में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि अतिशय शुद्ध जो धर्म्यध्यान है वही शुक्लध्यान है जो दोनों श्रेणियों में होता है। वह चार प्रकार का है। उन चार भेदों में प्रथम वितर्क, वीचार और पृथक्त्व से सहित तथा इसके विपरीत दूसरा वितर्क से सहि वीचार से रहित होकर एकत्व से युक्त होता है। वितर्क का अर्थ श्रुतज्ञान और पृथक्त्व का अर्थ विभिन्न अर्थों का प्रतिभास है। योग, शब्द और अर्थ के संक्रम को वीचार कहा जाता है। ये दोनों शुक्लध्यान पूर्ववेदी (श्रुतकेवली) के होते हैं । योग की अपेक्षा वे क्रम से तीनों योग वाले और किसी एक ही योग वाले के होते हैं । तीसरा सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाती शुक्लध्यान शरीर की सूक्ष्म क्रिया से युक्त सयोग केवली के होता है। समुच्छिन्नक्रिय-अनिवर्ती नाम का चौथा शुक्लध्यान समस्त प्रात्मप्रदेशों की स्थिरता से युक्त अयोग केवली के होता है (१६-२१) ।
यहां यह शंका उपस्थित हुई है कि अनेक पदार्थों का पालम्वन करने वाली चिन्ता जब मोह के नष्ट हो जाने पर सर्वज्ञ जिनके सम्भव नहीं है तब वैसी अवस्था में उक्त चिन्ता के निरोधस्वरूप वह ध्यान सर्वज्ञ के कैसे सम्भव है ? इसके समाधान में यह कहा गया है कि सयोग और प्रयोग केवलियों के जो देशतः या पूर्णरूप से योगों का निरोध होता है वही उनका ध्यान है। अथवा भूतपूर्वप्रज्ञापन नय की अपेक्षा उनके ध्यान का सद्भाव समझना चाहिए (२२-२३)।
आगे पूर्वोक्त सब ध्यान को फिर से पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत के भेद से चार प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है (२४)। उनमें से पिण्डस्थ ध्यान में अनेक अतिशयों व प्रातिहादि से विभूषित होकर कर्म को भस्मसात् करते हुए अपने शरीर में स्थित अरहन्त परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है (२५-२८) । पदस्थ ध्यान में ध्याता एकाग्रतापूर्वक अरहन्त के नामपदों से संयुक्त मंत्र को जपता है (२६) । रूपस्थ ध्यान उस योगी के कहा गया है जो जिनेन्द्र के नामाक्षर और धवल प्रतिबिम्ब का भिन्न ध्यान कर रहा हो । अथवा जो शुद्ध, धवल, आत्मा से भिन्न व प्रातिहार्यादि से विभूषित शरीर से सहित अरहन्त का ध्यान करता है उसके ध्यान को रूपस्थ ध्यान समझना चाहिए (३०-३१)। जो अपने में स्थित, शरीर प्रमाण, ज्ञान-दर्शनस्वरूप, हर्ष-बिषाद से रहित और कर्म-मल से निर्मुक्त आत्मसंवेद्य परमात्मा का ध्यान करता है उसके मोक्ष का कारणभूत रूपस्थ ध्यान कहा गया है (३२-३६)। यहां ध्यान का कथन समाप्त हो जाता है। यह ध्यानविषयक वर्णन चूंकि जिन देव को लक्ष्य करके उनकी स्तुति के रूप में किया गया है, अतएव यहां 'देव' और 'हे प्रभो' आदि सम्बोधन पदों के साथ 'त्वया उक्ता' व 'त्वया गीतम्' आदि पदों का उपयोग किया है।
आगे जाकर बहिरात्मा और अन्तरात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि हे देव ! जो शरीरादि के विषय में ममकार और अहंकार बुद्धि को रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है और वह आत्मविमुख होने से आपको नहीं देख सकता है (३७) । जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से युक्त होकर प्रमाण, नय और निक्षेप के आश्रय से यथार्थरूप में जीवादि नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रव्यों और पांच अस्तिकायों के साथ शरीर व आत्मा के भेद को जानता है उसे अन्तरात्मा कहते हैं। वह आपके देखने में सदा समर्थ है (३८-३९)।
इस प्रकार बहिरात्मा और अन्तरात्मा जीवों के स्वरूप को दिखला कर आगे क्रम से प्रसंगप्राप्त उक्त नौ पदार्थों (४०-५६), सात तत्त्वों (५७), छह द्रव्यों (५८-६४), पांच अस्तिकायों (६५-६७), प्रमाण (६८), नय (६६-७२) और निक्षेप (७३ ७६) का विवेचन किया गया है ।
तत्पश्चात् अन्तरात्मा के प्रसंग में जिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारिच का निर्देश किया गया था उन तीनों का भी क्रम से (७७-८८, ८६ व ६०-६१) विवेचन किया गया है। अनन्तर उक्त