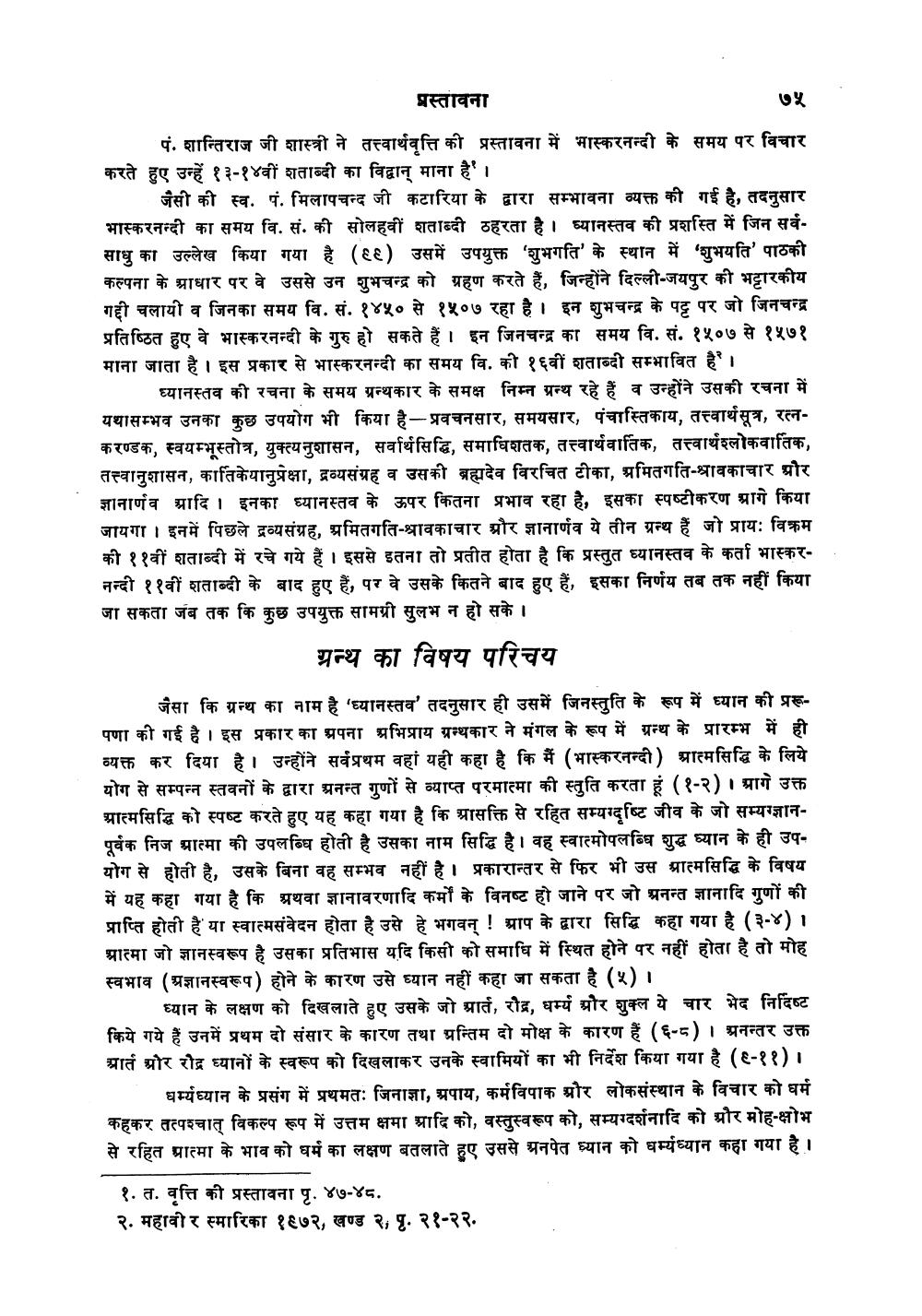________________
प्रस्तावना
७५
पं. शान्तिराज जी शास्त्री ने तत्त्वार्थवृत्ति की प्रस्तावना में भास्करनन्दी के समय पर विचार करते हुए उन्हें १३-१४वीं शताब्दी का विद्वान् माना है' ।
जैसी की स्व. पं. मिलापचन्द जी कटारिया के द्वारा सम्भावना व्यक्त की गई है, तदनुसार भास्करनन्दी का समय वि. सं. की सोलहवीं शताब्दी ठहरता है । ध्यानस्तव की प्रशस्ति में जिन सर्वसाधु का उल्लेख किया गया है ( ६६ ) उसमें उपयुक्त 'शुभगति' के स्थान में 'शुभयति' पाठकी कल्पना के आधार पर वे उससे उन शुभचन्द्र को ग्रहण करते हैं, जिन्होंने दिल्ली-जयपुर की भट्टारकीय गद्दी चलायी व जिनका समय वि. सं. १४५० से १५०७ रहा है। इन शुभचन्द्र के पट्ट पर जो जिनचन्द्र प्रतिष्ठित हुए वे भास्करनन्दी के गुरु हो सकते हैं। इन जिनचन्द्र का समय वि. सं. १५०७ से १५७१ माना जाता है । इस प्रकार से भास्करनन्दी का समय वि. की १६वीं शताब्दी सम्भावित है ।
ध्यानस्तव की रचना के समय ग्रन्थकार के समक्ष निम्न ग्रन्थ रहे हैं व उन्होंने उसकी रचना में यथासम्भव उनका कुछ उपयोग भी किया है - प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, तत्त्वार्थ सूत्र, रत्नकरण्डक, स्वयम्भू स्तोत्र, युक्त्यनुशासन, सर्वार्थसिद्धि, समाधिशतक, तत्त्वार्थवार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, तस्वानुशासन, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, द्रव्यसंग्रह व उसकी ब्रह्मदेव विरचित टीका, अमितगति श्रावकाचार श्रीर ज्ञानार्णव आदि। इनका ध्यानस्तव के ऊपर कितना प्रभाव रहा है, इसका स्पष्टीकरण मागे किया जायगा । इनमें पिछले द्रव्यसंग्रह, श्रमितगति श्रावकाचार और ज्ञानार्णव ये तीन ग्रन्थ हैं जो प्रायः विक्रम की ११वीं शताब्दी में रचे गये हैं । इससे इतना तो प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ध्यानस्तव के कर्ता भास्करनन्दी ११वीं शताब्दी के बाद हुए हैं, पर वे उसके कितने बाद हुए हैं, इसका निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कुछ उपयुक्त सामग्री सुलभ न हो सके ।
ग्रन्थ का विषय परिचय
जैसा कि ग्रन्थ का नाम है 'ध्यानस्तव' तदनुसार ही उसमें जिनस्तुति के रूप में ध्यान की प्ररूपणा की गई है । इस प्रकार का अपना अभिप्राय ग्रन्थकार ने मंगल के रूप में ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही व्यक्त कर दिया है । उन्होंने सर्वप्रथम वहां यही कहा है कि मैं ( भास्करनन्दी ) श्रात्मसिद्धि के लिये योग से सम्पन्न स्तवनों के द्वारा अनन्त गुणों से व्याप्त परमात्मा की स्तुति करता हूं ( १-२ ) । आगे उक्त आत्मसिद्धि को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि आसक्ति से रहित सम्यग्दृष्टि जीव के जो सम्यग्ज्ञानपूर्वक निज श्रात्मा की उपलब्धि होती है उसका नाम सिद्धि है । वह स्वात्मोपलब्धि शुद्ध ध्यान के ही उपयोग से होती है, उसके बिना वह सम्भव नहीं है । प्रकारान्तर से फिर भी उस श्रात्मसिद्धि के विषय में यह कहा गया है कि अथवा ज्ञानावरणादि कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जो अनन्त ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति होती है या स्वात्मसंवेदन होता है उसे हे भगवन् ! आप के द्वारा सिद्धि कहा गया है ( ३-४ ) । श्रात्मा जो ज्ञानस्वरूप है उसका प्रतिभास यदि किसी को समाधि में स्थित होने पर नहीं होता है तो मोह स्वभाव (प्रज्ञानस्वरूप ) होने के कारण उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता है (५) ।
ध्यान के लक्षण को दिखलाते हुए उसके जो प्रार्त, रौद्र, धर्म्यं किये गये हैं उनमें प्रथम दो संसार के कारण तथा अन्तिम दो मोक्ष के आर्त और रौद्र ध्यानों के स्वरूप को दिखलाकर उनके स्वामियों का भी
और शुक्ल ये चार भेद निर्दिष्ट कारण हैं ( ६-८ ) । अनन्तर उक्त निर्देश किया गया है ( ६-११) ।
ध्यान के प्रसंग में प्रथमतः जिनाज्ञा, अपाय, कर्मविपाक और लोकसंस्थान के विचार को धर्म कहकर तत्पश्चात् विकल्प रूप में उत्तम क्षमा आदि को, वस्तुस्वरूप को, सम्यग्दर्शनादि को और मोह-क्षोभ से रहित प्रात्मा के भाव को धर्म का लक्षण बतलाते हुए उससे अनपेत ध्यान को धर्म्यध्यान कहा गया है ।
१. त. वृत्ति की प्रस्तावना पृ. ४७-४८.
२. महावीर स्मारिका १६७२, खण्ड २, पृ. २१-२२.