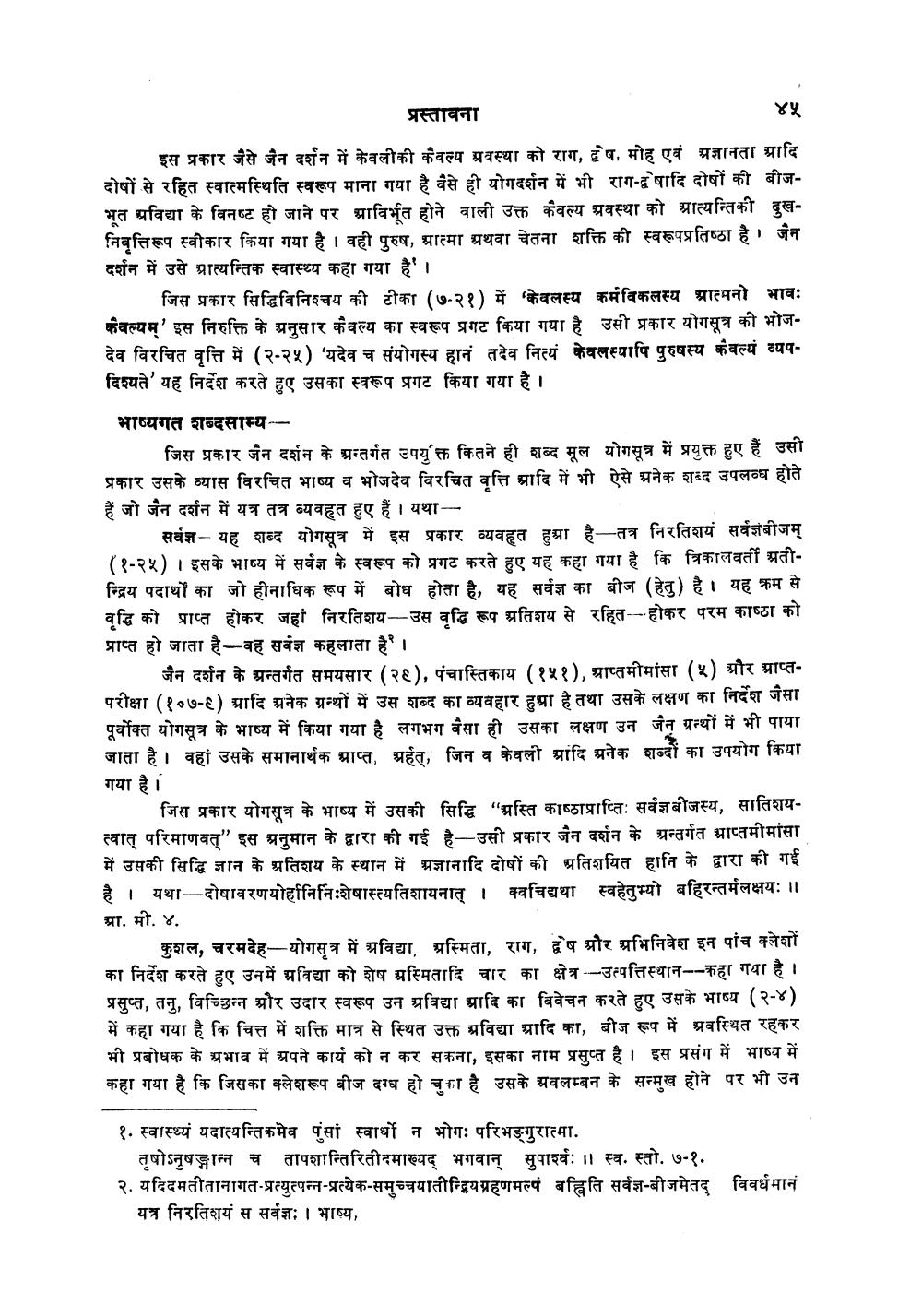________________
प्रस्तावना
४५
इस प्रकार जैसे जैन दर्शन में केवलीकी कैवल्य अवस्था को राग, द्वेष, मोह एवं अज्ञानता आदि दोषों से रहित स्वात्मस्थिति स्वरूप माना गया है वैसे ही योगदर्शन में भी राग-द्वषादि दोषों की बीजभूत अविद्या के विनष्ट हो जाने पर आविर्भूत होने वाली उक्त कैवल्य अवस्था को प्रात्यन्तिकी दुखनिवृत्तिरूप स्वीकार किया गया है । वही पुरुष, प्रात्मा अथवा चेतना शक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठा है। जैन दर्शन में उसे प्रात्यन्तिक स्वास्थ्य कहा गया है।
जिस प्रकार सिद्धिविनिश्चय की टीका (७-२१) में केवलस्य कर्मविकलस्य प्रात्मनो भावः कैवल्यम्' इस निरुक्ति के अनुसार कैवल्य का स्वरूप प्रगट किया गया है उसी प्रकार योगसूत्र की भोजदेव विरचित वृत्ति में (२-२५) 'यदेव च संयोगस्य हानं तदेव नित्यं केवलस्यापि पुरुषस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते' यह निर्देश करते हुए उसका स्वरूप प्रगट किया गया है। भाष्यगत शब्दसाम्य--
जिस प्रकार जैन दर्शन के अन्तर्गत उपयूक्त कितने ही शब्द मूल योगसूत्र में प्रयुक्त हुए हैं उसी प्रकार उसके व्यास विरचित भाष्य व भोजदेव विरचित वत्ति आदि में भी ऐसे अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो जैन दर्शन में यत्र तत्र ब्यवहृत हुए हैं। यथा
सर्वज्ञ--- यह शब्द योगसूत्र में इस प्रकार व्यवहृत हना है-तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् (१-२५) । इसके भाष्य में सर्वज्ञ के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि त्रिकालवर्ती प्रतीन्द्रिय पदार्थों का जो हीनाधिक रूप में बोध होता है, यह सर्वज्ञ का बीज (हेतु) है। यह क्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर जहां निरतिशय-उस वृद्धि रूप अतिशय से रहित-- होकर परम काष्ठा को प्राप्त हो जाता है-वह सर्वज्ञ कहलाता है।
जैन दर्शन के अन्तर्गत समयसार (२६), पंचास्तिकाय (१५१), प्राप्तमीमांसा (५) और प्राप्तपरीक्षा (१०७-६) आदि अनेक ग्रन्थों में उस शब्द का व्यवहार हमा है तथा उसके लक्षण का निर्देश जैसा पूर्वोक्त योगसूत्र के भाष्य में किया गया है लगभग वैसा ही उसका लक्षण उन जैन ग्रन्थों में भी पाया जाता है। वहां उसके समानार्थक प्राप्त, अर्हत, जिन व केवली प्रांदि अनेक शब्दों का उपयोग किया
गया है।
जिस प्रकार योगसूत्र के भाष्य में उसकी सिद्धि "अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य, सातिशयत्वात् परिमाणवत्" इस अनुमान के द्वारा की गई है-उसी प्रकार जैन दर्शन के अन्तर्गत प्राप्तमीमांसा में उसकी सिद्धि ज्ञान के अतिशय के स्थान में अज्ञानादि दोषों की अतिशयित हानि के द्वारा की गई है । यथा-दोषावरणयोहानिनिःशेषास्त्यतिशायनात । क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ।। प्रा. मी. ४.
कुशल, चरमदेह-योगसूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पांच क्लेशों का निर्देश करते हुए उनमें अविद्या को शेष अस्मितादि चार का क्षेत्र--उत्पत्तिस्थान--कहा गया है । प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार स्वरूप उन अविद्या प्रादि का विवेचन करते हुए उसके भाष्य (२-४) में कहा गया है कि चित्त में शक्ति मात्र से स्थित उक्त अविद्या प्रादि का, बीज रूप में अवस्थित रहकर भी प्रबोधक के अभाव में अपने कार्य को न कर सकना, इसका नाम प्रसुप्त है। इस प्रसंग में भाष्य में कहा गया है कि जिसका क्लेशरूप बीज दग्ध हो च का है उसके अवलम्बन के सन्मुख होने पर भी उन
१. स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा.
तृषोऽनुषङ्गान्त च तापशान्तिरितीदमाख्यद् भगवान् सुपार्श्वः । स्व. स्तो. ७-१. २. यदिदमतीतानागत-प्रत्युत्पन्न-प्रत्येक-समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणमल्पं बह्विति सर्वज्ञ-बीजमेतद् विवर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । भाष्य,
मगवान् स्यात् । अतो मत८ विर्धमान