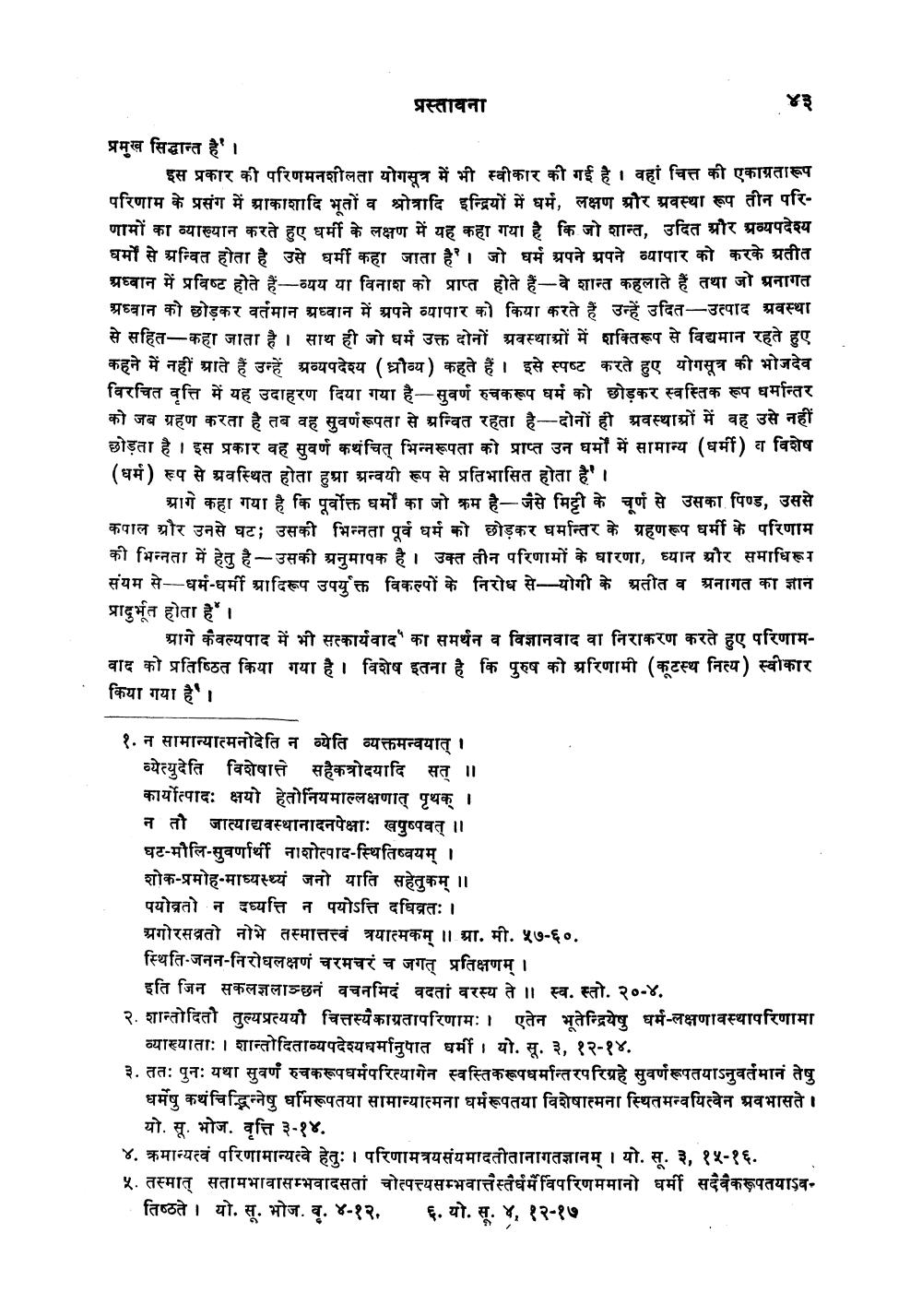________________
प्रस्तावना
प्रमुख सिद्धान्त है'
इस प्रकार की परिणमनशीलता योगसूत्र में भी स्वीकार की गई है । वहां चित्त की एकाग्रतारूप परिणाम के प्रसंग में आकाशादि भूतों व श्रोत्रादि इन्द्रियों में धर्म, लक्षण और अवस्था रूप तीन परिणामों का व्याख्यान करते हुए धर्मी के लक्षण में यह कहा गया है कि जो शान्त, उदित और प्रव्यपदेश्य धर्मों से अन्वित होता है उसे धर्मी कहा जाता है । जो धर्म अपने अपने व्यापार को करके प्रतीत अध्वान में प्रविष्ट होते हैं - व्यय या विनाश को प्राप्त होते हैं - वे शान्त कहलाते हैं तथा जो अनागत
४३
वान को छोड़कर वर्तमान अध्वान में अपने व्यापार को किया करते हैं उन्हें उदित - उत्पाद अवस्था से सहित - कहा जाता है। साथ ही जो धर्म उक्त दोनों अवस्थाओं में शक्तिरूप से विद्यमान रहते हुए कहने में नहीं आते हैं उन्हें अव्यपदेश्य ( ध्रौव्य ) कहते हैं । इसे स्पष्ट करते हुए योगसूत्र की भोजदेव विरचित वृत्ति में यह उदाहरण दिया गया है- सुवर्ण रुचकरूप धर्म को छोड़कर स्वस्तिक रूप धर्मान्तर को जब ग्रहण करता है तब वह सुवर्णरूपता से श्रन्वित रहता है— दोनों ही अवस्थाओं में वह उसे नहीं छोड़ता है । इस प्रकार वह सुवर्ण कथंचित् भिन्नरूपता को प्राप्त उन धर्मों में सामान्य (धर्मी) व विशेष (धर्म) रूप से अवस्थित होता हुआ अन्वयी रूप से प्रतिभासित होता है' ।
आगे कहा गया है कि पूर्वोक्त धर्मों का जो क्रम है - जैसे मिट्टी के चूर्ण से उसका पिण्ड, उससे कपाल और उनसे घट; उसकी भिन्नता पूर्व धर्म को छोड़कर घर्मान्तर के ग्रहणरूप धर्मी के परिणाम की भिन्नता में हेतु है— उसकी अनुमापक है । उक्त तीन परिणामों के धारणा, ध्यान और समाधिरून संयम से -- धर्म-धर्मी आदिरूप उपर्युक्त विकल्पों के निरोध से —— योगी के प्रतीत व अनागत का ज्ञान प्रादुर्भूत होता है।
आगे कैवल्यपाद में भी सत्कार्यवाद' का समर्थन व विज्ञानवाद वा निराकरण करते हुए परिणामवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। विशेष इतना है कि पुरुष को अरिणामी ( कूटस्थ नित्य ) स्वीकार किया गया है।
१. न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् । व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥ कार्योत्पादः क्षयो हेतोर्नियमाल्लक्षणात् पृथक् । न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेक्षाः खपुष्पवत् ॥ घट-मौलि सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थितिष्वयम् । शोक-प्रमोह- माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥ पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः ।
गोरसव्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ।। प्रा. मी. ५७-६०.
स्थिति-जनन-निरोधलक्षणं चरमचरं च जगत् प्रतिक्षणम् ।
इति जिन सकलज्ञलाञ्छनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते ॥ स्व. स्तो. २०-४.
२. शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः । एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म-लक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः । शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपात धर्मी । यो. सू. ३, १२-१४.
३. ततः पुनः यथा सुवर्णं रुचकरूपधर्मपरित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्णरूपतयाऽनुवर्तमानं तेषु धर्मेषु कथंचिद्भिन्नेषु धर्मरूपतया सामान्यात्मना धर्मरूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयित्वेन श्रवभासते । यो. सू. भोज. वृत्ति ३-१४.
४. क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् । यो. सू. ३, १५-१६.
I
५. तस्मात् सतामभावासम्भवादसतां चोत्पत्त्यसम्भवात्तैस्तैर्घ में विपरिणममानो घर्मी सदैवैकरूपतया वतिष्ठते । यो. सू. भोज. बृ. ४-१२. ६. यो. सू. ४, १२-१७