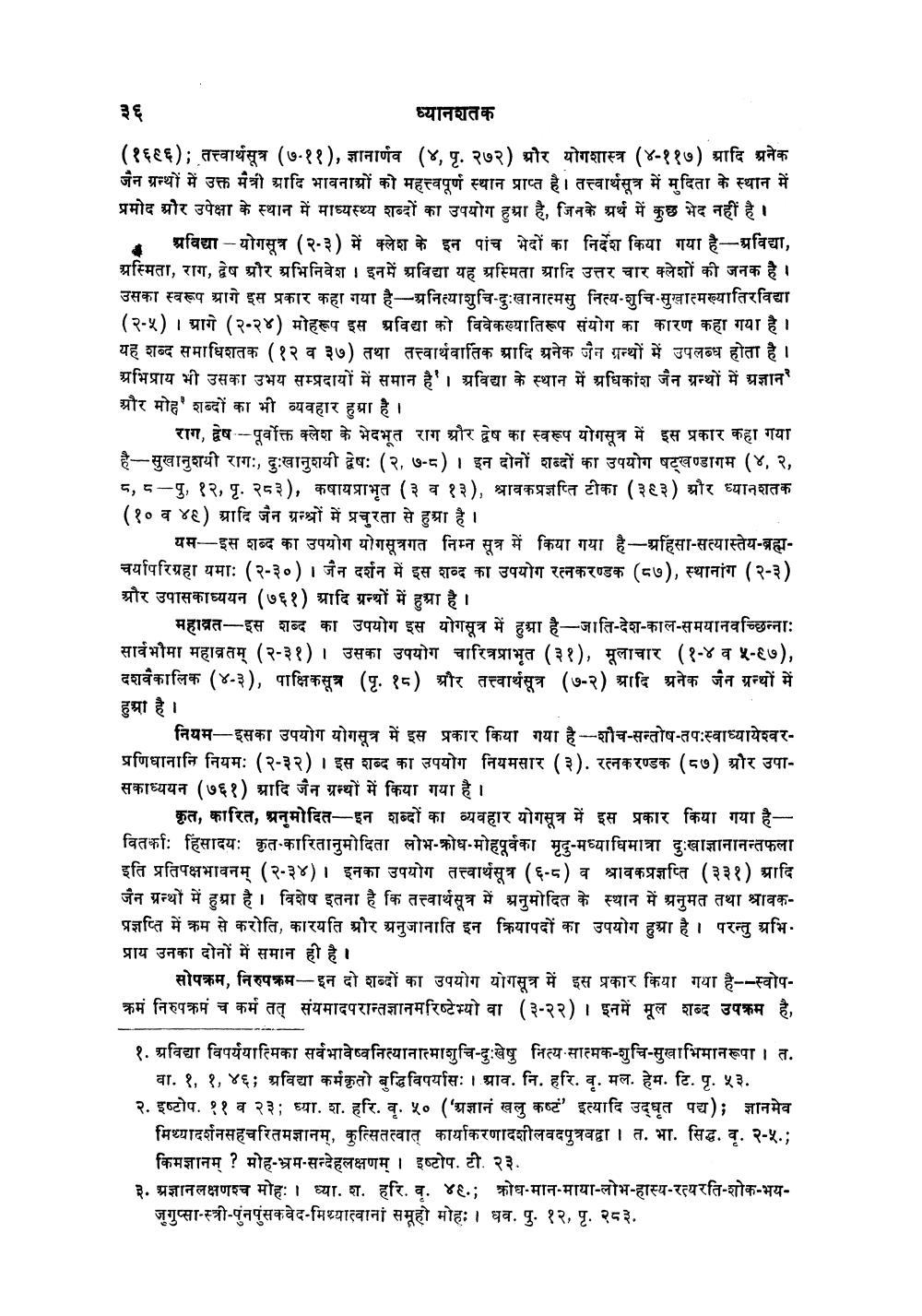________________
ध्यानशतक
(१६९६); तत्त्वार्थसूत्र (७.११), ज्ञानार्णव (४, पृ. २७२) और योगशास्त्र (४-११७) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उक्त मैत्री आदि भावनाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तत्त्वार्थसूत्र में मुदिता के स्थान में प्रमोद और उपेक्षा के स्थान में माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग हमा है, जिनके अर्थ में कुछ भेद नहीं है।
अविद्या -योगसूत्र (२-३) में क्लेश के इन पांच भेदों का निर्देश किया गया है-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । इनमें अविद्या यह अस्मिता आदि उत्तर चार क्लेशों की जनक है । उसका स्वरूप आगे इस प्रकार कहा गया है-अनित्याशुचि-दुःखानात्मसु नित्य-शुचि-सुखात्मख्यातिरविद्या (२-५) । प्रागे (२.२४) मोहरूप इस अविद्या को विवेकख्यातिरूप संयोग का कारण कहा गया है। यह शब्द समाधिशतक (१२ व ३७) तथा तत्त्वार्थवार्तिक आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । अभिप्राय भी उसका उभय सम्प्रदायों में समान है। अविद्या के स्थान में अधिकांश जैन ग्रन्थों में अज्ञान' और मोह शब्दों का भी व्यवहार हुमा है ।
राग, द्वेष -पूर्वोक्त क्लेश के भेदभूत राग और द्वेष का स्वरूप योगसूत्र में इस प्रकार कहा गया है-सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः (२, ७-८)। इन दोनों शब्दों का उपयोग षट्खण्डागम (४, २, ८,८-पु, १२, पृ. २८३), कषायप्राभृत (३ व १३), श्रावकप्रज्ञप्ति टीका (३६३) और ध्यानशतक (१० व ४६) प्रादि जैन ग्रन्थों में प्रचुरता से हुआ है।
यम-इस शब्द का उपयोग योगसूत्रगत निम्न सूत्र में किया गया है-अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (२-३०) । जैन दर्शन में इस शब्द का उपयोग रत्नकरण्डक (८७), स्थानांग (२-३) और उपासकाध्ययन (७६१) आदि ग्रन्थों में हुआ है।
महाव्रत-इस शब्द का उपयोग इस योगसूत्र में हना है-जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् (२-३१)। उसका उपयोग चारित्रप्राभूत (३१), मूलाचार (१-४ व ५-६७), दशवकालिक (४-३), पाक्षिकसूत्र (पृ. १८) और तत्त्वार्थसूत्र (७-२) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में हुआ है।
नियम-इसका उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है-शौच-सन्तोष-तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमः (२-३२) । इस शब्द का उपयोग नियमसार (३). रत्नकरण्डक (८७) और उपासकाध्ययन (७६१) आदि जैन ग्रन्थों में किया गया है।
कृत, कारित, अनुमोदित-इन शब्दों का व्यवहार योगसूत्र में इस प्रकार किया गया हैवितर्काः हिंसादयः कृत-कारितानुमोदिता लोभ-क्रोध-मोहपूर्वका मृदु-मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् (२-३४)। इनका उपयोग तत्त्वार्थसूत्र (६-८) व श्रावकप्रज्ञप्ति (३३१) आदि जैन ग्रन्थों में हुप्रा है। विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसूत्र में अनुमोदित के स्थान में अनुमत तथा श्रावकप्रज्ञप्ति में कम से करोति, कारयति और अनुजानाति इन क्रियापदों का उपयोग हुआ है। परन्तु अभिप्राय उनका दोनों में समान ही है।।
सोपक्रम, निरुपक्रम-इन दो शब्दों का उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार किया गया है--स्वोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत् संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा (३-२२)। इनमें मूल शब्द उपक्रम है,
१. अविद्या विपर्ययात्मिका सर्वभावेष्वनित्यानात्माशुचि-दुःखेषु नित्य-सात्मक-शुचि-सुखाभिमानरूपा। त.
वा. १, १, ४६; अविद्या कर्मकृतो बुद्धिविपर्यासः । प्राव. नि. हरि. व. मल. हेम. टि. पृ. ५३. २. इष्टोप. ११ व २३; ध्या. श. हरि. व. ५० ('अज्ञानं खलु कष्ट' इत्यादि उद्धृत पद्य); ज्ञानमेव मिथ्यादर्शनसहचरितमज्ञानम्, कुत्सितत्वात् कार्याकरणादशीलवदपुत्रवद्वा । त. भा. सिद्ध. व. २-५.;
किमज्ञानम् ? मोह-भ्रम-सन्देहलक्षणम् । इष्टोप. टी. २३. ३. अज्ञानलक्षणश्च मोहः । ध्या. श. हरि. व. ४६.; क्रोध-मान-माया-लोभ-हास्य-रत्यरति-शोक-भय
जुगुप्सा-स्त्री-पुंनपुंसकवेद-मिथ्यात्वानां समूहो मोहः। धव. पु. १२, पृ. २८३.