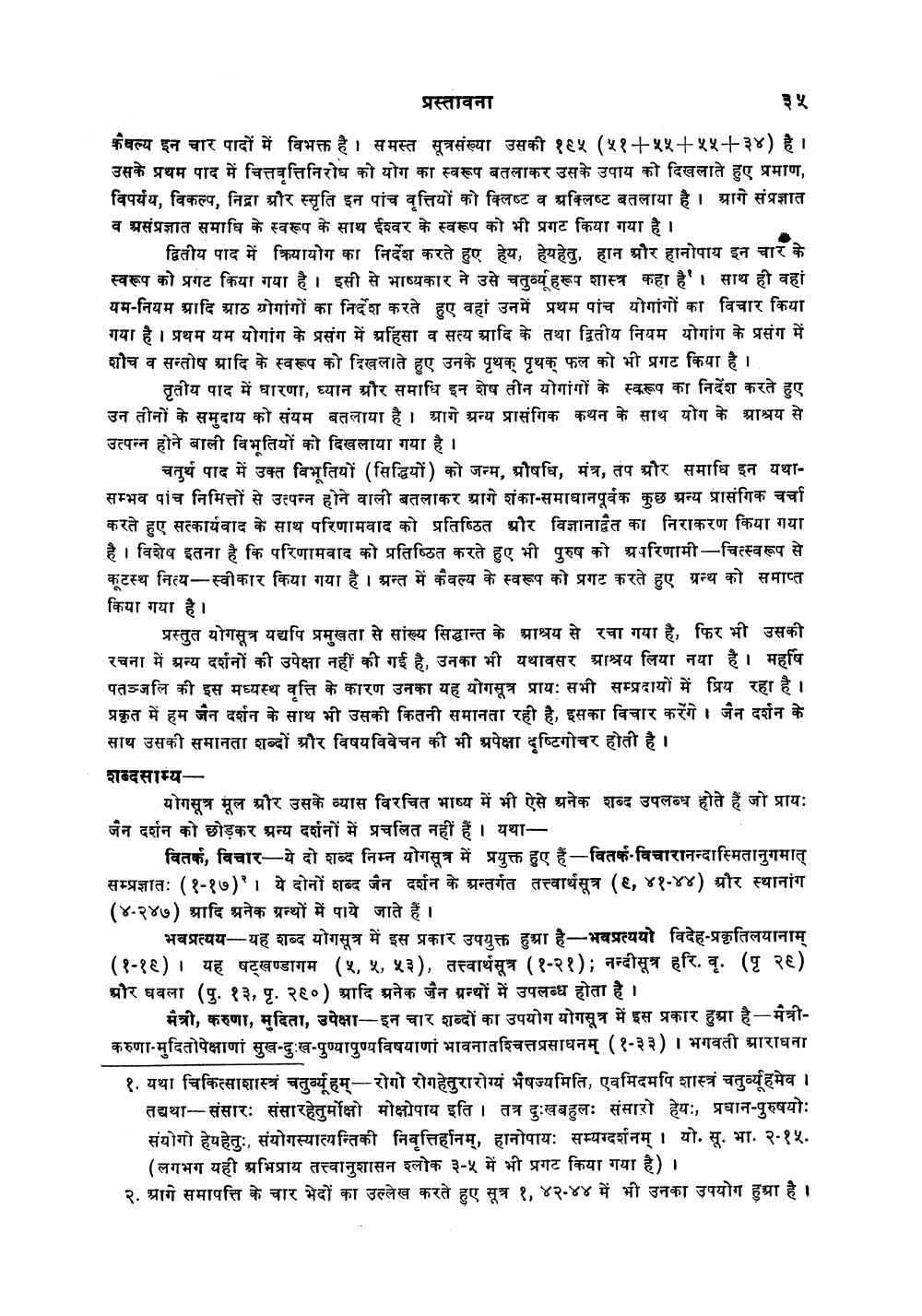________________
प्रस्तावना
३५
ल्य इन चार पादों में विभक्त है । समस्त सूत्रसंख्या उसकी १६५ (५१÷५५ + ५५+३४) है। उसके प्रथम पाद में चित्तवृत्तिनिरोध को योग का स्वरूप बतलाकर उसके उपाय को दिखलाते हुए प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पांच वृत्तियों को क्लिष्ट व अक्लिष्ट बतलाया | आगे संप्रज्ञात व संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप के साथ ईश्वर के स्वरूप को भी प्रगट किया गया है ।
द्वितीयपाद में क्रियायोग का निर्देश करते हुए हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय इन चार के स्वरूप को प्रगट किया गया है । इसी से भाष्यकार ने उसे चतुर्व्यू हरूप शास्त्र कहा है'। साथ ही वहां यम-नियम आदि आठ योगांगों का निर्देश करते हुए वहां उनमें प्रथम पांच योगांगों का विचार किया गया है । प्रथम यम योगांग के प्रसंग में अहिंसा व सत्य आदि के शौच व सन्तोष आदि के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके पृथक् पृथक् फल को भी प्रगट किया है ।
तथा द्वितीय नियम योगांग के प्रसंग में
तृतीय पाद में धारणा, ध्यान और समाधि इन शेष तीन योगांगों के स्वरूप का निर्देश करते हुए उन तीनों के समुदाय को संयम बतलाया है । आगे अन्य प्रासंगिक कथन के साथ योग के आश्रय से उत्पन्न होने बाली विभूतियों को दिखलाया गया है ।
चतुर्थ पाद में उक्त विभूतियों (सिद्धियों) को जन्म, श्रौषधि, मंत्र, तप और समाधि इन यथासम्भव पांच निमित्तों से उत्पन्न होने वाली बतलाकर श्रागे शंका-समाधानपूर्वक कुछ अन्य प्रासंगिक चर्चा करते हुए सत्कार्यवाद के साथ परिणामवाद को प्रतिष्ठित श्रीर विज्ञानाद्वैत का निराकरण किया गया है । विशेष इतना है कि परिणामवाद को प्रतिष्ठित करते हुए भी पुरुष को अपरिणामी – चित्स्वरूप से कूटस्थ नित्य — स्वीकार किया गया है । अन्त में कैवल्य के स्वरूप को प्रगट करते हुए ग्रन्थ को समाप्त किया गया है ।
प्रस्तुत योगसूत्र यद्यपि प्रमुखता से सांख्य सिद्धान्त के श्राश्रय से रचा गया है, फिर भी उसकी रचना में अन्य दर्शनों की उपेक्षा नहीं की गई है, उनका भी यथावसर आश्रय लिया नया है । महर्षि पतञ्जलि की इस मध्यस्थ वृत्ति के कारण उनका यह योगसूत्र प्रायः सभी सम्प्रदायों में प्रिय रहा है । प्रकृत में हम जैन दर्शन के साथ भी उसकी कितनी समानता रही है, इसका विचार करेंगे। जैन दर्शन के साथ उसकी समानता शब्दों और विषयविवेचन की भी अपेक्षा दृष्टिगोचर होती है ।
शब्दसाम्य
योगसूत्र मूल और उसके व्यास विरचित भाष्य में भी ऐसे अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं जो प्रायः जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शनों में प्रचलित नहीं हैं। यथा
वितर्क, विचार – ये दो शब्द निम्न योगसूत्र में प्रयुक्त हुए हैं - वितर्क-विचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः (१-१७) ' । ये दोनों शब्द जैन दर्शन के अन्तर्गत तत्त्वार्थसूत्र (६, ४१-४४ ) और स्थानांग ( ४- २४७ ) आदि अनेक ग्रन्थों में पाये जाते हैं ।
भवप्रत्यय - यह शब्द योगसूत्र में इस प्रकार उपयुक्त हुआ है-भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् (१-१९ ) । यह षट्खण्डागम ( ५, ५, ५३ ), तत्त्वार्थ सूत्र ( १ - २१ ) ; नन्दीसूत्र हरि वृ. ( पृ २६ ) और घवला (पु. १३, पृ. २६०) आदि अनेक जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा- इन चार शब्दों का उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार हुआ है - मैत्रीकरुणा मुदितोपेक्षाणां सुख-दुःख- पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसाधनम् (१-३३) । भगवती आराधना १. यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहम् - रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति, एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव । तद्यथा - संसारः संसारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः, संयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिर्ज्ञानम्, हानोपायः सम्यग्दर्शनम् । यो. सू. भा. २ - १५. ( लगभग यही अभिप्राय तत्त्वानुशासन श्लोक ३-५ में भी प्रगट किया गया है ) ।
२. प्रागे समापत्ति के चार भेदों का उल्लेख करते हुए सूत्र १, ४२-४४ में भी उनका उपयोग हुआ है ।