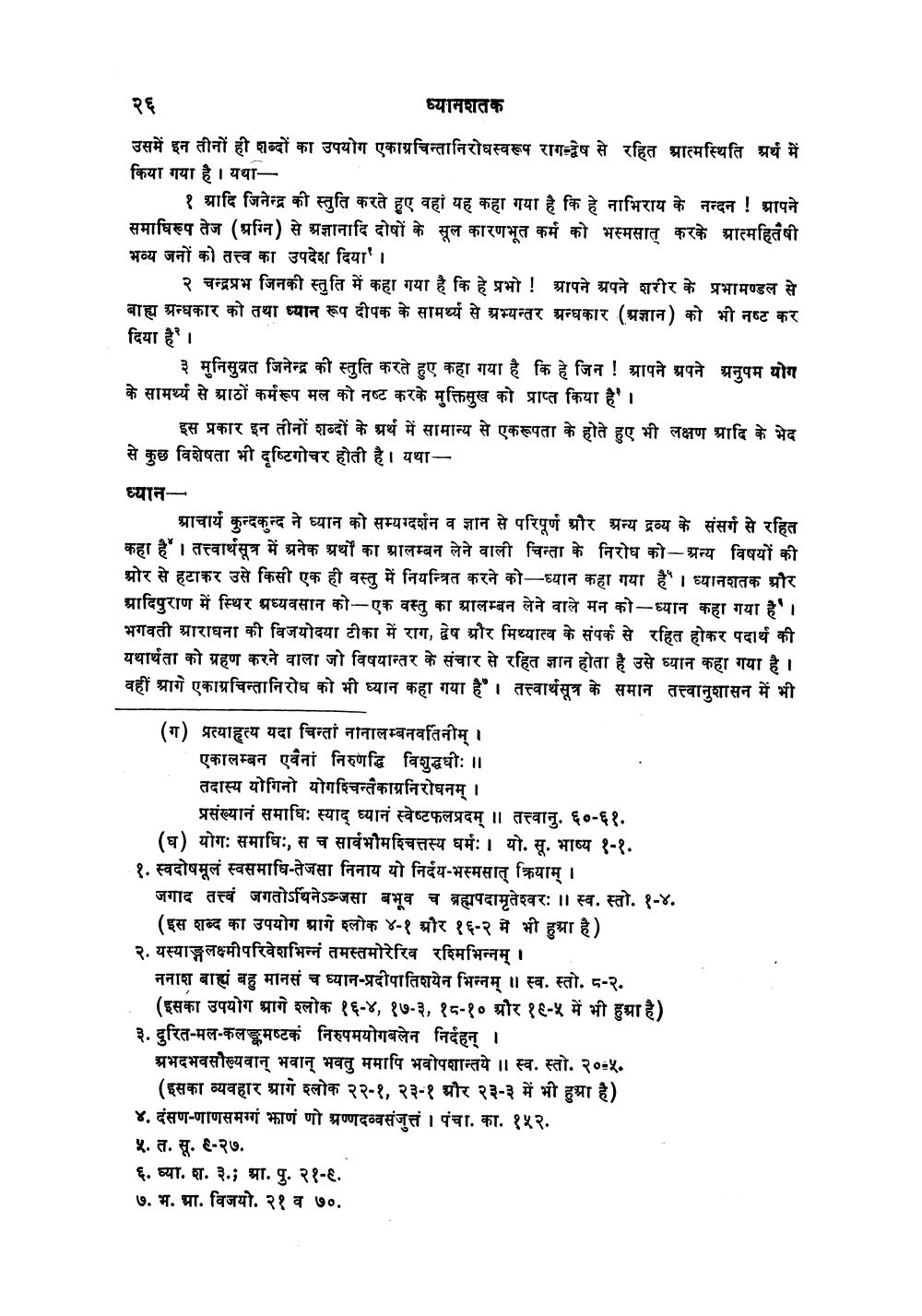________________
२६
ध्यानशतक
उसमें इन तीनों ही शब्दों का उपयोग एकाग्रचिन्तानिरोधस्वरूप राग-द्वेष से रहित प्रात्मस्थिति अर्थ में किया गया है । यथा
१ आदि जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए वहां यह कहा गया है कि हे नाभिराय के नन्दन ! आपने समाधिरूप तेज (अग्नि) से अज्ञानादि दोषों के सूल कारणभूत कर्म को भस्मसात् करके आत्महितषी भव्य जनों को तत्त्व का उपदेश दिया।
२ चन्द्रप्रभ जिनकी स्तुति में कहा गया है कि हे प्रभो! आपने अपने शरीर के प्रभामण्डल से बाह्य अन्धकार को तथा ध्यान रूप दीपक के सामर्थ्य से अभ्यन्तर अन्धकार (अज्ञान) को भी नष्ट कर दिया है।
३ मुनिसुव्रत जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे जिन ! आपने अपने अनुपम योग के सामर्थ्य से पाठों कर्मरूप मल को नष्ट करके मुक्तिसुख को प्राप्त किया है।
इस प्रकार इन तीनों शब्दों के अर्थ में सामान्य से एकरूपता के होते हुए भी लक्षण प्रादि के भेद से कुछ विशेषता भी दृष्टिगोचर होती है। यथा
ध्यान
प्राचार्य कुन्दकुन्द ने ध्यान को सम्यग्दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य द्रव्य के संसर्ग से रहित कहा है । तत्त्वार्थसूत्र में अनेक अर्थों का पालम्बन लेने वाली चिन्ता के निरोध को- अन्य विषयों की ओर से हटाकर उसे किसी एक ही वस्तु में नियन्त्रित करने को-ध्यान कहा गया है। ध्यानशतक और आदिपुराण में स्थिर अध्यवसान को-एक वस्तु का पालम्बन लेने वाले मन को-ध्यान कहा गया है। भगवती आराधना की विजयोदया टीका में राग, द्वेष और मिथ्यात्व के संपर्क से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करने वाला जो विषयान्तर के संचार से रहित ज्ञान होता है उसे ध्यान कहा गया है। वहीं आगे एकाग्रचिन्तानिरोध को भी ध्यान कहा गया है। तत्त्वार्थसूत्र के समान तत्त्वानुशासन में भी
(ग) प्रत्याहृत्य यदा चिन्तां नानालम्बनवतिनीम् ।
एकालम्बन एवैनां निरुणद्धि विशुद्धधीः ।। तदास्य योगिनो योगश्चिन्तकाग्रनिरोधनम् ।
प्रसंख्यानं समाधिः स्याद् ध्यानं स्वेष्टफलप्रदम् ॥ तत्त्वानु. ६०-६१. (घ) योगः समाधिः, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। यो. सू. भाष्य १-१. १. स्वदोषमूलं स्वसमाधि-तेजसा निनाय यो निर्दय-भस्मसात् क्रियाम् ।
जगाद तत्त्वं जगतोऽथिनेऽञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥ स्व. स्तो. १-४. (इस शब्द का उपयोग आगे श्लोक ४-१ और १६-२ में भी हुआ है) २. यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेशभिन्नं तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नम् । ननाश बाह्यं बहु मानसं च ध्यान-प्रदीपातिशयेन भिन्नम् ॥ स्व. स्तो. ८-२. (इसका उपयोग आगे श्लोक १६-४, १७-३, १८-१० और १९-५ में भी हुआ है) ३. दुरित-मल-कलङ्कमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्दहन् । अभदभवसौख्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशान्तये ।। स्व. स्तो. २०-५.
(इसका व्यवहार प्रागे श्लोक २२-१, २३-१ और २३-३ में भी हुआ है) ४. सण-णाणसमग्गं झाणं णो अण्णदव्वसंजुत्तं । पंचा. का. १५२. ५. त. सू. ६-२७. ६. ध्या. श. ३., प्रा. पु. २१-६. ७. भ. प्रा. विजयो. २१ व ७०.