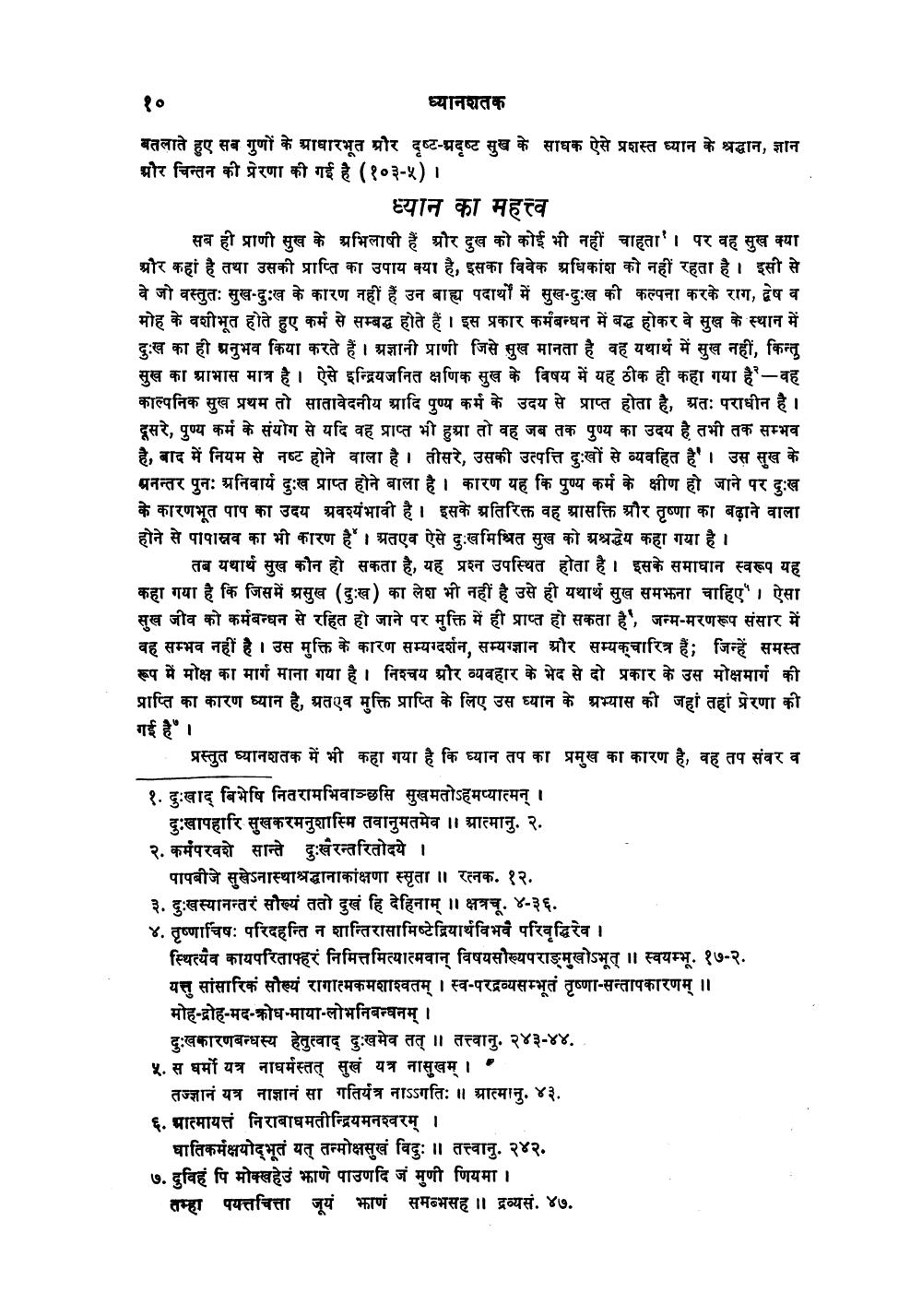________________
१०
ध्यानशतक
बतलाते हुए सब गुणों के आधारभूत और दृष्ट-प्रदृष्ट सुख के साधक ऐसे प्रशस्त ध्यान के श्रद्धान, ज्ञान और चिन्तन की प्रेरणा की गई है (१०३-५) ।
ध्यान का महत्त्व सब ही प्राणी सुख के अभिलाषी हैं और दुख को कोई भी नहीं चाहता। पर वह सुख क्या और कहां है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका विवेक अधिकांश को नहीं रहता है। इसी से वे जो वस्तुतः सुख-दुःख के कारण नहीं हैं उन बाह्य पदार्थों में सुख-दुःख की कल्पना करके राग, द्वेष व मोह के वशीभूत होते हुए कर्म से सम्बद्ध होते हैं । इस प्रकार कर्मबन्धन में बद्ध होकर बे सुख के स्थान में दुःख का ही अनुभव किया करते हैं । अज्ञानी प्राणी जिसे सुख मानता है वह यथार्थ में सुख नहीं, किन्तु सुख का आभास मात्र है। ऐसे इन्द्रियजनित क्षणिक सुख के विषय में यह ठीक ही कहा गया है। वह काल्पनिक सुख प्रथम तो सातावेदनीय आदि पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है, अतः पराधीन है। दूसरे, पुण्य कर्म के संयोग से यदि वह प्राप्त भी हुआ तो वह जब तक पुण्य का उदय है तभी तक सम्भव है, बाद में नियम से नष्ट होने वाला है। तीसरे, उसकी उत्पत्ति दुःखों से व्यवहित है'। उस सुख के अनन्तर पुनः अनिवार्य दुःख प्राप्त होने बाला है। कारण यह कि पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर दुःख के कारणभूत पाप का उदय अवश्यंभावी है। इसके अतिरिक्त वह आसक्ति और तृष्णा का बढ़ाने वाला होने से पापासव का भी कारण है। अतएव ऐसे दुःखमिश्रित सुख को अश्रद्धेय कहा गया है।
तब यथार्थ सुख कौन हो सकता है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसके समाधान स्वरूप यह कहा गया है कि जिसमें असुख (दुःख) का लेश भी नहीं है उसे ही यथार्थ सुख समझना चाहिए। ऐसा सुख जीव को कर्मबन्धन से रहित हो जाने पर मुक्ति में ही प्राप्त हो सकता है', जन्म-मरणरूप संसार में वह सम्भव नहीं है । उस मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं, जिन्हें समस्त रूप में मोक्ष का मार्ग माना गया है। निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार के उस मोक्षमार्ग की प्राप्ति का कारण ध्यान है, अतएव मुक्ति प्राप्ति के लिए उस ध्यान के अभ्यास की जहां तहां प्रेरणा की गई है।
- प्रस्तुत ध्यानशतक में भी कहा गया है कि ध्यान तप का प्रमुख का कारण है, वह तप संवर व १. दुःखाद् बिभेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।
दु:खापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ।। आत्मानु. २. २. कर्मपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये ।
पापबीजे सुखेऽनास्थाश्रद्धानाकांक्षणा स्सृता ॥ रत्नक. १२. ३. दुःखस्यानन्तरं सौख्यं ततो दुखं हि देहिनाम् ॥ क्षत्रचू. ४-३६. ४. तृष्णाचिष: परिदहन्ति न शान्तिरासामिष्टेद्रियार्थविभवै परिवद्धिरेव । स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्तमित्यात्मवान् विषयसौख्यपराङ्मुखोऽभूत् ।। स्वयम्भू. १७-२. यस्तु सांसारिक सौख्यं रागात्मकमशाश्वतम् । स्व-परद्रव्यसम्भूतं तृष्णा-सन्तापकारणम् ।। मोह-द्रोह-मद-क्रोध-माया-लोभनिबन्धनम् ।
दुःखकारणबन्धस्य हेतुत्वाद् दुःखमेव तत् ॥ तत्त्वानु. २४३-४४. ५. स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत् सुखं यत्र नासुखम् । .
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नाऽऽगतिः ॥ आत्मानु. ४३. ६.मात्मायत्तं निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरम् ।
घातिकर्मक्षयोद्भूतं यत् तन्मोक्षसुखं विदुः ॥ तत्त्वानु. २४२. ७. दुविहं पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जं मुणी णियमा । तम्हा पयत्तचित्ता जूयं झाणं समन्भसह ॥ द्रव्यसं. ४७.