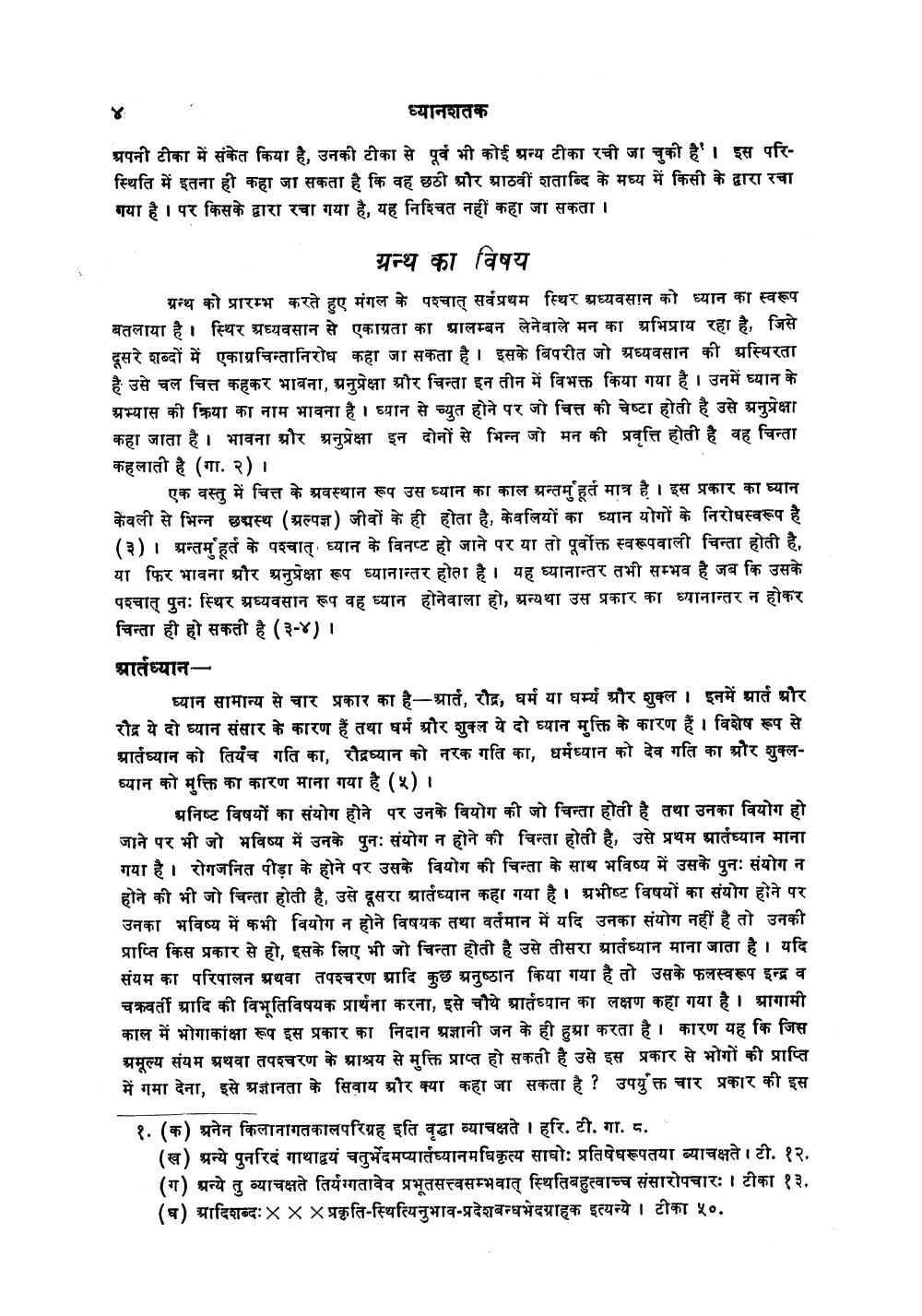________________
ध्यानशतक
अपनी टीका में संकेत किया है, उनकी टीका से पूर्व भी कोई अन्य टीका रची जा चुकी है। इस परिस्थिति में इतना ही कहा जा सकता है कि वह छठी और पाठवीं शताब्दि के मध्य में किसी के द्वारा रचा गया है । पर किसके द्वारा रचा गया है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।
ग्रन्थ का विषय ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए मंगल के पश्चात् सर्वप्रथम स्थिर अध्यवसान को ध्यान का स्वरूप बतलाया है। स्थिर अध्यवसान से एकाग्रता का पालम्बन लेनेवाले मन का अभिप्राय रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जा सकता है। इसके विपरीत जो अध्यवसान की अस्थिरता है उसे चल चित्त कहकर भाबना, अनुप्रेक्षा और चिन्ता इन तीन में विभक्त किया गया है। उनमें ध्यान के अभ्यास की क्रिया का नाम भावना है। ध्यान से च्युत होने पर जो चित्त की चेष्टा होती है उसे अनुप्रेक्षा कहा जाता है। भावना और अनुप्रेक्षा इन दोनों से भिन्न जो मन की प्रवृत्ति होती है वह चिन्ता कहलाती है (गा. २)।
एक वस्तु में चित्त के अवस्थान रूप उस ध्यान का काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है । इस प्रकार का ध्यान केवली से भिन्न छद्मस्थ (अल्पज्ञ) जीवों के ही होता है, केवलियों का ध्यान योगों के निरोधस्वरूप है (३)। अन्तमहर्त के पश्चात ध्यान के विनष्ट हो जाने पर या तो पूर्वोक्त स्वरूपवाली चिन्ता होती है, या फिर भावना और अनुप्रेक्षा रूप ध्यानान्तर होता है। यह ध्यानान्तर तभी सम्भव है जब कि उसके पश्चात् पुनः स्थिर अध्यवसान रूप वह ध्यान होनेवाला हो, अन्यथा उस प्रकार का ध्यानान्तर न होकर चिन्ता ही हो सकती है (३-४) । प्रार्तध्यान
ध्यान सामान्य से चार प्रकार का है-पात, रौद्र, धर्म या धर्म्य और शुक्ल । इनमें प्रार्त और रौद्र ये दो ध्यान संसार के कारण हैं तथा धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान मुक्ति के कारण हैं। विशेष रूप से प्रार्तध्यान को तिथंच गति का, रौद्रध्यान को नरक गति का, धर्मध्यान को देव गति का और शुक्लध्यान को मुक्ति का कारण माना गया है (५)।
अनिष्ट विषयों का संयोग होने पर उनके वियोग की जो चिन्ता होती है तथा उनका वियोग हो जाने पर भी जो भविष्य में उनके पुनः संयोग न होने की चिन्ता होती है, उसे प्रथम प्रार्तध्यान माना गया है। रोगजनित पीड़ा के होने पर उसके वियोग की चिन्ता के साथ भविष्य में उसके पुनः संयोग न होने की भी जो चिन्ता होती है, उसे दूसरा आर्तध्यान कहा गया है। अभीष्ट विषयों का संयोग होने पर उनका भविष्य में कभी वियोग न होने विषयक तथा वर्तमान में यदि उनका संयोग नहीं है तो उनकी प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसके लिए भी जो चिन्ता होती है उसे तीसरा पार्तध्यान माना जाता है। यदि संयम का परिपालन अथवा तपश्चरण आदि कुछ अनुष्ठान किया गया है तो उसके फलस्वरूप इन्द्र व चक्रवर्ती आदि की विभूतिविषयक प्रार्थना करना, इसे चौथे आर्तध्यान का लक्षण कहा गया है। आगामी काल में भोगाकांक्षा रूप इस प्रकार का निदान अज्ञानी जन के ही हुआ करता है। कारण यह कि जिस अमूल्य संयम अथवा तपश्चरण के प्राश्रय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे इस प्रकार से भोगों की प्राप्ति में गमा देना, इसे अज्ञानता के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? उपर्युक्त चार प्रकार की इस
१. (क) अनेन किलानागतकालपरिग्रह इति वृद्धा व्याचक्षते । हरि. टी. गा. ८.
(ख) अन्ये पुनरिदं गाथाद्वयं चतुर्भेदमप्यार्तध्यानमधिकृत्य साघोः प्रतिषेधरूपतया ब्याचक्षते । टी. १२. (ग) अन्ये तु व्याचक्षते तिर्यग्गतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भवात् स्थितिबहुत्वाच्च संसारोपचारः। टीका १३. (घ) आदिशब्दःxxxप्रकृति-स्थित्यिनुभाव-प्रदेशबन्धभेदग्राहक इत्यन्ये । टीका ५०.