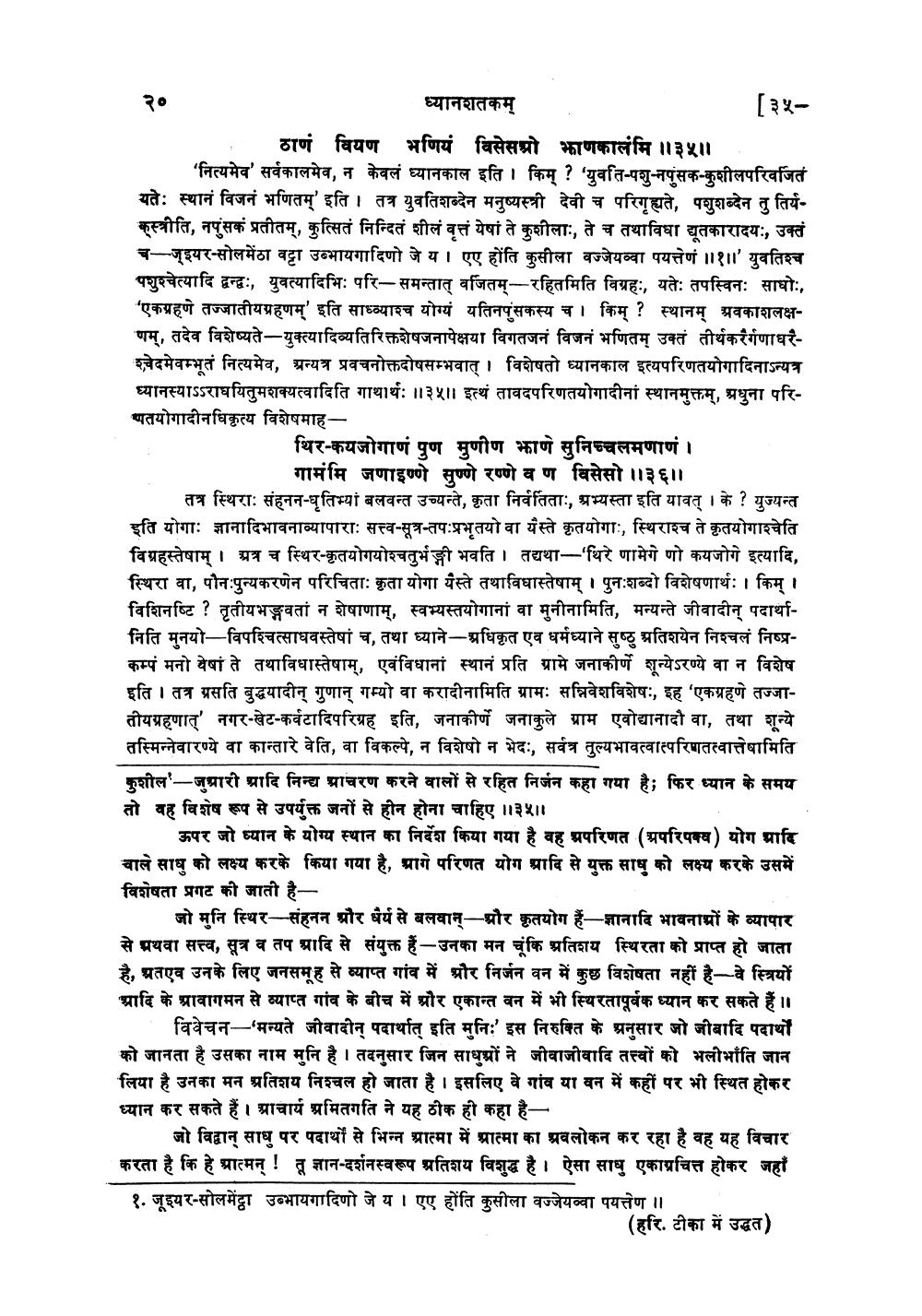________________
ध्यानशतकम्
[३५ठाणं वियण भणियं विसेसमो झाणकालंमि ॥३५॥ . 'नित्यमेव' सर्वकालमेव, न केवलं ध्यानकाल इति । किम् ? 'युवति-पशु-नपुंसक-कुशीलपरिवजितं यते: स्थानं विजनं भणितम्' इति । तत्र युवतिशब्देन मनुष्यस्त्री देवी च परिगृह्यते, पशुशब्देन तु तिर्यस्त्रीति, नपुंसकं प्रतीतम्, कुत्सितं निन्दितं शीलं वृत्तं येषां ते कुशीलाः, ते च तथाविधा द्यूतकारादयः, उक्तं च-जइयर-सोलमेंठा वट्टा उब्भायगादिणो जे य । एए होंति कूसीला वज्जेयव्वा पयत्तेणं ॥१॥' युवतिश्च पशुश्चेत्यादि द्वन्द्वः, युवत्यादिभिः परि-समन्तात् वजितम्-रहितमिति विग्रहः, यतेः तपस्विनः साधोः, "एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणम्' इति साध्व्याश्च योग्यं यतिनपुंसकस्य च । किम् ? स्थानम् अवकाशलक्षणम्, तदेव विशेष्यते-युक्त्यादिव्यतिरिक्तशेषजनापेक्षया विगतजनं विजनं भणितम् उक्तं तीर्थकरैर्गणाधरैश्वेदमेवम्भूतं नित्यमेव, अन्यत्र प्रवचनोक्तदोषसम्भवात् । विशेषतो ध्यानकाल इत्यपरिणतयोगादिनाऽन्यत्र ध्यानस्याऽऽराधयितुमशक्यत्वादिति गाथार्थः ॥३५॥ इत्थं तावदपरिणतयोगादीनां स्थानमुक्तम्, अधुना परिणतयोगादीनधिकृत्य विशेषमाह
थिर-कयजोगाणं पुण मुणीण झाणे सुनिच्चलमणाणं ।
गामंमि जणाइण्णे सुण्णे रणे व ण विसेसो ॥३६॥ तत्र स्थिराः संहनन-धृतिभ्यां बलवन्त उच्यन्ते, कृता निर्वतिताः, अभ्यस्ता इति यावत् । के ? युज्यन्त इति योगाः ज्ञानादिभावनाव्यापाराः सत्त्व-सूत्र-तपःप्रभृतयो वा यैस्ते कृतयोगाः, स्थिराश्च ते कृतयोगाश्चेति विग्रहस्तेषाम् । अत्र च स्थिर-कृतयोगयोश्चतुर्भङ्गी भवति । तद्यथा-'थिरे णामेगे णो कयजोगे इत्यादि, स्थिरा वा, पौनःपुन्यकरणेन परिचिताः कृता योगा यस्ते तथाविधास्तेषाम् । पुनःशब्दो विशेषणार्थः । किम् । विशिनष्टि ? तृतीयभङ्गवतां न शेषाणाम्, स्वभ्यस्तयोगानां वा मुनीनामिति, मन्यन्ते जीवादीन् पदार्थानिति मुनयो-विपश्चित्साधवस्तेषां च, तथा ध्याने-अधिकृत एव धर्मध्याने सुष्ठु अतिशयेन निश्चलं निष्प्रकम्पं मनो येषां ते तथाविधास्तेषाम्, एवंविधानां स्थानं प्रति ग्रामे जनाकीर्णे शून्येऽरण्ये वा न विशेष इति । तत्र असति बुद्धयादीन् गुणान् गम्यो वा करादीनामिति ग्रामः सन्निवेशविशेषः, इह 'एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्' नगर-खेट-कर्वटादिपरिग्रह इति, जनाकीर्णे जनाकुले ग्राम एवोद्यानादौ वा, तथा शून्ये तस्मिन्नेवारण्ये वा कान्तारे वेति, वा विकल्पे, न विशेषो न भेदः, सर्वत्र तुल्यभावत्वात्परिणतत्वात्तेषामिति कुशील'—जुपारी प्रादि निन्द्य पाचरण करने वालों से रहित निर्जन कहा गया है। फिर ध्यान के समय तो वह विशेष रूप से उपर्युक्त जनों से हीन होना चाहिए ॥३५॥
ऊपर जो ध्यान के योग्य स्थान का निर्देश किया गया है वह अपरिणत (अपरिपक्व) योग प्रादि वाले साधु को लक्ष्य करके किया गया है, प्रागे परिणत योग प्रादि से युक्त साधु को लक्ष्य करके उसमें विशेषता प्रगट की जाती है
जो मुनि स्थिर-संहनन और धैर्य से बलवान-और कृतयोग हैं-ज्ञानादि भावनामों के व्यापार से प्रथवा सत्त्व, सूत्र व तप आदि से संयुक्त हैं-उनका मन चूंकि अतिशय स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, अतएव उनके लिए जनसमूह से व्याप्त गांव में और निर्जन वन में कुछ विशेषता नहीं है-वे स्त्रियों आदि के आवागमन से व्याप्त गांव के बीच में और एकान्त वन में भी स्थिरतापूर्वक ध्यान कर सकते हैं।
विवेचन–'मन्यते जीवादीन् पदार्थात् इति मुनिः' इस निरुक्ति के अनुसार जो जीबादि पदार्थों । जानता है उसका नाम मुनि है । तदनुसार जिन साधुनों ने जीवाजीवादि तत्त्वों को भलीभाँति जान लिया है उनका मन अतिशय निश्चल हो जाता है । इसलिए वे गांव या वन में कहीं पर भी स्थित होकर ध्यान कर सकते हैं। प्राचार्य अमितगति ने यह ठीक ही कहा है
____ जो विद्वान् साधु पर पदार्थों से भिन्न प्रात्मा में प्रात्मा का अवलोकन कर रहा है वह यह विचार करता है कि हे प्रात्मन् ! तू ज्ञान-दर्शनस्वरूप अतिशय विशुद्ध है। ऐसा साधु एकाग्रचित्त होकर जहाँ १. जूइयर-सोलमेंट्टा उन्भायगादिणो जे य । एए होंति कुसीला वज्जेयन्वा पयत्तेण ।।
(हरि. टीका में उद्धत)