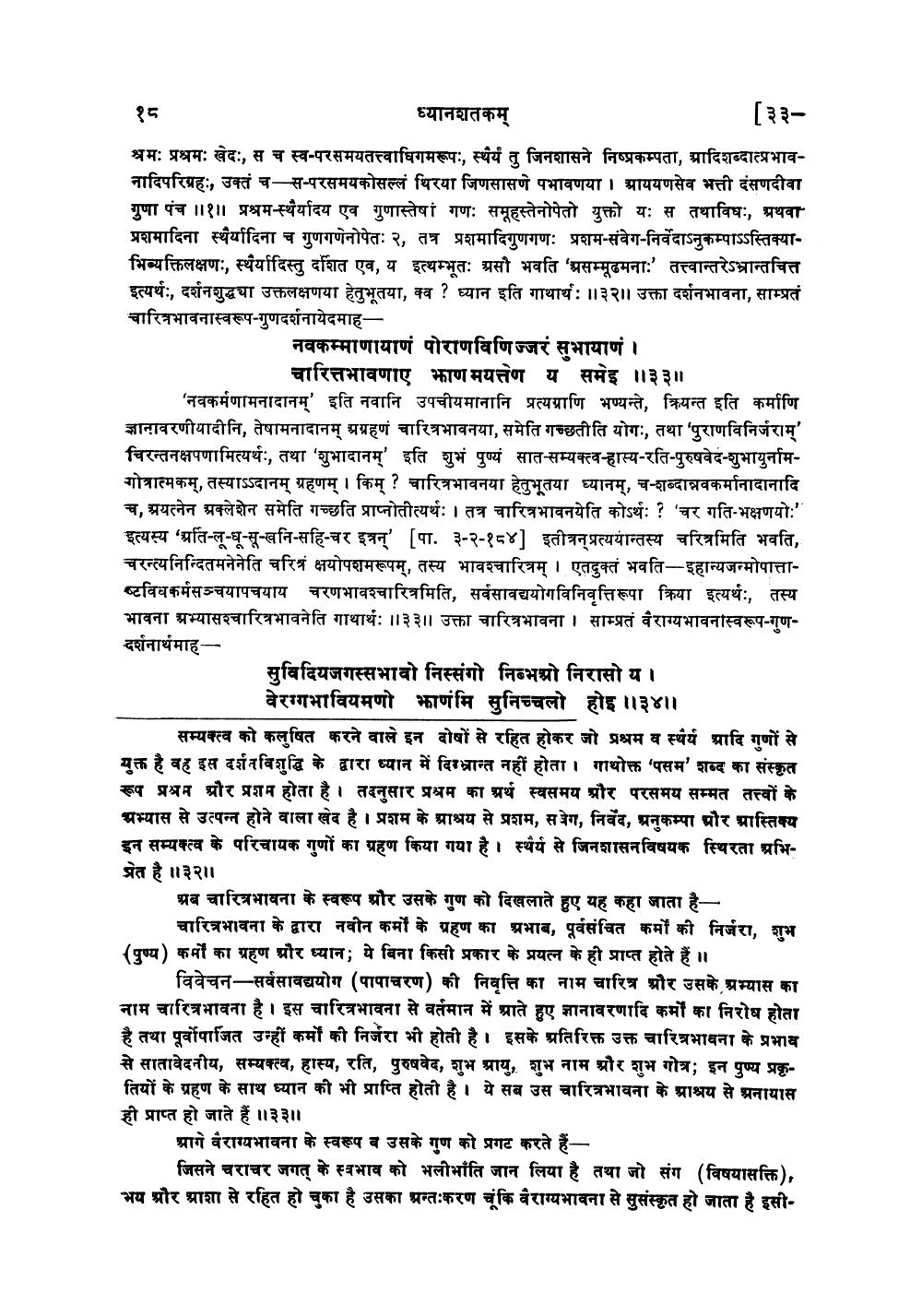________________
ध्यानशतकम्
[३३
श्रमः प्रश्रमः खेदः, स च स्व-परसमयतत्त्वाधिगमरूपः, स्थैर्य तु जिनशासने निष्प्रकम्पता, आदिशब्दात्प्रभावनादिपरिग्रहः, उक्तं च-स-परसमयकोसल्लं थिरया जिणसासणे पभावणया। प्राययणसेव भत्ती दंसणदीव गुणा पंच ॥१॥ प्रश्रम-स्थैर्यादय एव गुणास्तेषां गणः समूहस्तेनोपेतो युक्तो यः स तथाविधः, अथवा प्रशमादिना स्थैर्यादिना च गुणगणेनोपेतः २, तत्र प्रशमादिगुणगणः प्रशम-संवेग-निर्वेदाऽनुकम्पाऽऽस्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणः, स्थैर्यादिस्तु दर्शित एव, य इत्थम्भूतः असौ भवति 'असम्मूढमनाः' तत्त्वान्तरेऽभ्रान्तचित्त इत्यर्थः, दर्शनशुद्धया उक्तलक्षणया हेतुभूतया, क्व ? ध्यान इति गाथार्थः ॥३२॥ उक्ता दर्शनभावना, साम्प्रतं चारित्रभावनास्वरूप-गुणदर्शनायेदमाह
नवकम्माणायाणं पोराणविणिज्जरं सुभायाणं ।
चारित्तभावणाए झाणमयत्तण य समेइ ॥३३॥ 'नवकर्मणामनादानम्' इति नवानि उपचीयमानानि प्रत्यग्राणि भण्यन्ते, क्रियन्त इति कर्माणि ज्ञानावरणीयादीनि, तेषामनादानम् अग्रहणं चारित्रभावनया, समेति गच्छतीति योगः, तथा 'पुराणविनिर्जराम्' चिरन्तनक्षपणामित्यर्थः, तथा 'शुभादानम्' इति शुभं पुण्यं सात-सम्यक्त्व-हास्य-रति-पुरुषवेद-शुभायुर्नामगोत्रात्मकम्, तस्याऽऽदानम् ग्रहणम् । किम् ? चारित्रभावनया हेतुभूतया ध्यानम्, च-शब्दान्नवकर्मानादानादि च, अयत्नेन अक्लेशेन समेति गच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः । तत्र चारित्रभावनयेति कोऽर्थः ? 'चर गति-भक्षणयोः' इत्यस्य 'अति-लू-धू-सू-खनि-सहि-चर इत्रन्' [पा. ३-२-१८४] इतीत्रन्प्रत्ययान्तस्य चरित्रमिति भवति, चरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्रं क्षयोपशमरूपम्, तस्य भावश्चारित्रम् । एतदुक्तं भवति-इहान्यजन्मोपात्ताष्टविवकर्मसञ्चयापचयाय चरणभावश्चारित्रमिति, सर्वसावद्ययोगविनिवत्तिरूपा क्रिया इत्यर्थः, तस्य भावना अभ्यासश्चारित्रभावनेति गाथार्थः ॥३३॥ उक्ता चारित्रभावना। साम्प्रतं वैराग्यभावनास्वरूप-गुणदर्शनार्थमाह
सुविदियजगस्सभावो निस्संगो निब्भनो निरासो य।
वेरग्गभावियमणो झाणंमि सुनिच्चलो होइ ॥३४॥ सम्यक्त्व को कलुषित करने वाले इन दोषों से रहित होकर जो प्रश्रम व स्थर्य प्रादि गुणों से युक्त है वह इस दर्शनविशुद्धि के द्वारा ध्यान में दिग्भ्रान्त नहीं होता। गाथोक्त 'पसम' शब्द का संस्कृत रूप प्रश्रम और प्रशम होता है। तदनुसार प्रश्रम का अर्थ स्वसमय और परसमय सम्मत तत्त्वों के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला खेद है। प्रशम के प्राश्रय से प्रशम, सबेग, निवेद, अनुकम्पा और मास्तिक्य इन सम्यक्त्व के परिचायक गुणों का ग्रहण किया गया है। स्थैर्य से जिनशासनविषयक स्थिरता अभिप्रेत है ॥३२॥
अब चारित्रभावना के स्वरूप और उसके गुण को दिखलाते हुए यह कहा जाता है
चारित्रभावना के द्वारा नवीन कर्मों के ग्रहण का प्रभाब, पूर्वसंचित कर्मों की निर्जरा, शुभ (पुण्य) कर्मों का ग्रहण और ध्यान; ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के ही प्राप्त होते हैं ।
विवेचन-सर्वसावद्ययोग (पापाचरण) की निवृत्ति का नाम चारित्र और उसके अभ्यास का नाम चारित्रभावना है। इस चारित्रभावना से वर्तमान में प्राते हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का निरोध होता है तथा पूर्वोपाजित उन्हीं कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसके अतिरिक्त उक्त चारित्रभावना के प्रभाव से सातावेदनीय, सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुषवेद, शुभ प्रायु, शुभ नाम और शुभ गोत्र; इन पुण्य प्रकृतियों के ग्रहण के साथ ध्यान की भी प्राप्ति होती है। ये सब उस चारित्रभावना के प्राश्रय से अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥३३॥
आगे वैराग्यभावना के स्वरूप व उसके गुण को प्रगट करते हैं
जिसने चराचर जगत् के स्वभाव को भलीभाँति जान लिया है तथा जो संग (विषयासक्ति), भय और पाशा से रहित हो चुका है उसका अन्तःकरण चूंकि वैराग्यभावना से सुसंस्कृत हो जाता है इसी