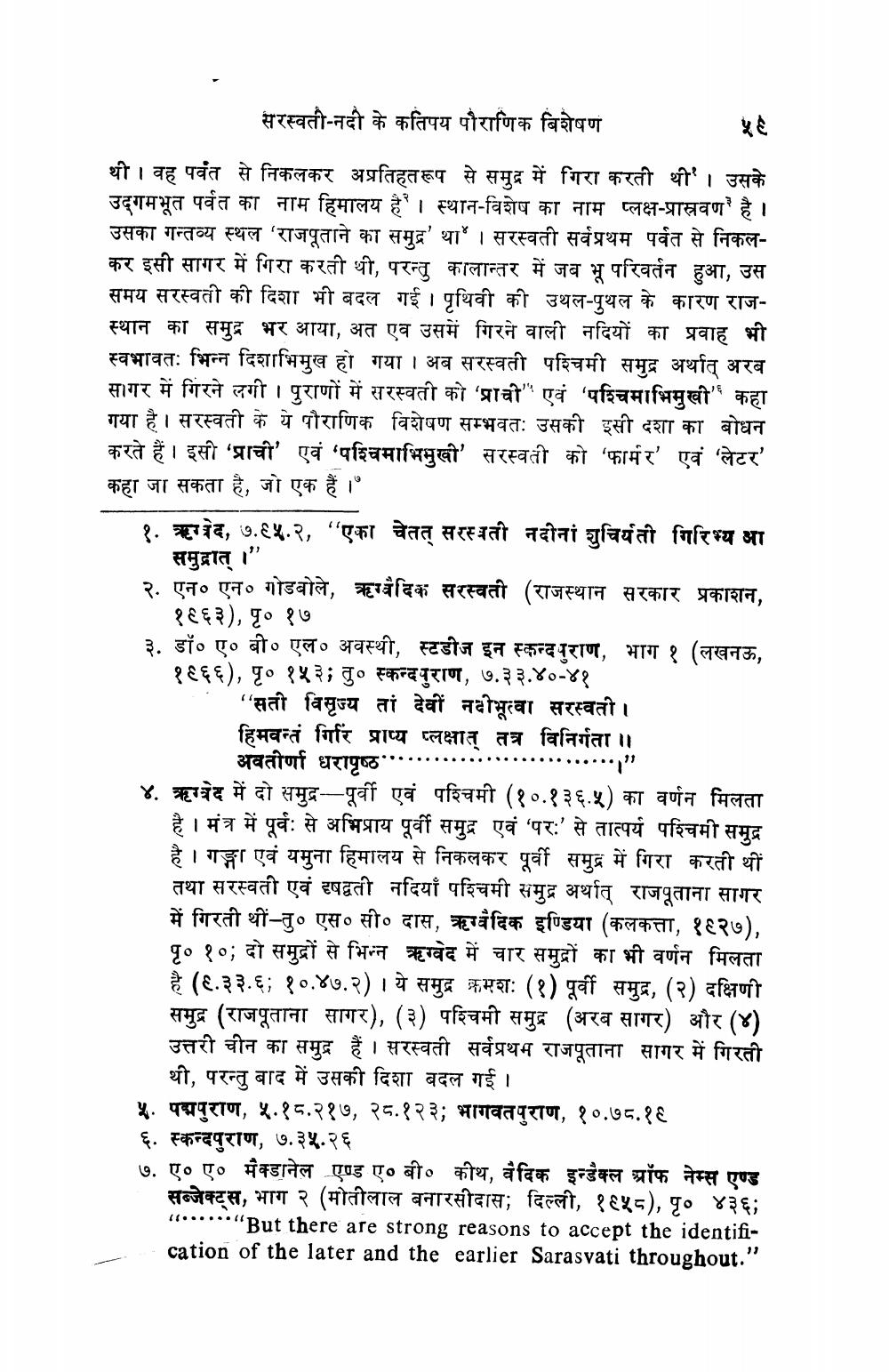________________
सरस्वती नदी के कतिपय पौराणिक विशेषण
५ह
थी । वह पर्वत से निकलकर अप्रतिहतरूप से समुद्र में गिरा करती थी । उसके उद्गमभूत पर्वत का नाम हिमालय है । स्थान- विशेष का नाम प्लक्ष - प्रास्रवण है । उसका गन्तव्य स्थल 'राजपूताने का समुद्र' था । सरस्वती सर्वप्रथम पर्वत से निकलकर इसी सागर में गिरा करती थी, परन्तु कालान्तर में जब भू परिवर्तन हुआ, उस समय सरस्वती की दिशा भी बदल गई । पृथिवी की उथल-पुथल के कारण राजस्थान का समुद्र भर आया, अत एव उसमें गिरने वाली नदियों का प्रवाह भी स्वभावतः भिन्न दिशाभिमुख हो गया । अब सरस्वती पश्चिमी समुद्र अर्थात् अरब सागर में गिरने लगी । पुराणों में सरस्वती को 'प्राची" एवं 'पश्चिमाभिमुखी" कहा गया है । सरस्वती के ये पौराणिक विशेषण सम्भवतः उसकी इसी दशा का बोधन करते हैं । इसी 'प्राची' एवं 'पश्चिमाभिमुखी' सरस्वती को 'फार्मर' एवं 'लेटर' कहा जा सकता है, जो एक हैं । "
१. ऋग्वेद, ७.६५.२, "एका चेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात्
२. एन० एन० गोडबोले, ऋग्वैदिक सरस्वती ( राजस्थान सरकार प्रकाशन, १९६३), पृ० १७
३. डॉ० ए० बी० एल० अवस्थी, स्टडीज इन स्कन्दपुराण भाग १ ( लखनऊ, १९६६), पृ० १५३; तु० स्कन्दपुराण, ७.३३.४०-४१
" सती विसृज्य तां देवीं नदीभूत्वा सरस्वती । हिमवन्तं गिरिं प्राप्य लक्षात् तत्र विनिर्गता ॥ अवतीर्णा धरापृष्ठ
"1
४. ऋग्वेद में दो समुद्र - पूर्वी एवं पश्चिमी ( १०.१३६. ५ ) का वर्णन मिलता है । मंत्र में पूर्व से अभिप्राय पूर्वी समुद्र एवं ' पर : ' से तात्पर्य पश्चिमी समुद्र है । गङ्गा एवं यमुना हिमालय से निकलकर पूर्वी समुद्र में गिरा करती थीं तथा सरस्वती एवं दृषद्वती नदियाँ पश्चिमी समुद्र अर्थात् राजपूताना सागर में गिरती थीं- तु० एस० सी० दास, ऋग्वैदिक इण्डिया ( कलकत्ता, १९२७), पृ० १०; दो समुद्रों से भिन्न ऋग्वेद में चार समुद्रों का भी वर्णन मिलता है (६.३३.६; १०.४७ . २ ) । ये समुद्र क्रमश: ( १ ) पूर्वी समुद्र, (२) दक्षिणी समुद्र ( राजपूताना सागर), (३) पश्चिमी समुद्र ( अरब सागर ) और (४) उत्तरी चीन का समुद्र हैं । सरस्वती सर्वप्रथम राजपूताना सागर में गिरती थी, परन्तु बाद में उसकी दिशा बदल गई ।
५. पद्मपुराण, ५.१८.२१७, २८.१२३; भागवत पुराण, १०.७८.१६ ६. स्कन्दपुराण, ७.३५.२६
७. ए० ए० मैक्डानेल एण्ड ए० बी० कीथ, वैदिक इन्डेक्ल प्रॉफ नेम्स एण्ड सब्जेक्ट्स, भाग २ (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९५८), पृ० ४३६; “••••••‘But there are strong reasons to accept the identification of the later and the earlier Sarasvati throughout."