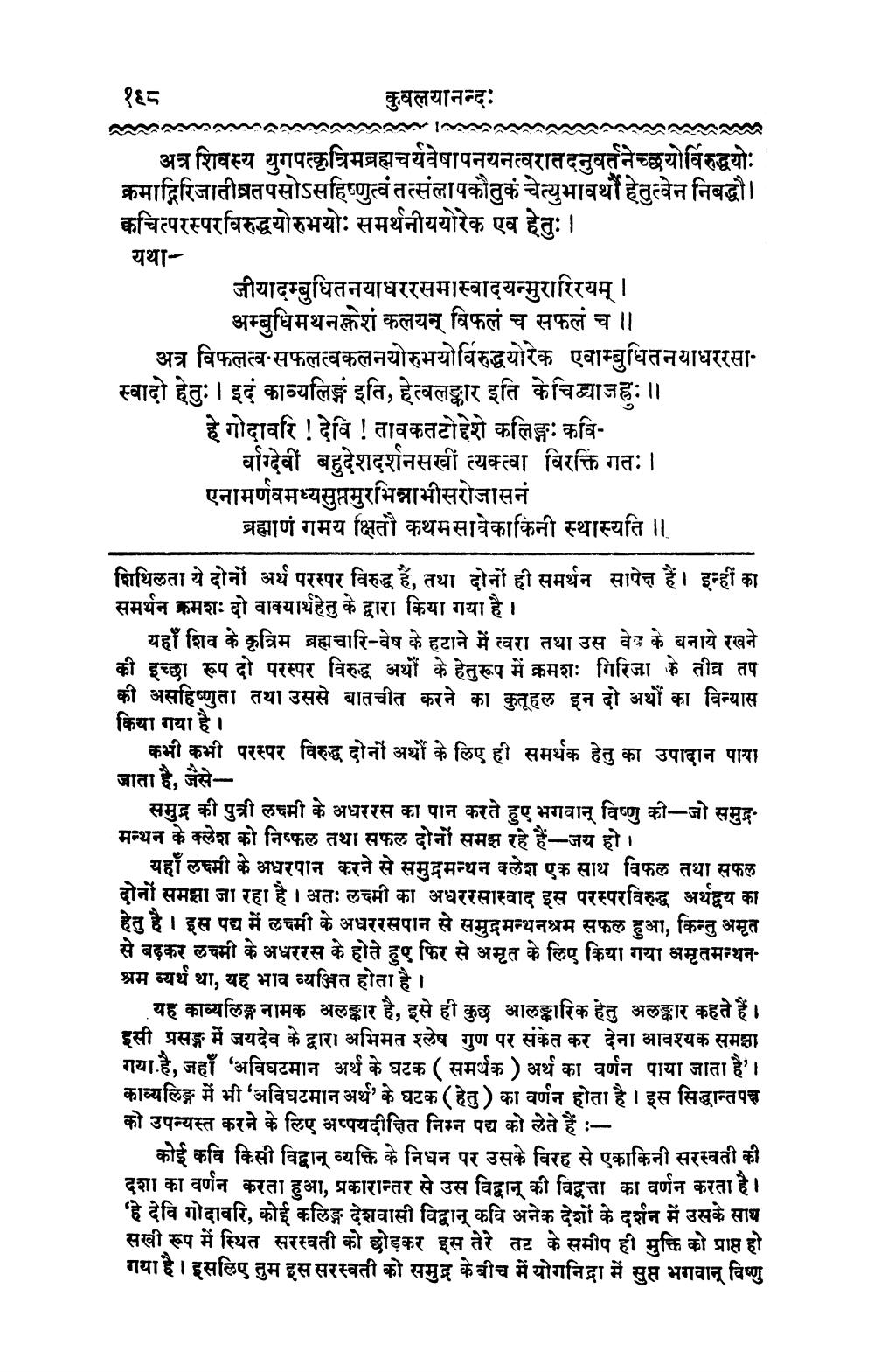________________
१६८
कुवलयानन्दः
Inv
अत्र शिवस्य युगपत्कृत्रिमब्रह्मचर्यवेषापनयनत्व तदनुवर्तनेच्छयोर्विरुद्धयोः क्रमा गिरिजा तीव्रतपसोऽसहिष्णुत्वं तत्संदा पकौतुकं चेत्युभावर्थी हेतुत्वेन निबद्धौ । क्वचित्परस्परविरुद्धयोरुभयोः समर्थनीययोरेक एव हेतुः ।
यथा
जीयादम्बुधितनयाघररसमास्वादयन्मुराश्रियम् । अम्बुधिमथनक्लेशं कलयन् विफलं च सफलं च ।।
अत्र विफलत्व·सफलत्वकलनयोरुभयोर्विरुद्धयोरेक एवाम्बुधितनयाधररसास्वादो हेतुः । इदं काव्यलिङ्गं इति, हेत्वलङ्कार इति केचिद्व्याजहुः ॥ गोदावरि ! देवि ! तावकतटोद्देशे कलिङ्गः कविर्वाग्देवीं बहुदेशदर्शनसखीं त्यक्त्वा विरक्तिं गतः । एनामर्णवमध्य सुप्तमुरभिन्नाभीसरोजासनं
ब्रह्माणं गमय क्षितौ कथमसावेकाकिनी स्थास्यति ॥
शिथिलता ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हैं, तथा दोनों ही समर्थन सापेक्ष हैं। इन्हीं का समर्थन क्रमशः दो वाक्यार्थहेतु के द्वारा किया गया है ।
यहाँ शिव के कृत्रिम ब्रह्मचारि-वेष के हटाने में खरा तथा उस वे के बनाये रखने की इच्छा रूप दो परस्पर विरुद्ध अर्थों के हेतुरूप में क्रमशः गिरिजा के तीव्र तप की असहिष्णुता तथा उससे बातचीत करने का कुतूहल इन दो अर्थों का विन्यास किया गया है।
कभी कभी परस्पर विरुद्ध दोनों अर्थों के लिए ही समर्थक हेतु का उपादान पाया जाता है, जैसे
समुद्र की पुत्री लक्ष्मी के अधररस का पान करते हुए भगवान् विष्णु की — जो समुद्रमन्थन के क्लेश को निष्फल तथा सफल दोनों समझ रहे हैं- -जय हो ।
यहाँ लक्ष्मी के अधरपान करने से समुद्रमन्थन क्लेश एक साथ विफल तथा सफल दोनों समझा जा रहा है । अतः लक्ष्मी का अधररसास्वाद इस परस्परविरुद्ध अर्थद्वय का हेतु है । इस पद्य में लक्ष्मी के अधररसपान से समुद्रमन्थनश्रम सफल हुआ, किन्तु अमृत से बढ़कर लक्ष्मी के अधररस के होते हुए फिर से अमृत के लिए किया गया अमृतमन्थनश्रम व्यर्थ था, यह भाव व्यञ्जित होता है ।
. यह काव्यलिङ्ग नामक अलङ्कार है, इसे ही कुछ आलङ्कारिक हेतु अलङ्कार कहते हैं । इसी प्रसङ्ग में जयदेव के द्वारा अभिमत श्लेष गुण पर संकेत कर देना आवश्यक समझा गया है, जहाँ 'अविघटमान अर्थ के घटक ( समर्थक ) अर्थ का वर्णन पाया जाता है'। rator oङ्ग में भी 'अविघटमान अर्थ' के घटक (हेतु) का वर्णन होता है । इस सिद्धान्तप को उपन्यस्त करने के लिए अप्पयदीक्षित निम्न पद्य को लेते हैं।
:
कोई कवि किसी विद्वान् व्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती की दशा का वर्णन करता हुआ, प्रकारान्तर से उस विद्वान् की विद्वत्ता का वर्णन करता है । 'हे देवि गोदावरि, कोई कलिङ्ग देशवासी विद्वान् कवि अनेक देशों के दर्शन में उसके साथ सखी रूप में स्थित सरस्वती को छोड़कर इस तेरे तट के समीप ही मुक्ति को प्राप्त हो गया है । इसलिए तुम इस सरस्वती को समुद्र के बीच में योगनिद्रा में सुप्त भगवान् विष्णु