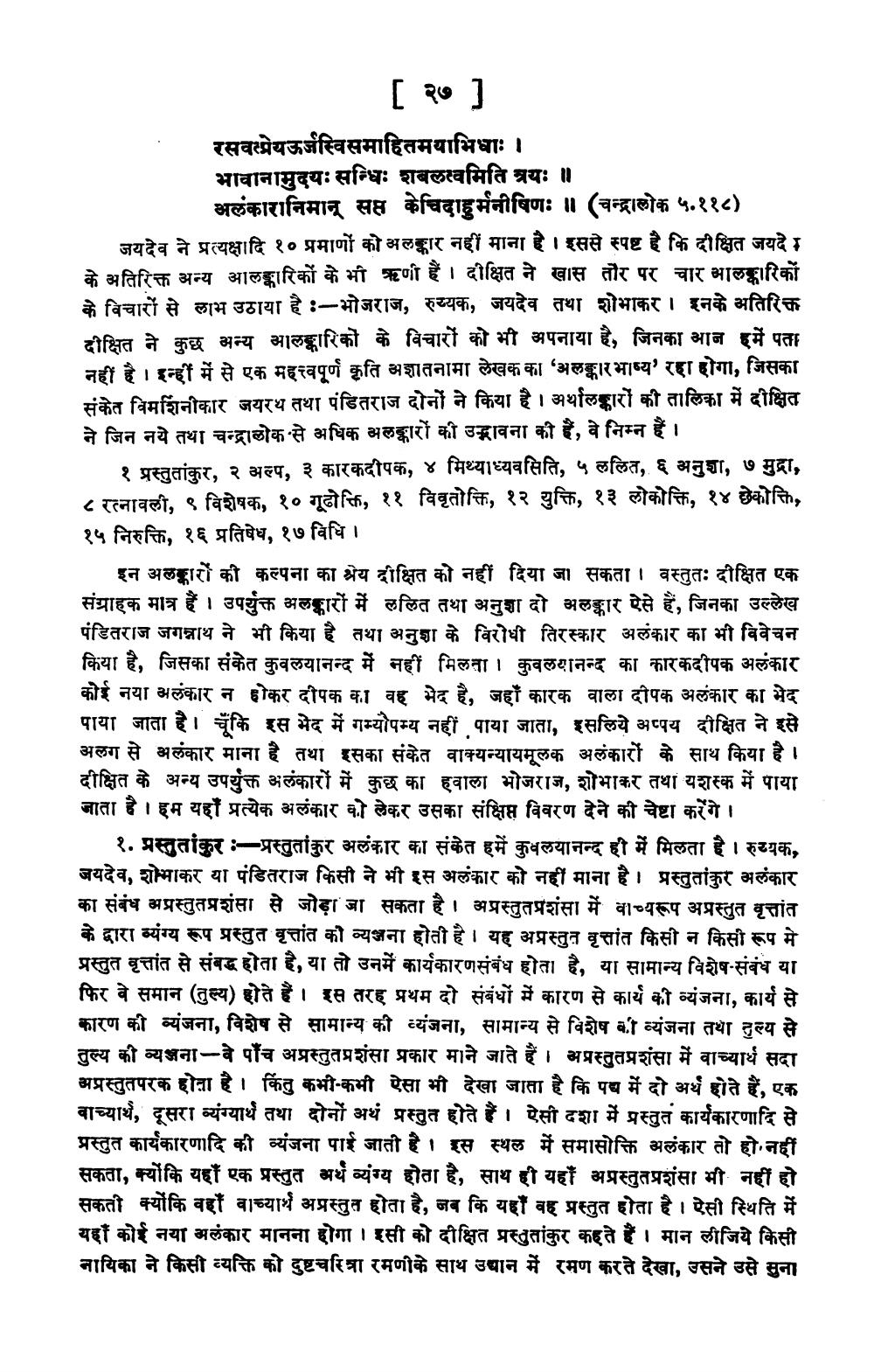________________
[२७]
रसवत्प्रेयऊर्जस्विसमाहितमयाभिधाः ।
भावानामुदयः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः ॥
अलंकारानिमान् सप्त केचिदाहुर्मनीषिणः ॥ (चन्द्रालोक ५.११८)
जयदेव ने प्रत्यक्षादि १० प्रमाणों को अलङ्कार नहीं माना है। इससे स्पष्ट है कि दीक्षित जयदे के अतिरिक्त अन्य आलङ्कारिकों के भी ऋणी हैं। दीक्षित ने खास तौर पर चार आलङ्कारिकों के विचारों से लाभ उठाया है :- भोजराज, रुय्यक, जयदेव तथा शोभाकर । इनके अतिरिक्त दीक्षित ने कुछ अन्य आलङ्कारिकों के विचारों को भी अपनाया है, जिनका आन हमें पता नहीं है । इन्हीं में से एक महत्त्वपूर्ण कृति अज्ञातनामा लेखक का 'अलङ्कार भाष्य' रहा होगा, जिसका संकेत विमर्शिनीकार जयरथ तथा पंडितराज दोनों ने किया है । अर्थालङ्कारों की तालिका में दीक्षित ने जिन नये तथा चन्द्रालोक से अधिक अलङ्कारों की उद्भावना की हैं, वे निम्न हैं ।
१ प्रस्तुतांकुर, २ अल्प, ३ कारकदीपक, ४ मिथ्याध्यवसिति, ५ ललित, ६ अनुज्ञा, ७ मुद्रा, ८ रत्नावली, ९ विशेषक, १० गूढोक्ति, ११ विवृतोक्ति, १२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, १४ छेकोक्ति, १५ निरुक्ति, १६ प्रतिषेध, १७ विधि ।
इन अलङ्कारों की कल्पना का श्रेय दीक्षित को नहीं दिया जा सकता । वस्तुतः दीक्षित एक संग्राहक मात्र हैं । उपर्युक्त अलङ्कारों में ललित तथा अनुशा दो अलङ्कार ऐसे हैं, जिनका उल्लेख पंडितराज जगन्नाथ ने भी किया है तथा अनुज्ञा के विरोधी तिरस्कार अलंकार का भी विवेचन किया है, जिसका संकेत कुवलयानन्द में नहीं मिलता । कुवलयानन्द का कारकदीपक अलंकार कोई नया अलंकार न होकर दीपक का वह भेद है, जहाँ कारक वाला दीपक अलंकार का भेद पाया जाता है। चूँकि इस भेद में गम्यौपम्य नहीं पाया जाता, इसलिये अप्पय दीक्षित ने इसे अलग से अलंकार माना है तथा इसका संकेत वाक्यन्यायमूलक अलंकारों के साथ किया है । दीक्षित के अन्य उपर्युक्त अलंकारों में कुछ का हवाला भोजराज, शोभाकर तथा यशस्क में पाया जाता है । हम यहाँ प्रत्येक अलंकार को लेकर उसका संक्षिप्त विवरण देने की चेष्टा करेंगे ।
१. प्रस्तुतांकुर : - प्रस्तुतांकुर अलंकार का संकेत हमें कुवलयानन्द ही में मिलता है । रुय्यक, जयदेव, शोभाकर या पंडितराज किसी ने भी इस अलंकार को नहीं माना है। प्रस्तुतांकुर अलंकार का संबंध अप्रस्तुतप्रशंसा से जोड़ा जा सकता है । अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यरूप अप्रस्तुत वृत्तांत के द्वारा व्यंग्य रूप प्रस्तुत वृत्तांत को व्यञ्जना होती है । यह अप्रस्तुत वृत्तांत किसी न किसी रूप मे प्रस्तुत वृत्तांत से संबद्ध होता है, या तो उनमें कार्यकारणसंबंध होता है, या सामान्य विशेष संबंध या फिर वे समान (तुल्य) होते हैं । इस तरह प्रथम दो संबंधों में कारण से कार्य की व्यंजना, कार्य से कारण की व्यंजना, विशेष से सामान्य की व्यंजना, सामान्य से विशेष की व्यंजना तथा तुल्य से तुल्य की व्यञ्जना - वे पाँच अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकार माने जाते हैं । अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थं सदा अप्रस्तुतपरक होता है। किंतु कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है पद्य में दो अर्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ दूसरा व्यंग्यार्थं तथा दोनों अथं प्रस्तुत होते हैं। ऐसी दशा में प्रस्तुत कार्यकारणादि से प्रस्तुत कार्यकारणादि की व्यंजना पाई जाती है। इस स्थल में समासोक्ति अलंकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य होता है, साथ ही यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा भी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ वाच्यार्थ अप्रस्तुत होता है, जब कि यहाँ वह प्रस्तुत होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ कोई नया अलंकार मानना होगा । इसी को दीक्षित प्रस्तुतांकुर कहते हैं। मान लीजिये किसी नायिका ने किसी व्यक्ति को दुष्टचरित्रा रमणीके साथ उद्यान में रमण करते देखा, उसने उसे सुना