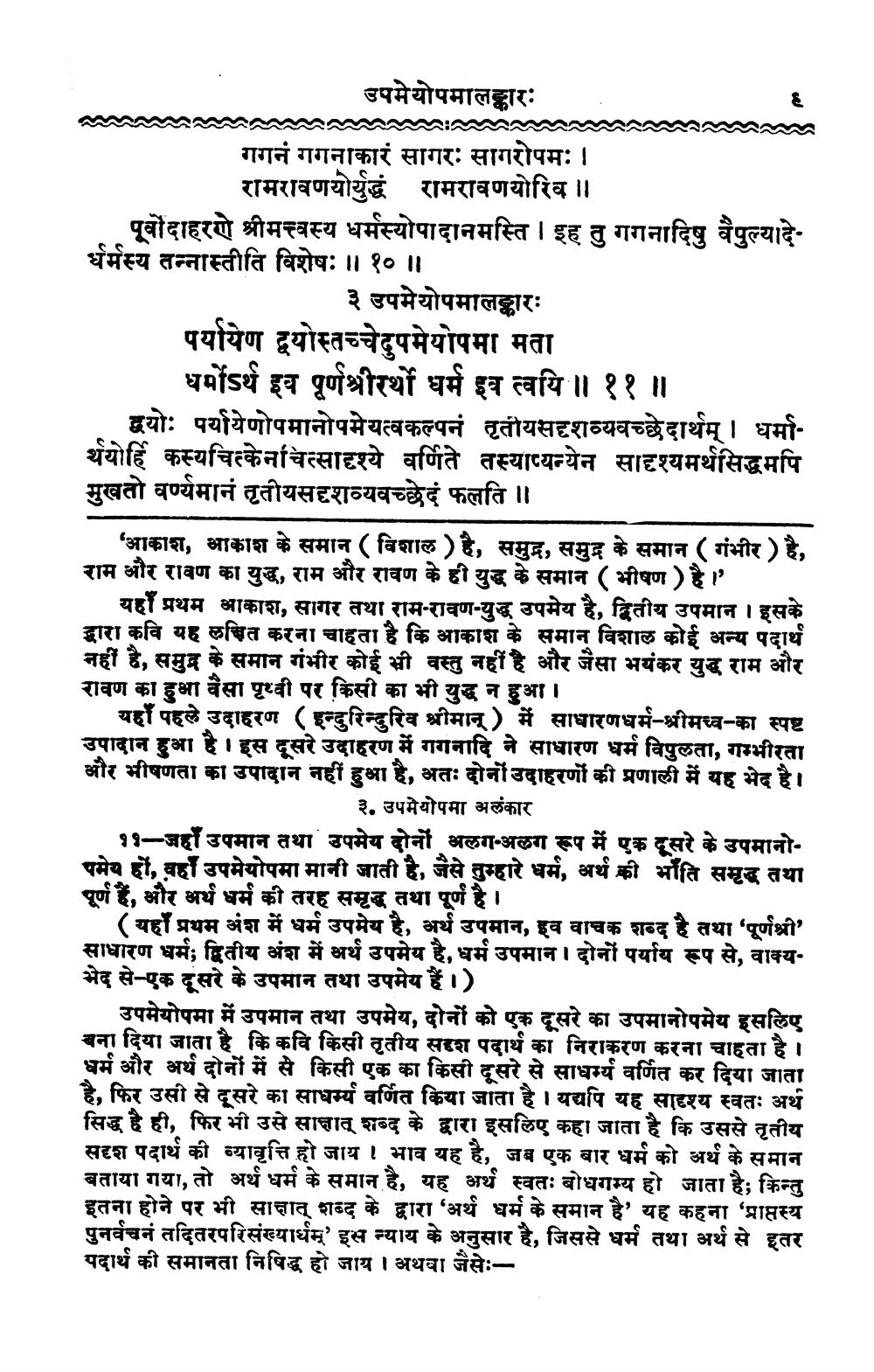________________
उपमेयोपमालङ्कारः
-
-
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ।
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ।। पूर्वोदाहरणे श्रीमत्त्वस्य धर्मस्योपादानमस्ति | इह तु गगनादिषु वैपुल्यादे. धर्मस्य तन्नास्तीति विशेषः ।। १० ॥
३ उपमेयोपमालङ्कारः पर्यायेण द्वयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता
धर्मोऽर्थ इव पूर्णश्रीरर्थो धर्म इव त्वयि ॥ ११ ॥ द्वयोः पर्यायेणोपमानोपमेयत्वकल्पनं तृतीयसदृशव्यवच्छेदार्थम् | धर्माः र्थयोहि कस्यचित्केनचित्सादृश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन सादृश्यमर्थसिद्धमपि मुखतो वर्ण्यमानं तृतीयसदृशव्यवच्छेदं फलति ॥
'आकाश, आकाश के समान (विशाल) है, समुद्र, समुद्र के समान (गंभीर) है, राम और रावण का युद्ध, राम और रावण के ही युद्ध के समान (भीषण) है।'
यहाँ प्रथम आकाश, सागर तथा राम-रावण-युद्ध उपमेय है, द्वितीय उपमान । इसके द्वारा कवि यह लक्षित करना चाहता है कि आकाश के समान विशाल कोई अन्य पदार्थ नहीं है, समुद्र के समान गंभीर कोई भी वस्तु नहीं है और जैसा भयंकर युद्ध राम और रावण का हुभा वैसा पृथ्वी पर किसी का भी युद्ध न हुआ। ___ यहाँ पहले उदाहरण (इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान् ) में साधारणधर्म-श्रीमच्व-का स्पष्ट उपादान हुआ है। इस दूसरे उदाहरण में गगनादि ने साधारण धर्म विपुलता, गम्भीरता और भीषणता का उपादान नहीं हुआ है, अतः दोनों उदाहरणों की प्रणाली में यह भेद है।
३. उपमेयोपमा अलंकार ११-जहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों अलग-अलग रूप में एक दूसरे के उपमानो. पमेय हो, वहाँ उपमेयोपमा मानी जाती है, जैसे तुम्हारे धर्म, अर्थ की भांति समृद्ध तथा पूर्ण हैं, और अर्थ धर्म की तरह समृद्ध तथा पूर्ण है।
(यहाँ प्रथम अंश में धर्म उपमेय है, अर्थ उपमान, इव वाचक शब्द है तथा 'पूर्णश्री' साधारण धर्म; द्वितीय अंश में अर्थ उपमेय है, धर्म उपमान । दोनों पर्याय रूप से, वाक्य. भेद से-एक दूसरे के उपमान तथा उपमेय हैं।)
उपमेयोपमा में उपमान तथा उपमेय, दोनों को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसलिए बना दिया जाता है कि कवि किसी तृतीय सहश पदार्थ का निराकरण करना चाहता है। धर्म और अर्थ दोनों में से किसी एक का किसी दूसरे से साधर्म्य वर्णित कर दिया जाता है, फिर उसी से दूसरे का साधर्म्य वर्णित किया जाता है । यद्यपि यह सादृश्य स्वतः अर्थ सिद्ध है ही, फिर भी उसे साक्षात् शब्द के द्वारा इसलिए कहा जाता है कि उससे तृतीय सदृश पदार्थ की व्यावृत्ति हो जाय । भाव यह है, जब एक बार धर्म को अर्थ के समान बताया गया, तो अर्थ धर्म के समान है, यह अर्थ स्वतः बोधगम्य हो जाता है। किन्तु इतना होने पर भी साक्षात् शब्द के द्वारा 'अर्थ धर्म के समान है' यह कहना 'प्राप्तस्य पुनर्वचनं तदितरपरिसंख्यार्धम्' इस न्याय के अनुसार है, जिससे धर्म तथा अर्थ से इतर पदार्थ की समानता निषिद्ध हो जाय । अथवा जैसे: