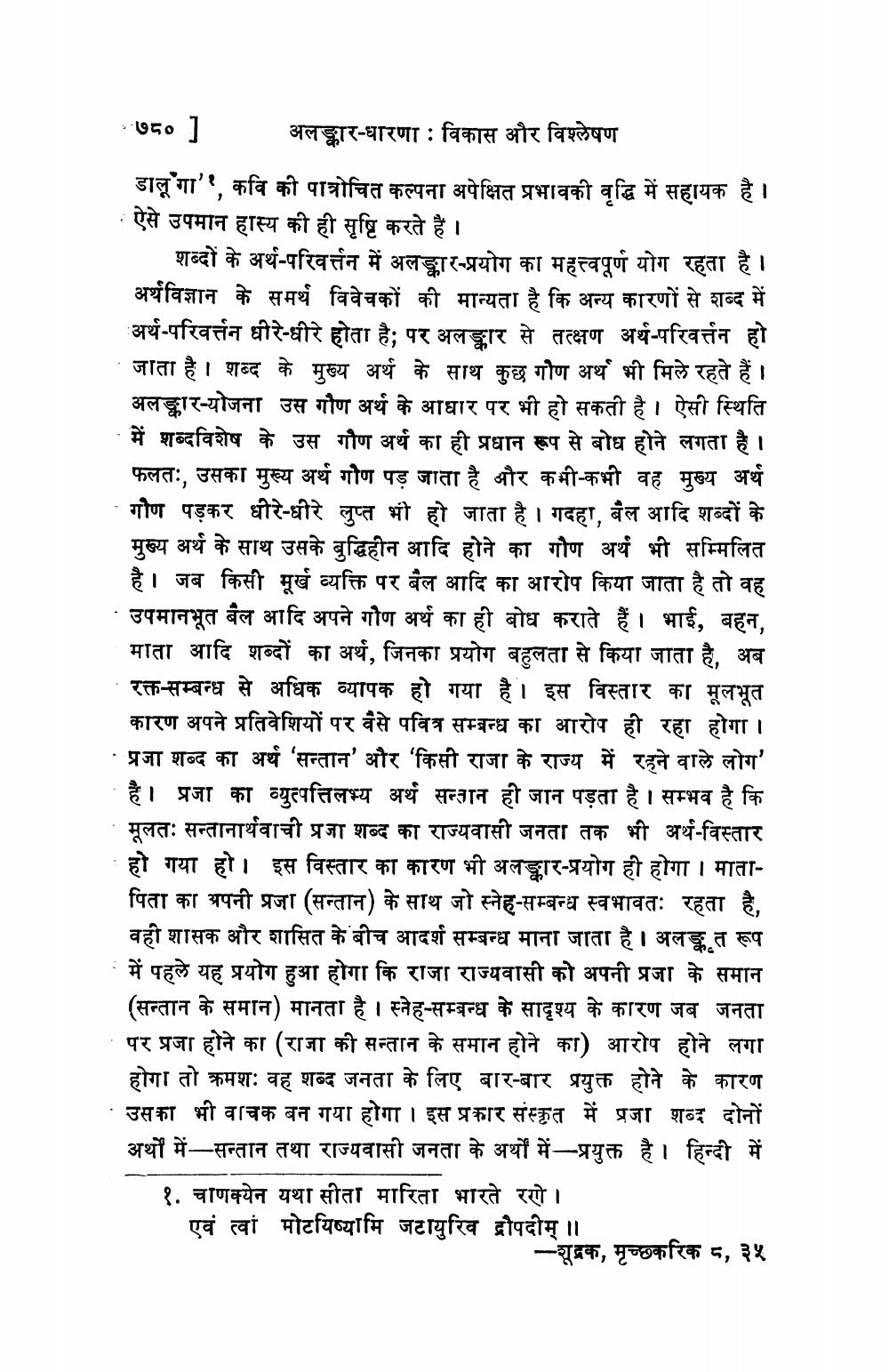________________
• ७८० ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण डालूगा'१. कवि की पात्रोचित कल्पना अपेक्षित प्रभावकी वृद्धि में सहायक है। ऐसे उपमान हास्य की ही सृष्टि करते हैं।
__ शब्दों के अर्थ-परिवर्तन में अलङ्कार-प्रयोग का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। अर्थविज्ञान के समर्थ विवेचकों की मान्यता है कि अन्य कारणों से शब्द में अर्थ-परिवर्तन धीरे-धीरे होता है; पर अलङ्कार से तत्क्षण अर्थ-परिवर्तन हो · जाता है। शब्द के मुख्य अर्थ के साथ कुछ गौण अर्थ भी मिले रहते हैं।
अलङ्कार-योजना उस गौण अर्थ के आधार पर भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में शब्दविशेष के उस गौण अर्थ का ही प्रधान रूप से बोध होने लगता है । फलतः, उसका मुख्य अर्थ गौण पड़ जाता है और कभी-कभी वह मुख्य अर्थ गौण पड़कर धीरे-धीरे लुप्त भी हो जाता है। गदहा, बैल आदि शब्दों के मुख्य अर्थ के साथ उसके बुद्धिहीन आदि होने का गौण अर्थ भी सम्मिलित है। जब किसी मूर्ख व्यक्ति पर बैल आदि का आरोप किया जाता है तो वह · उपमानभूत बैल आदि अपने गौण अर्थ का ही बोध कराते हैं। भाई, बहन, माता आदि शब्दों का अर्थ, जिनका प्रयोग बहुलता से किया जाता है, अब रक्त-सम्बन्ध से अधिक व्यापक हो गया है। इस विस्तार का मूलभूत कारण अपने प्रतिवेशियों पर वैसे पवित्र सम्बन्ध का आरोप ही रहा होगा। प्रजा शब्द का अर्थ 'सन्तान' और 'किसी राजा के राज्य में रहने वाले लोग' है। प्रजा का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ सन्तान ही जान पड़ता है । सम्भव है कि मूलतः सन्तानार्थवाची प्रजा शब्द का राज्यवासी जनता तक भी अर्थ-विस्तार हो गया हो। इस विस्तार का कारण भी अलङ्कार-प्रयोग ही होगा । मातापिता का अपनी प्रजा (सन्तान) के साथ जो स्नेह-सम्बन्ध स्वभावतः रहता है, वही शासक और शासित के बीच आदर्श सम्बन्ध माना जाता है । अलङ्क त रूप में पहले यह प्रयोग हुआ होगा कि राजा राज्यवासी को अपनी प्रजा के समान (सन्तान के समान) मानता है । स्नेह-सम्बन्ध के सादृश्य के कारण जब जनता · पर प्रजा होने का (राजा की सन्तान के समान होने का आरोप होने लगा होगा तो क्रमशः वह शब्द जनता के लिए बार-बार प्रयुक्त होने के कारण उसका भी वाचक बन गया होगा। इस प्रकार संस्कृत में प्रजा शब्द दोनों अर्थों में—सन्तान तथा राज्यवासी जनता के अर्थों में प्रयुक्त है। हिन्दी में १. चाणक्येन यथा सीता मारिता भारते रणे। एवं त्वां मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम् ॥
-शूद्रक, मृच्छकरिक ८, ३५