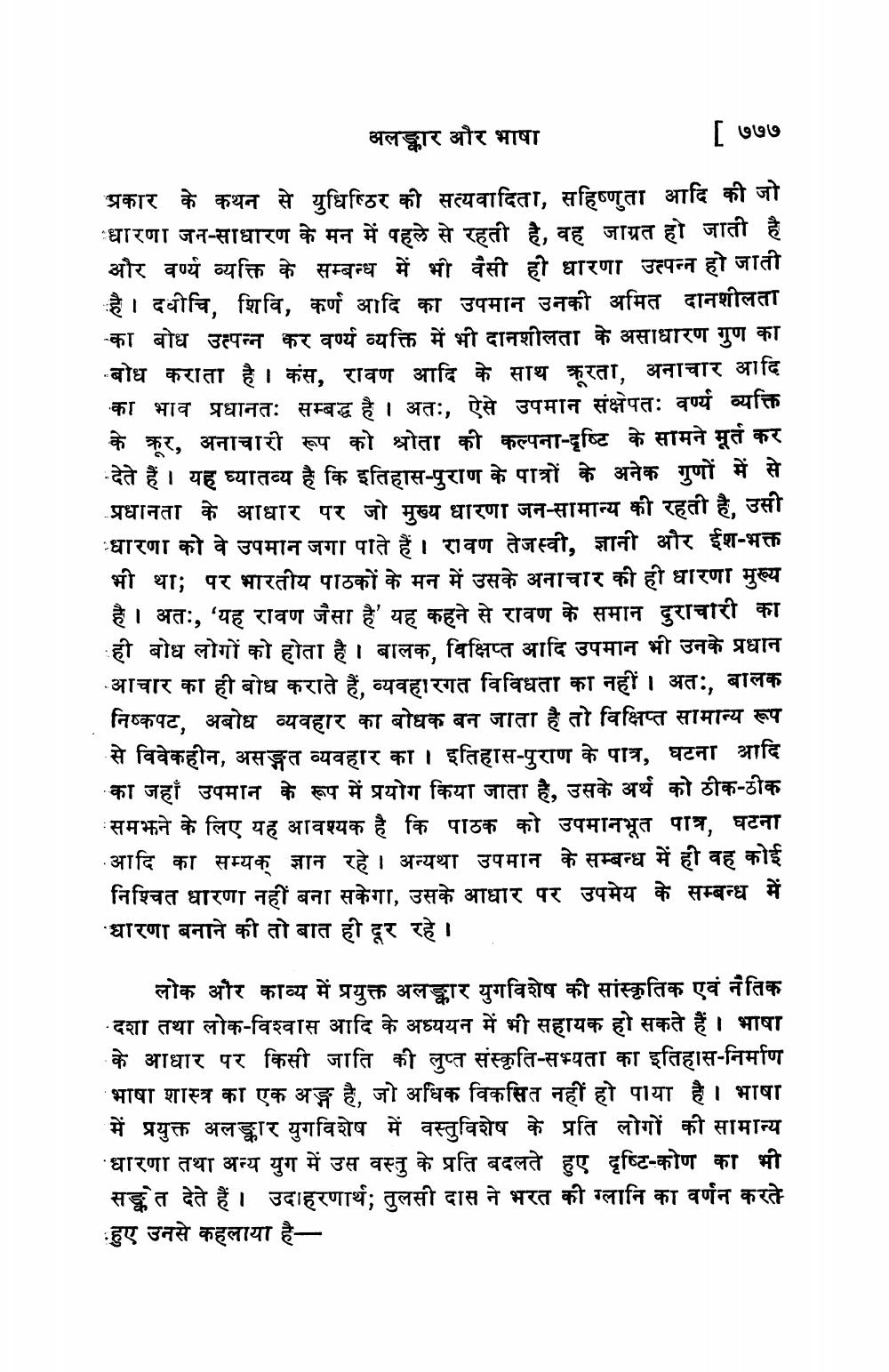________________
अलङ्कार और भाषा
[ ७७७
प्रकार के कथन से युधिष्ठिर की सत्यवादिता, सहिष्णुता आदि की जो धारणा जन-साधारण के मन में पहले से रहती है, वह जाग्रत हो जाती है और वर्ण्य व्यक्ति के सम्बन्ध में भी वैसी ही धारणा उत्पन्न हो जाती है। दधीचि, शिवि, कर्ण आदि का उपमान उनकी अमित दानशीलता का बोध उत्पन्न कर वर्ण्य व्यक्ति में भी दानशीलता के असाधारण गुण का बोध कराता है। कंस, रावण आदि के साथ क्रूरता, अनाचार आदि का भाव प्रधानतः सम्बद्ध है । अतः, ऐसे उपमान संक्षेपतः वर्ण्य व्यक्ति के क्रूर, अनाचारी रूप को श्रोता की कल्पना-दृष्टि के सामने मूर्त कर देते हैं। यह ध्यातव्य है कि इतिहास-पुराण के पात्रों के अनेक गुणों में से प्रधानता के आधार पर जो मुख्य धारणा जन-सामान्य की रहती है, उसी धारणा को वे उपमान जगा पाते हैं। रावण तेजस्वी, ज्ञानी और ईश-भक्त भी था; पर भारतीय पाठकों के मन में उसके अनाचार की ही धारणा मुख्य है। अतः, 'यह रावण जैसा है' यह कहने से रावण के समान दुराचारी का ही बोध लोगों को होता है। बालक, विक्षिप्त आदि उपमान भी उनके प्रधान आचार का ही बोध कराते हैं, व्यवहारगत विविधता का नहीं। अतः, बालक निष्कपट, अबोध व्यवहार का बोधक बन जाता है तो विक्षिप्त सामान्य रूप से विवेकहीन, असङ्गत व्यवहार का। इतिहास-पुराण के पात्र, घटना आदि का जहाँ उपमान के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ को ठीक-ठीक समझने के लिए यह आवश्यक है कि पाठक को उपमानभूत पात्र, घटना आदि का सम्यक् ज्ञान रहे। अन्यथा उपमान के सम्बन्ध में ही वह कोई निश्चित धारणा नहीं बना सकेगा, उसके आधार पर उपमेय के सम्बन्ध में 'धारणा बनाने की तो बात ही दूर रहे।
लोक और काव्य में प्रयुक्त अलङ्कार युगविशेष की सांस्कृतिक एवं नैतिक ‘दशा तथा लोक-विश्वास आदि के अध्ययन में भी सहायक हो सकते हैं। भाषा के आधार पर किसी जाति की लुप्त संस्कृति-सभ्यता का इतिहास-निर्माण भाषा शास्त्र का एक अङ्ग है, जो अधिक विकसित नहीं हो पाया है। भाषा में प्रयुक्त अलङ्कार युगविशेष में वस्तुविशेष के प्रति लोगों की सामान्य धारणा तथा अन्य युग में उस वस्तु के प्रति बदलते हुए दृष्टि-कोण का भी सङ्कत देते हैं। उदाहरणार्थ; तुलसी दास ने भरत की ग्लानि का वर्णन करते हुए उनसे कहलाया है