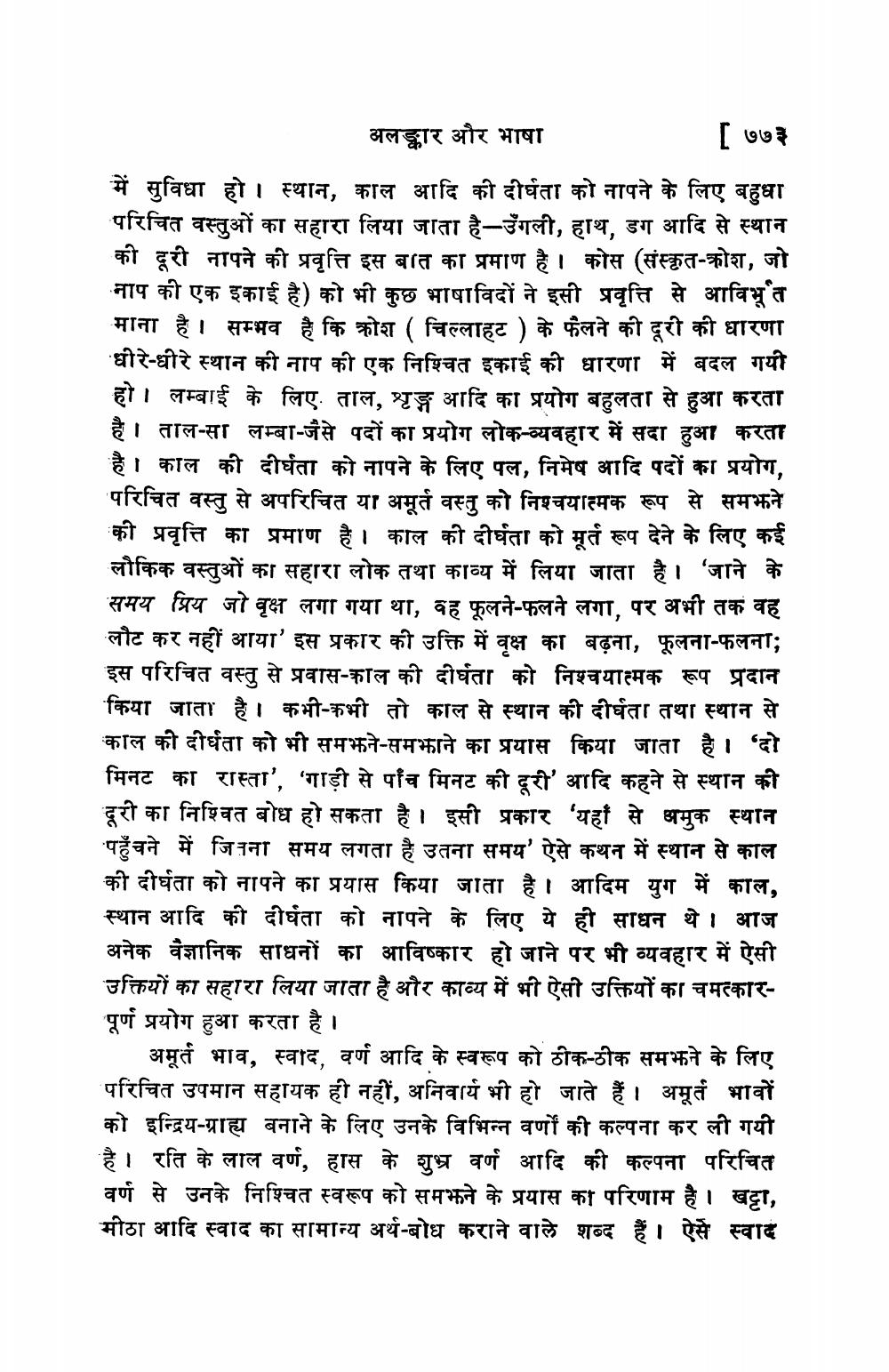________________
अलङ्कार और भाषा
[७७३
में सुविधा हो। स्थान, काल आदि की दीर्घता को नापने के लिए बहुधा परिचित वस्तुओं का सहारा लिया जाता है-उँगली, हाथ, डग आदि से स्थान की दूरी नापने की प्रवृत्ति इस बात का प्रमाण है। कोस (संस्कृत-क्रोश, जो नाप की एक इकाई है) को भी कुछ भाषाविदों ने इसी प्रवृत्ति से आविर्भूत माना है। सम्भव है कि क्रोश ( चिल्लाहट ) के फैलने की दूरी की धारणा धीरे-धीरे स्थान की नाप की एक निश्चित इकाई की धारणा में बदल गयी हो। लम्बाई के लिए. ताल, शृङ्ग आदि का प्रयोग बहुलता से हुआ करता है। ताल-सा लम्बा-जैसे पदों का प्रयोग लोक-व्यवहार में सदा हुआ करता है। काल की दीर्घता को नापने के लिए पल, निमेष आदि पदों का प्रयोग, परिचित वस्तु से अपरिचित या अमूर्त वस्तु को निश्चयात्मक रूप से समझने की प्रवृत्ति का प्रमाण है। काल की दीर्घता को मूर्त रूप देने के लिए कई लौकिक वस्तुओं का सहारा लोक तथा काव्य में लिया जाता है। 'जाने के समय प्रिय जो वृक्ष लगा गया था, वह फूलने-फलने लगा, पर अभी तक वह लौट कर नहीं आया' इस प्रकार की उक्ति में वृक्ष का बढ़ना, फूलना-फलना; इस परिचित वस्तु से प्रवास-काल की दीर्घता को निश्चयात्मक रूप प्रदान किया जाता है। कभी-कभी तो काल से स्थान की दीर्घता तथा स्थान से काल की दीर्घता को भी समझने-समझाने का प्रयास किया जाता है। 'दो मिनट का रास्ता', 'गाड़ी से पांच मिनट की दूरी' आदि कहने से स्थान की दूरी का निश्चित बोध हो सकता है। इसी प्रकार 'यहाँ से अमुक स्थान पहुँचने में जितना समय लगता है उतना समय' ऐसे कथन में स्थान से काल की दीर्घता को नापने का प्रयास किया जाता है। आदिम युग में काल, स्थान आदि की दीर्घता को नापने के लिए ये ही साधन थे। आज अनेक वैज्ञानिक साधनों का आविष्कार हो जाने पर भी व्यवहार में ऐसी उक्तियों का सहारा लिया जाता है और काव्य में भी ऐसी उक्तियों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ करता है। ___अमूर्त भाव, स्वाद, वर्ण आदि के स्वरूप को ठीक-ठीक समझने के लिए परिचित उपमान सहायक ही नहीं, अनिवार्य भी हो जाते हैं। अमूर्त भावों को इन्द्रिय-ग्राह्य बनाने के लिए उनके विभिन्न वर्गों की कल्पना कर ली गयी है। रति के लाल वर्ण, हास के शुभ्र वर्ण आदि की कल्पना परिचित वर्ण से उनके निश्चित स्वरूप को समझने के प्रयास का परिणाम है। खट्टा, मीठा आदि स्वाद का सामान्य अर्थ-बोध कराने वाले शब्द हैं। ऐसे स्वाद