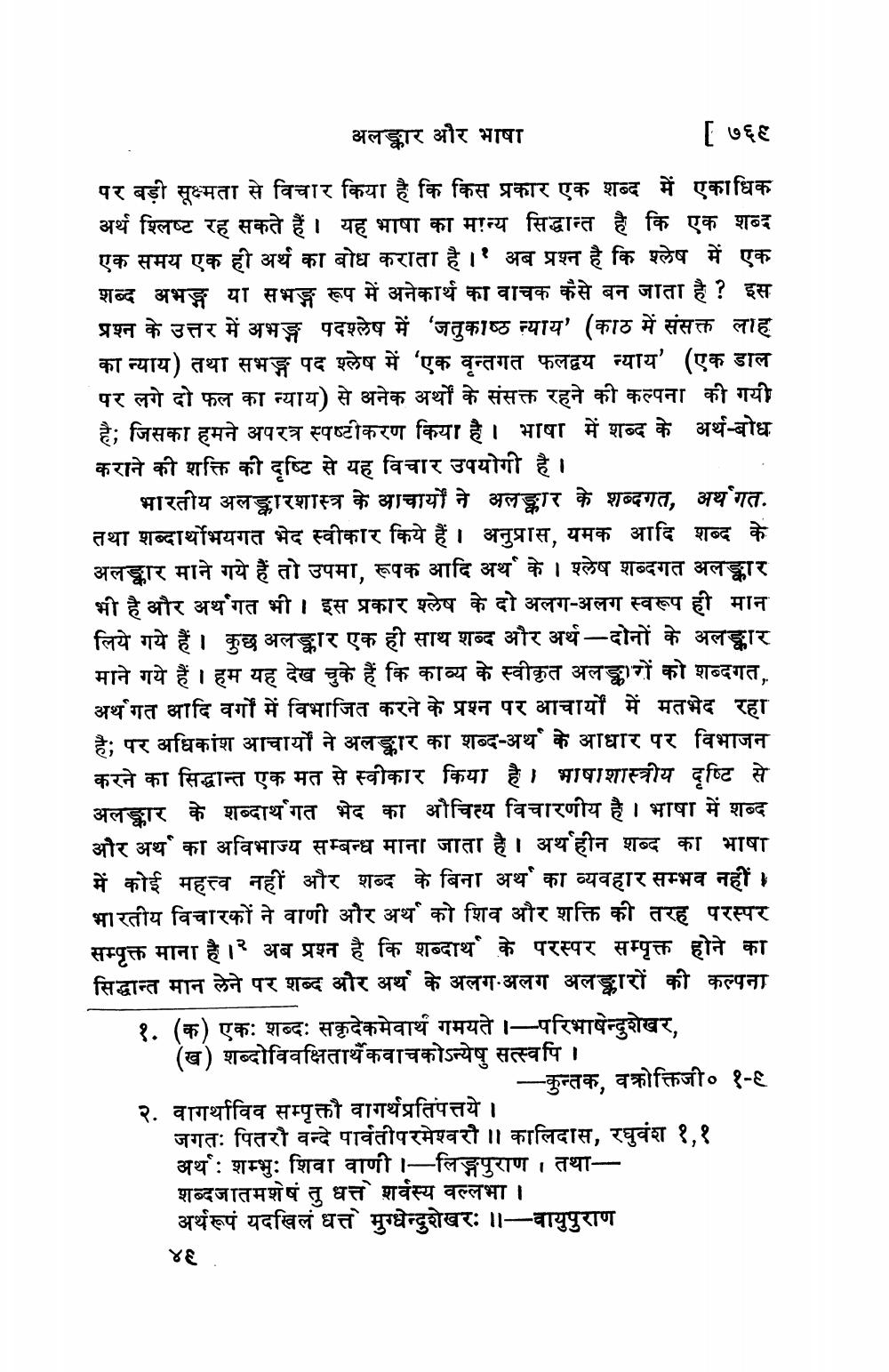________________
अलङ्कार और भाषा
[ ७६६
पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है कि किस प्रकार एक शब्द में एकाधिक अर्थ श्लिष्ट रह सकते हैं । यह भाषा का मान्य सिद्धान्त है कि एक शब्द एक समय एक ही अर्थ का बोध कराता है । अब प्रश्न है कि श्लेष में एक शब्द अभङ्ग या सभङ्ग रूप में अनेकार्थ का वाचक कैसे बन जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में अभङ्ग पदश्लेष में 'जतुकाष्ठ न्याय' (काठ में संसक्त लाह का न्याय) तथा सभङ्ग पद श्लेष में 'एक वृन्तगत फलद्वय न्याय' (एक डाल पर लगे दो फल का न्याय) से अनेक अर्थों के संसक्त रहने की कल्पना की गयी है; जिसका हमने अपरत्र स्पष्टीकरण किया है । भाषा में शब्द के अर्थ- बोध कराने की शक्ति की दृष्टि से यह विचार उपयोगी है ।
भारतीय अलङ्कारशास्त्र के आचार्यों ने अलङ्कार के शब्दगत, अर्थं गत. तथा शब्दार्थोभयगत भेद स्वीकार किये हैं । अनुप्रास, यमक आदि शब्द के अलङ्कार माने गये हैं तो उपमा, रूपक आदि अर्थ के । श्लेष शब्दगत अलङ्कार भी है और अर्थगत भी । इस प्रकार श्लेष के दो अलग-अलग स्वरूप ही मान लिये गये हैं । कुछ अलङ्कार एक ही साथ शब्द और अर्थ - दोनों के अलङ्कार माने गये हैं । हम यह देख चुके हैं कि काव्य के स्वीकृत अलङ्कारों को शब्दगत, अर्थ आदि वर्गों में विभाजित करने के प्रश्न पर आचार्यों में मतभेद रहा है; पर अधिकांश आचार्यों ने अलङ्कार का शब्द अर्थ के आधार पर विभाजन करने का सिद्धान्त एक मत से स्वीकार किया है । भाषाशास्त्रीय दृष्टि से अलङ्कार के शब्दार्थगत भेद का औचित्य विचारणीय है । भाषा में शब्द और अर्थ का अविभाज्य सम्बन्ध माना जाता है । अर्थहीन शब्द का भाषा में कोई महत्त्व नहीं और शब्द के बिना अर्थ का व्यवहार सम्भव नहीं । भारतीय विचारकों ने वाणी और अर्थ को शिव और शक्ति की तरह परस्पर सम्पृक्त माना है । अब प्रश्न है कि शब्दार्थ के परस्पर सम्पृक्त होने का सिद्धान्त मान लेने पर शब्द और अर्थ के अलग- अलग अलङ्कारों की कल्पना
१. (क) एकः शब्दः सकृदेकमेवार्थं गमयते । - परिभाषेन्दुशेखर, (ख) शब्दोविवक्षितार्थं कवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि ।
—कुन्तक, वक्रोक्तिजी ० ०१-६
२. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥ कालिदास, रघुवंश १, १ अर्थ : शम्भुः शिवा वाणी । - - लिङ्गपुराण । तथाशब्दजातमशेषं तु धत्त े शर्वस्य वल्लभा । अर्थरूपं यदखिलं धत्तं मुग्धेन्दुशेखरः ॥ - वायुपुराण
४६