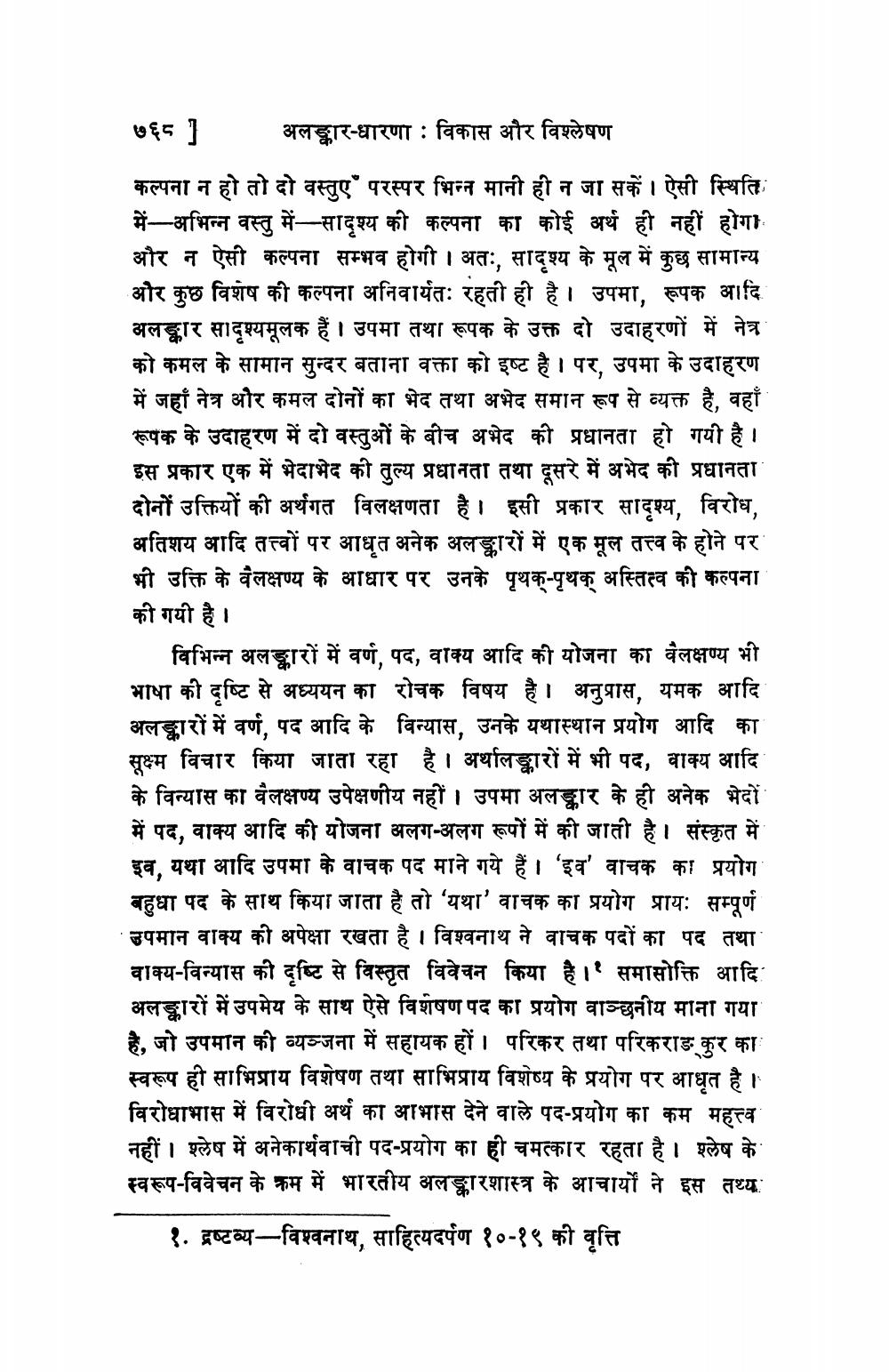________________
७६८ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण कल्पना न हो तो दो वस्तुएं परस्पर भिन्न मानी ही न जा सकें । ऐसी स्थिति में अभिन्न वस्तु में—सादृश्य की कल्पना का कोई अर्थ ही नहीं होगा और न ऐसी कल्पना सम्भव होगी। अतः, सादृश्य के मूल में कुछ सामान्य और कुछ विशेष की कल्पना अनिवार्यतः रहती ही है। उपमा, रूपक आदि अलङ्कार सादृश्यमूलक हैं । उपमा तथा रूपक के उक्त दो उदाहरणों में नेत्र को कमल के सामान सुन्दर बताना वक्ता को इष्ट है। पर, उपमा के उदाहरण में जहाँ नेत्र और कमल दोनों का भेद तथा अभेद समान रूप से व्यक्त है, वहाँ रूपक के उदाहरण में दो वस्तुओं के बीच अभेद की प्रधानता हो गयी है। इस प्रकार एक में भेदाभेद की तुल्य प्रधानता तथा दूसरे में अभेद की प्रधानता दोनों उक्तियों की अर्थगत विलक्षणता है। इसी प्रकार सादृश्य, विरोध, अतिशय आदि तत्त्वों पर आधृत अनेक अलङ्कारों में एक मूल तत्त्व के होने पर भी उक्ति के लक्षण्य के आधार पर उनके पृथक्-पृथक् अस्तित्व की कल्पना की गयी है।
विभिन्न अलङ्कारों में वर्ण, पद, वाक्य आदि की योजना का वैलक्षण्य भी भाषा की दृष्टि से अध्ययन का रोचक विषय है। अनुप्रास, यमक आदि अलङ्कारों में वर्ण, पद आदि के विन्यास, उनके यथास्थान प्रयोग आदि का सूक्ष्म विचार किया जाता रहा है। अर्थालङ्कारों में भी पद, वाक्य आदि के विन्यास का वैलक्षण्य उपेक्षणीय नहीं। उपमा अलङ्कार के ही अनेक भेदों में पद, वाक्य आदि की योजना अलग-अलग रूपों में की जाती है। संस्कृत में इव, यथा आदि उपमा के वाचक पद माने गये हैं। 'इव' वाचक का प्रयोग बहुधा पद के साथ किया जाता है तो 'यथा' वाचक का प्रयोग प्रायः सम्पूर्ण 'उपमान वाक्य की अपेक्षा रखता है । विश्वनाथ ने वाचक पदों का पद तथा वाक्य-विन्यास की दृष्टि से विस्तृत विवेचन किया है।' समासोक्ति आदि अलङ्कारों में उपमेय के साथ ऐसे विशेषण पद का प्रयोग वाञ्छनीय माना गया है, जो उपमान की व्यञ्जना में सहायक हों। परिकर तथा परिकराङ कुर का स्वरूप ही साभिप्राय विशेषण तथा साभिप्राय विशेष्य के प्रयोग पर आधृत है। विरोधाभास में विरोधी अर्थ का आभास देने वाले पद-प्रयोग का कम महत्त्व नहीं। श्लेष में अनेकार्थवाची पद-प्रयोग का ही चमत्कार रहता है। श्लेष के स्वरूप-विवेचन के क्रम में भारतीय अलङ्कारशास्त्र के आचार्यों ने इस तथ्यः
१. द्रष्टव्य-विश्वनाथ, साहित्यदर्पण १०-१९ की वृत्ति