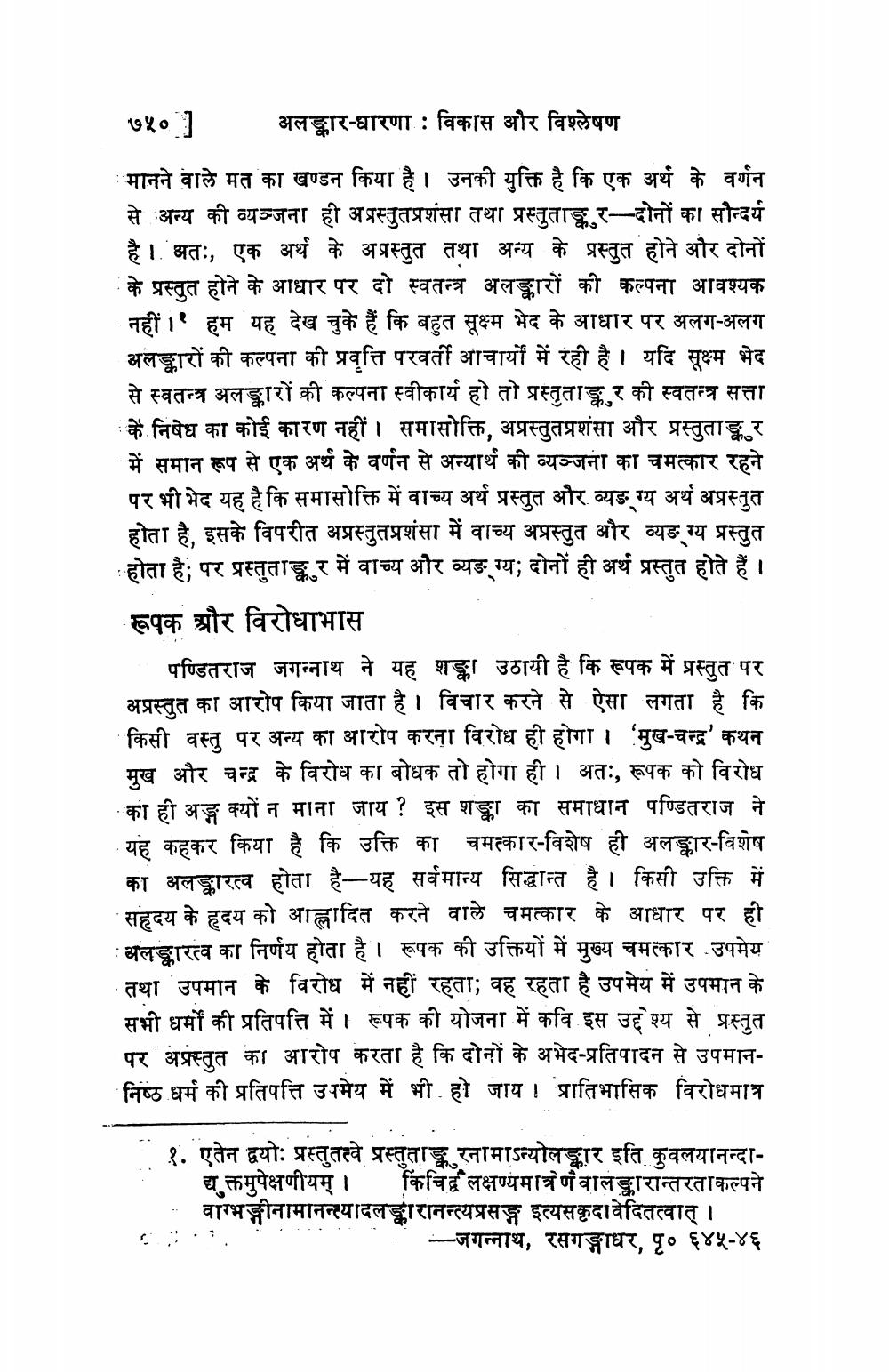________________
७५० ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
मानने वाले मत का खण्डन किया है। उनकी युक्ति है कि एक अर्थ के वर्णन से अन्य की व्यञ्जना ही अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुताङ्कर-दोनों का सौन्दर्य है। अतः, एक अर्थ के अप्रस्तुत तथा अन्य के प्रस्तुत होने और दोनों के प्रस्तुत होने के आधार पर दो स्वतन्त्र अलङ्कारों की कल्पना आवश्यक नहीं।' हम यह देख चुके हैं कि बहुत सूक्ष्म भेद के आधार पर अलग-अलग अलङ्कारों की कल्पना की प्रवृत्ति परवर्ती आचार्यों में रही है। यदि सूक्ष्म भेद से स्वतन्त्र अलङ्कारों की कल्पना स्वीकार्य हो तो प्रस्तुताङ्कर की स्वतन्त्र सत्ता के निषेध का कोई कारण नहीं। समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा और प्रस्तुताङ्क र में समान रूप से एक अर्थ के वर्णन से अन्यार्थ की व्यञ्जना का चमत्कार रहने पर भी भेद यह है कि समासोक्ति में वाच्य अर्थ प्रस्तुत और व्यङग्य अर्थ अप्रस्तुत होता है, इसके विपरीत अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्य अप्रस्तुत और व्यङग्य प्रस्तुत होता है; पर प्रस्तुताङ्कर में वाच्य और व्यङ ग्य; दोनों ही अर्थ प्रस्तुत होते हैं । रूपक और विरोधाभास
पण्डितराज जगन्नाथ ने यह शङ्का उठायी है कि रूपक में प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है। विचार करने से ऐसा लगता है कि किसी वस्तु पर अन्य का आरोप करना विरोध ही होगा। 'मुख-चन्द्र' कथन मुख और चन्द्र के विरोध का बोधक तो होगा ही। अतः, रूपक को विरोध का ही अङ्ग क्यों न माना जाय ? इस शङ्का का समाधान पण्डितराज ने यह कहकर किया है कि उक्ति का चमत्कार-विशेष ही अलङ्कार-विशेष का अलङ्कारत्व होता है-यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। किसी उक्ति में सहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाले चमत्कार के आधार पर ही अलङ्कारत्व का निर्णय होता है। रूपक की उक्तियों में मुख्य चमत्कार उपमेय तथा उपमान के विरोध में नहीं रहता; वह रहता है उपमेय में उपमान के सभी धर्मों की प्रतिपत्ति में । रूपक की योजना में कवि इस उद्देश्य से प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप करता है कि दोनों के अभेद-प्रतिपादन से उपमाननिष्ठ धर्म की प्रतिपत्ति उपमेय में भी हो जाय ! प्रातिभासिक विरोधमात्र
१. एतेन द्वयोः प्रस्तुतत्वे प्रस्तुताङ्क रनामाऽन्योलङ्कार इति कुवलयानन्दा
द्य क्तमुपेक्षणीयम्। किंचि_ लक्षण्यमात्रेण वालङ्कारान्तरताकल्पने - वाग्भङ्गीनामानन्त्यादलङ्कारानन्त्यप्रसङ्ग इत्यसकृदावेदितत्वात् ।
--जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ६४५-४६