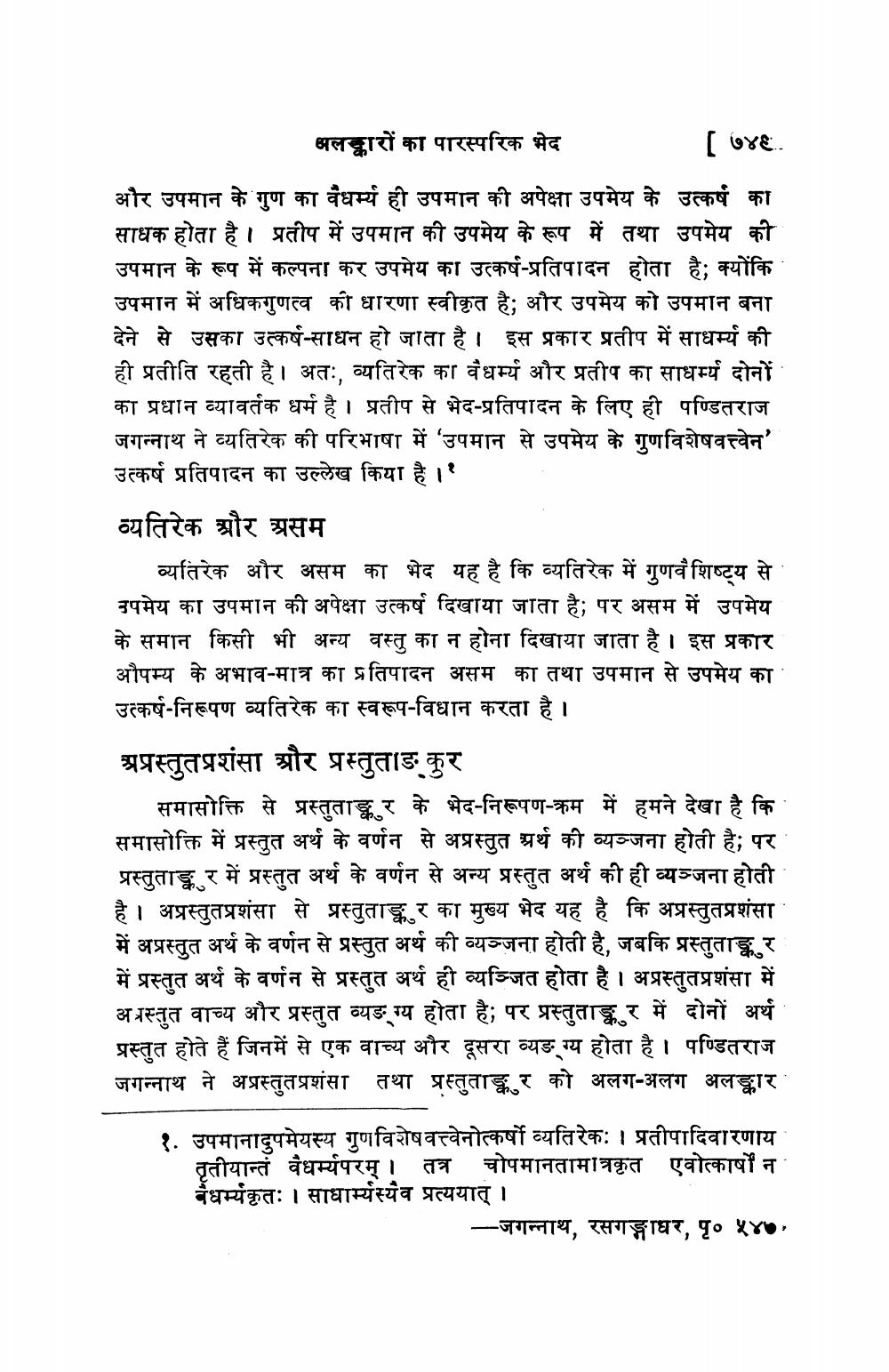________________
अलङ्कारों का पारस्परिक भेद
[७४६. और उपमान के गुण का वैधर्म्य ही उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष का साधक होता है। प्रतीप में उपमान की उपमेय के रूप में तथा उपमेय की उपमान के रूप में कल्पना कर उपमेय का उत्कर्ष-प्रतिपादन होता है; क्योंकि उपमान में अधिकगुणत्व की धारणा स्वीकृत है; और उपमेय को उपमान बना देने से उसका उत्कर्ष-साधन हो जाता है। इस प्रकार प्रतीप में साधर्म्य की ही प्रतीति रहती है। अतः, व्यतिरेक का वैधर्म्य और प्रतीप का साधर्म्य दोनों का प्रधान व्यावर्तक धर्म है। प्रतीप से भेद-प्रतिपादन के लिए ही पण्डितराज जगन्नाथ ने व्यतिरेक की परिभाषा में 'उपमान से उपमेय के गुणविशेषवत्त्वेन' उत्कर्ष प्रतिपादन का उल्लेख किया है।' व्यतिरेक और असम
व्यतिरेक और असम का भेद यह है कि व्यतिरेक में गुणवैशिष्ट्य से उपमेय का उपमान की अपेक्षा उत्कर्ष दिखाया जाता है; पर असम में उपमेय के समान किसी भी अन्य वस्तु का न होना दिखाया जाता है। इस प्रकार औपम्य के अभाव-मात्र का प्रतिपादन असम का तथा उपमान से उपमेय का उत्कर्ष-निरूपण व्यतिरेक का स्वरूप-विधान करता है। अप्रस्तुतप्रशंसा और प्रस्तुताङ कुर
समासोक्ति से प्रस्तुताङ्कर के भेद-निरूपण-क्रम में हमने देखा है कि समासोक्ति में प्रस्तुत अर्थ के वर्णन से अप्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना होती है; पर प्रस्तुताङ्क र में प्रस्तुत अर्थ के वर्णन से अन्य प्रस्तुत अर्थ की ही व्यञ्जना होती है। अप्रस्तुतप्रशंसा से प्रस्तुताङ्क र का मुख्य भेद यह है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत अर्थ के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना होती है, जबकि प्रस्तुताङ्कर में प्रस्तुत अर्थ के वर्णन से प्रस्तुत अर्थ ही व्यजित होता है । अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत वाच्य और प्रस्तुत व्यङ्ग्य होता है; पर प्रस्तुताङ्कर में दोनों अर्थ प्रस्तुत होते हैं जिनमें से एक वाच्य और दूसरा व्यङग्य होता है। पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुताङ्कर को अलग-अलग अलङ्कार १. उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषवत्त्वेनोत्कर्षों व्यतिरेकः । प्रतीपादिवारणाय
तृतीयान्तं वैधर्म्यपरम् । तत्र चोपमानतामात्रकृत एवोत्कार्षों न वैधर्म्यकृतः । साधार्म्यस्यैव प्रत्ययात् ।
-जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ५४."