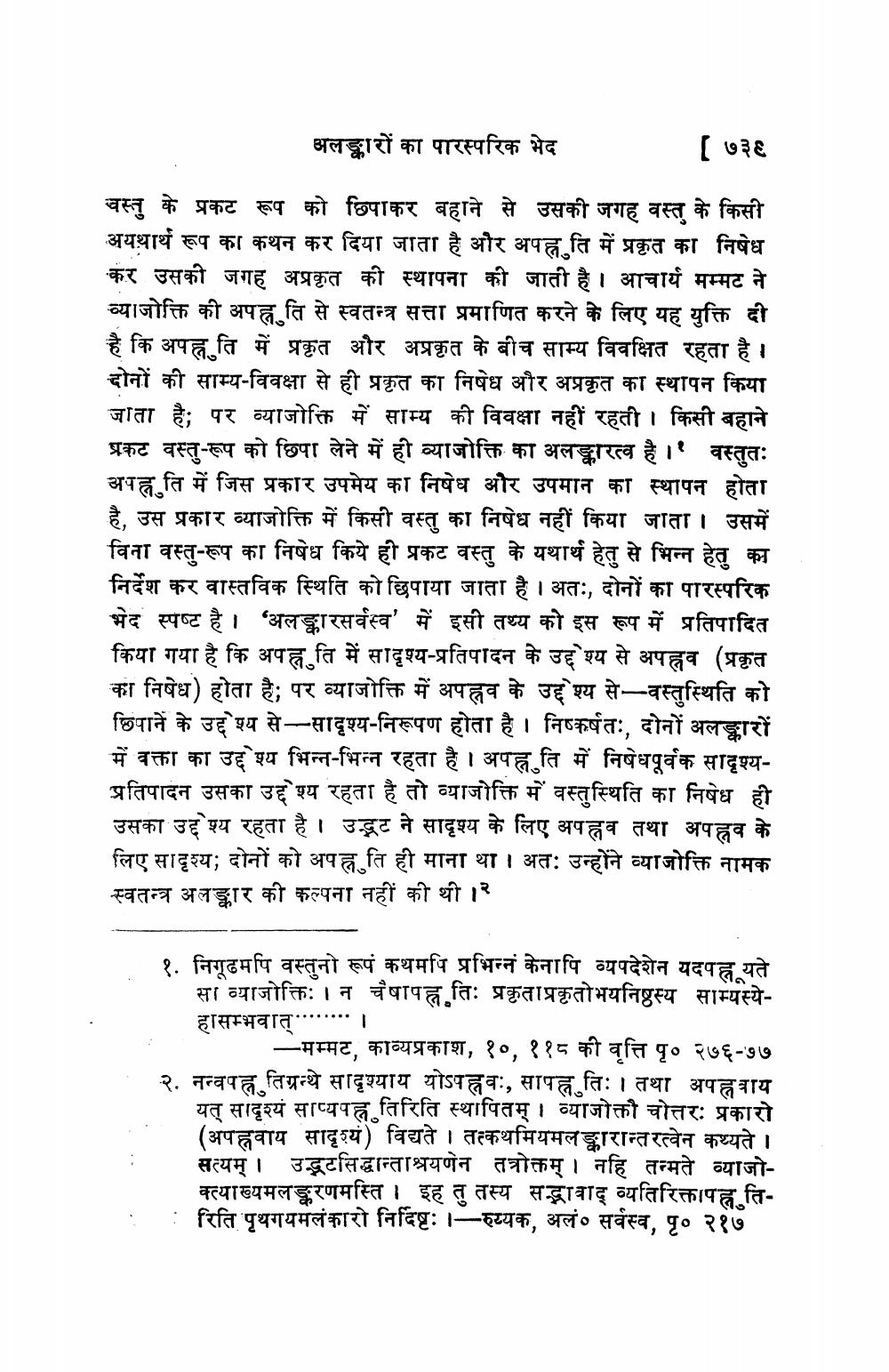________________
अलङ्कारों का पारस्परिक भेद
[ ७३६
वस्तु के प्रकट रूप को छिपाकर बहाने से उसकी जगह वस्तु के किसी अयथार्थ रूप का कथन कर दिया जाता है और अपह्न ुति में प्रकृत का निषेध कर उसकी जगह अप्रकृत की स्थापना की जाती है । आचार्य मम्मट ने व्याजोक्ति की अपह्नति से स्वतन्त्र सत्ता प्रमाणित करने के लिए यह युक्ति दी है कि अपह्नति में प्रकृत और अप्रकृत के बीच साम्य विवक्षित रहता है । दोनों की साम्य-विवक्षा से ही प्रकृत का निषेध और अप्रकृत का स्थापन किया जाता है; पर व्याजोक्ति में साम्य की विवक्षा नहीं रहती । किसी बहाने प्रकट वस्तु रूप को छिपा लेने में ही व्याजोक्ति का अलङ्कारत्व है । वस्तुतः अपह्नति में जिस प्रकार उपमेय का निषेध और उपमान का स्थापन होता है, उस प्रकार व्याजोक्ति में किसी वस्तु का निषेध नहीं किया जाता । उसमें विना वस्तु रूप का निषेध किये ही प्रकट वस्तु के यथार्थ हेतु से भिन्न हेतु का निर्देश कर वास्तविक स्थिति को छिपाया जाता है । अतः, दोनों का पारस्परिक भेद स्पष्ट है । 'अलङ्कारसर्वस्व' में इसी तथ्य को इस रूप में प्रतिपादित किया गया है कि अपह्न ुति में सादृश्य- प्रतिपादन के उद्देश्य से अपह्नव ( प्रकृत का निषेध) होता है; पर व्याजोक्ति में अपह्नव के उद्द ेश्य से - वस्तुस्थिति को छिपाने के उद्देश्य से - सादृश्य-निरूपण होता है । निष्कर्षतः, दोनों अलङ्कारों में वक्ता का उद्देश्य भिन्न-भिन्न रहता है । अपह्न ुति में निषेधपूर्वक सादृश्यप्रतिपादन उसका उद्देश्य रहता है तो व्याजोक्ति में वस्तुस्थिति का निषेध ही उसका उद्देश्य रहता है । उद्भट ने सादृश्य के लिए अपह्नव तथा अपह्नव के लिए सादृश्य; दोनों को अपह्न ुति ही माना था । अत: उन्होंने व्याजोक्ति नामक स्वतन्त्र अलङ्कार की कल्पना नहीं की थी । २
१. निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपह्नय • यते सा व्याजोक्तिः । न चैषापह्नतिः प्रकृताप्रकृतोभयनिष्ठस्य साम्यस्येहासम्भवात् I
- मम्मट, काव्यप्रकाश, १०, ११८ की वृत्ति पृ० २७६-७७ २. नन्वपह्न ुतिग्रन्थे सादृश्याय योऽपह्नवः, सापह्न तिः । तथा अपह्नवाय यत् सादृश्यं साप्यपह्न तिरिति स्थापितम् । व्याजोक्तौ चोत्तरः प्रकारो ( अपह्नवाय सादृश्यं) विद्यते । तत्कथमियमलङ्कारान्तरत्वेन कथ्यते । सत्यम् । उद्भटसिद्धान्ताश्रयणेन तत्रोक्तम् । नहि तन्मते व्याजोक्त्याख्यमलङ्करणमस्ति । इह तु तस्य सद्भावाद् व्यतिरिक्तापह्न ुतिरिति पृथगमलंकारो निर्दिष्टः । —रुय्यक, अलं० सर्वस्व, पृ० २१७