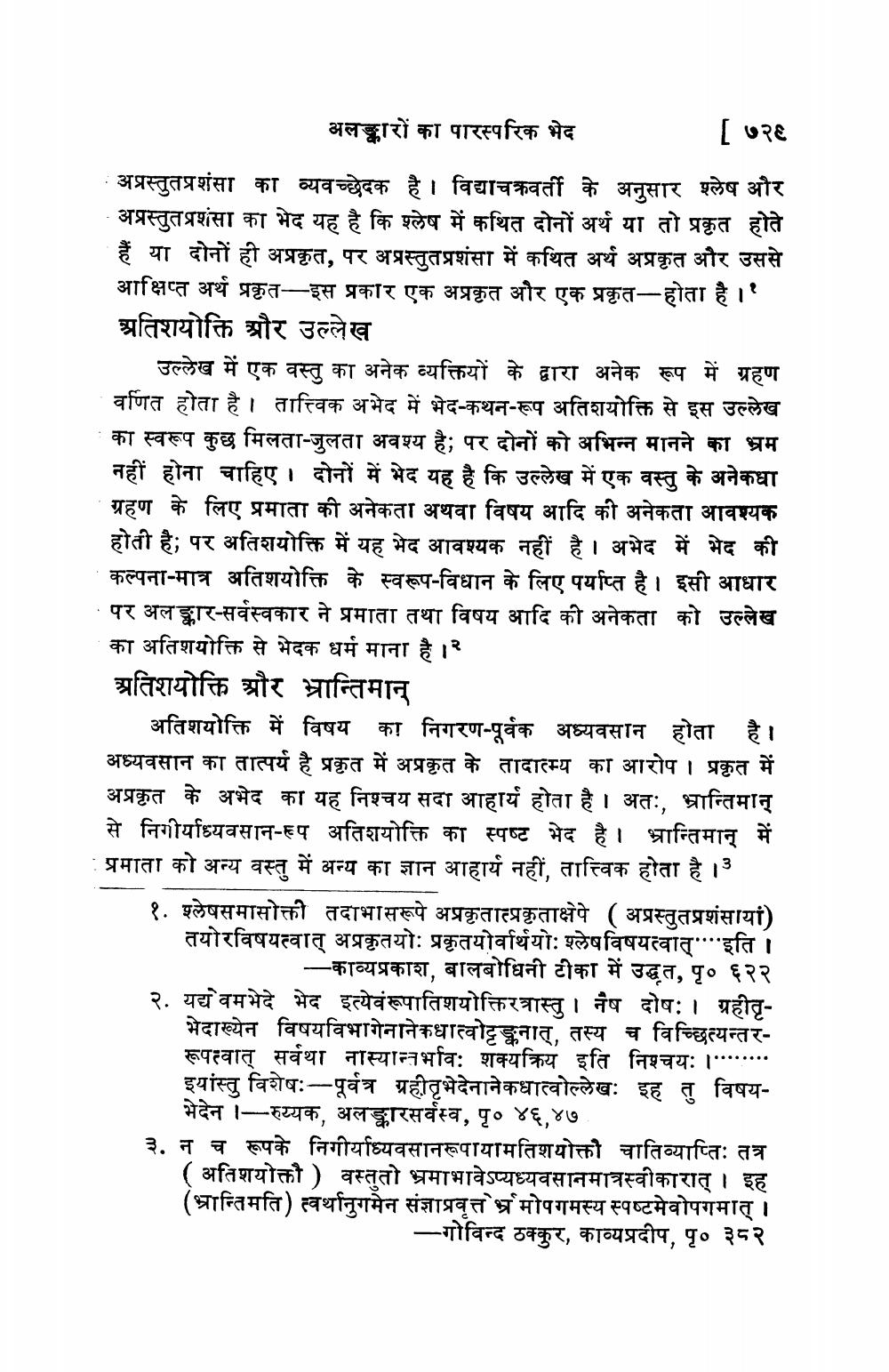________________
अलङ्कारों का पारस्परिक भेद
[ ७२६
अप्रस्तुतप्रशंसा का व्यवच्छेदक है । विद्याचक्रवर्ती के अनुसार श्लेष और अप्रस्तुतप्रशंसा का भेद यह है कि श्लेष में कथित दोनों अर्थ या तो प्रकृत होते हैं या दोनों ही अप्रकृत, पर अप्रस्तुतप्रशंसा में कथित अर्थ अप्रकृत और उससे आक्षिप्त अर्थ प्रकृत- - इस प्रकार एक अप्रकृत और एक प्रकृत — होता है । ' अतिशयोक्ति और उल्लेख
१
-
उल्लेख में एक वस्तु का अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक रूप में ग्रहण वर्णित होता है । तात्त्विक अभेद में भेद - कथन - रूप अतिशयोक्ति से इस उल्लेख का स्वरूप कुछ मिलता-जुलता अवश्य है; पर दोनों को अभिन्न मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए। दोनों में भेद यह है कि उल्लेख में एक वस्तु के अनेकधा ग्रहण के लिए प्रमाता की अनेकता अथवा विषय आदि की अनेकता आवश्यक होती है; पर अतिशयोक्ति में यह भेद आवश्यक नहीं है । अभेद में भेद की कल्पना मात्र अतिशयोक्ति के स्वरूप-विधान के लिए पर्याप्त है । इसी आधार पर अलङ्कार- सर्वस्वकार ने प्रमाता तथा विषय आदि की अनेकता को उल्लेख का अतिशयोक्ति से भेदक धर्म माना है ।
अतिशयोक्ति और भ्रान्तिमान्
अतिशयोक्ति में विषय का निगरण - पूर्वक अध्यवसान होता है । अध्यवसान का तात्पर्य है प्रकृत में अप्रकृत के तादात्म्य का आरोप । प्रकृत में अप्रकृत के अभेद का यह निश्चय सदा आहार्य होता है । अतः, भ्रान्तिमान् से निगीर्याध्यवसान - रूप अतिशयोक्ति का स्पष्ट भेद है । भ्रान्तिमान् में माता को अन्य वस्तु में अन्य का ज्ञान आहार्य नहीं, तात्त्विक होता है ।
१. श्लेषसमासोक्ती तदाभासरूपे अप्रकृतात्प्रकृताक्षेपे ( अप्रस्तुतप्रशंसायां ) तयोरविषयत्वात् अप्रकृतयोः प्रकृतयोर्वार्थयोः श्लेष विषयत्वात् इति । - काव्यप्रकाश, बालबोधिनी टीका में उद्धृत, पृ० ६२२ २. यद्य ेवमभेदे भेद इत्येवंरूपातिशयोक्तिरत्रास्तु । नैष दोषः । ग्रहीतृभेदाख्येन विषयविभागेनानेकधात्वोदृङ्कनात्, तस्य च विच्छित्यन्तररूपत्वात् सर्वथा नास्यान्तर्भावः शक्यक्रिय इति निश्चयः । ... इयांस्तु विशेषः - पूर्वत्र ग्रहीतृभेदेनानेकधात्वोल्लेखः इह तु विषयभेदेन । —रुय्यक, अलङ्कारसर्वस्व, पृ० ४६,४७
३. न च रूपके निगीर्याध्यवसानरूपायामतिशयोक्ती चातिव्याप्तिः तत्र ( अतिशयोक्तौ ) वस्तुतो भ्रमाभावेऽप्यध्यवसानमात्र स्वीकारात् । इह (भ्रान्तिमति) स्वर्थानुगमेन संज्ञाप्रवृत्त े भ्रं मोपगमस्य स्पष्टमेवोपगमात् । - गोविन्द ठक्कुर, काव्यप्रदीप, पृ० ३८२