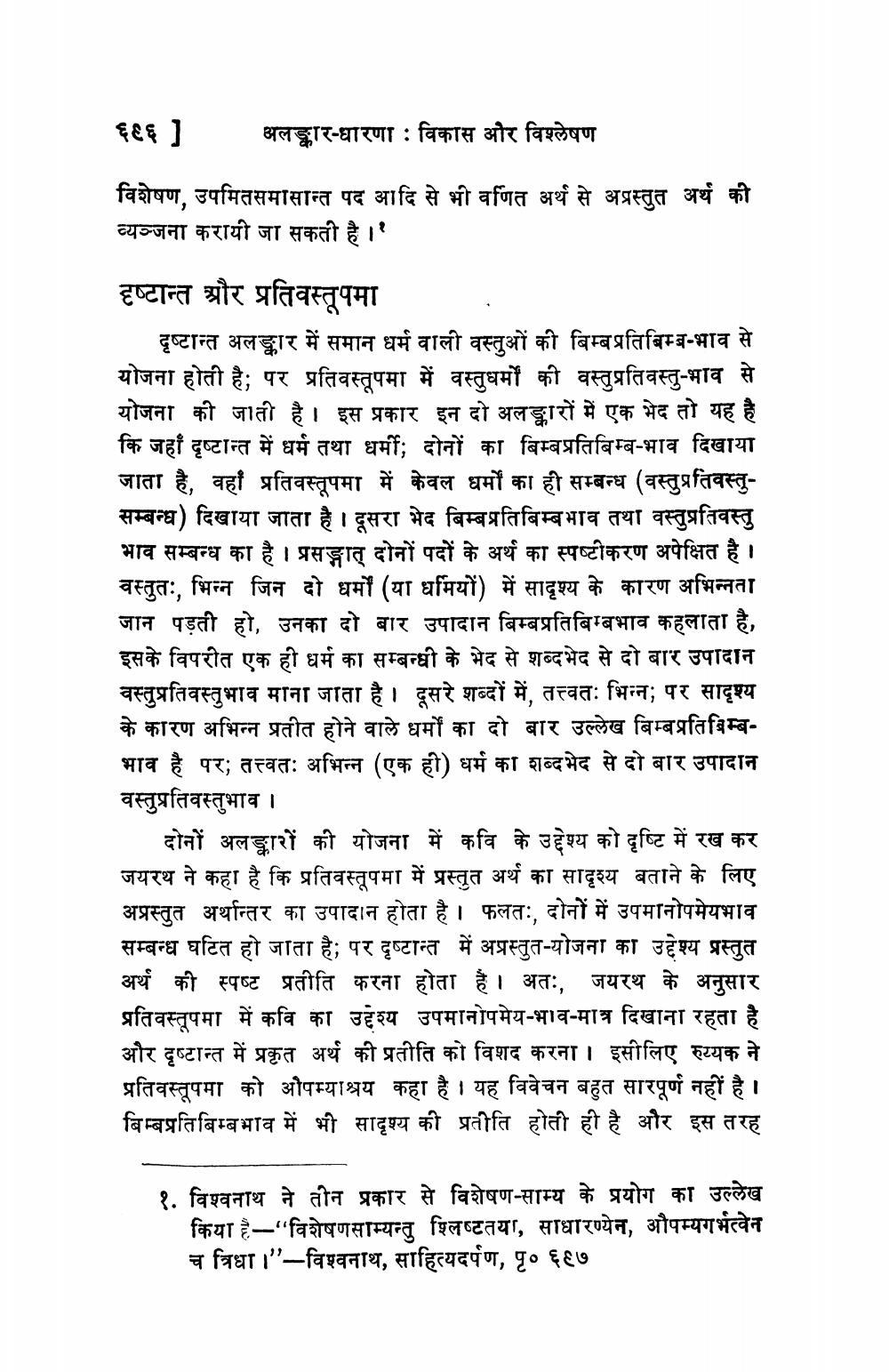________________
६६६ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
विशेषण, उपमितसमासान्त पद आदि से भी वणित अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना करायी जा सकती है।'
दृष्टान्त और प्रतिवस्तूपमा
दृष्टान्त अलङ्कार में समान धर्म वाली वस्तुओं की बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव से योजना होती है; पर प्रतिवस्तूपमा में वस्तुधर्मों की वस्तुप्रतिवस्तु-भाव से योजना की जाती है। इस प्रकार इन दो अलङ्कारों में एक भेद तो यह है कि जहाँ दृष्टान्त में धर्म तथा धर्मी; दोनों का बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव दिखाया जाता है, वहाँ प्रतिवस्तूपमा में केवल धर्मों का ही सम्बन्ध (वस्तुप्रतिवस्तुसम्बन्ध) दिखाया जाता है। दूसरा भेद बिम्बप्रतिबिम्बभाव तथा वस्तुप्रतिवस्तु भाव सम्बन्ध का है । प्रसङ्गात् दोनों पदों के अर्थ का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। वस्तुतः, भिन्न जिन दो धर्मों (या धर्मियों) में सादृश्य के कारण अभिन्नता जान पड़ती हो, उनका दो बार उपादान बिम्बप्रतिबिम्बभाव कहलाता है, इसके विपरीत एक ही धर्म का सम्बन्धी के भेद से शब्दभेद से दो बार उपादान वस्तुप्रतिवस्तुभाव माना जाता है। दूसरे शब्दों में, तत्त्वतः भिन्न; पर सादृश्य के कारण अभिन्न प्रतीत होने वाले धर्मों का दो बार उल्लेख बिम्बप्रतिबिम्बभाव है पर; तत्त्वतः अभिन्न (एक ही) धर्म का शब्द भेद से दो बार उपादान वस्तुप्रतिवस्तुभाव।
दोनों अलङ्कारों की योजना में कवि के उद्देश्य को दृष्टि में रख कर जयरथ ने कहा है कि प्रतिवस्तूपमा में प्रस्तुत अर्थ का सादृश्य बताने के लिए अप्रस्तुत अर्थान्तर का उपादान होता है। फलतः, दोनों में उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध घटित हो जाता है; पर दृष्टान्त में अप्रस्तुत-योजना का उद्देश्य प्रस्तुत अर्थ की स्पष्ट प्रतीति करना होता है। अतः, जयरथ के अनुसार प्रतिवस्तूपमा में कवि का उद्देश्य उपमानोपमेय-भाव-मात्र दिखाना रहता है और दृष्टान्त में प्रकृत अर्थ की प्रतीति को विशद करना। इसीलिए रुय्यक ने प्रतिवस्तूपमा को औपम्याश्रय कहा है। यह विवेचन बहुत सारपूर्ण नहीं है। बिम्बप्रतिबिम्बभाव में भी सादृश्य की प्रतीति होती ही है और इस तरह
१. विश्वनाथ ने तीन प्रकार से विशेषण-साम्य के प्रयोग का उल्लेख
किया है-"विशेषणसाम्यन्तु श्लिष्टतया, साधारण्येन, औपम्यगर्भत्वेन च त्रिधा।"-विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, पृ० ६६७