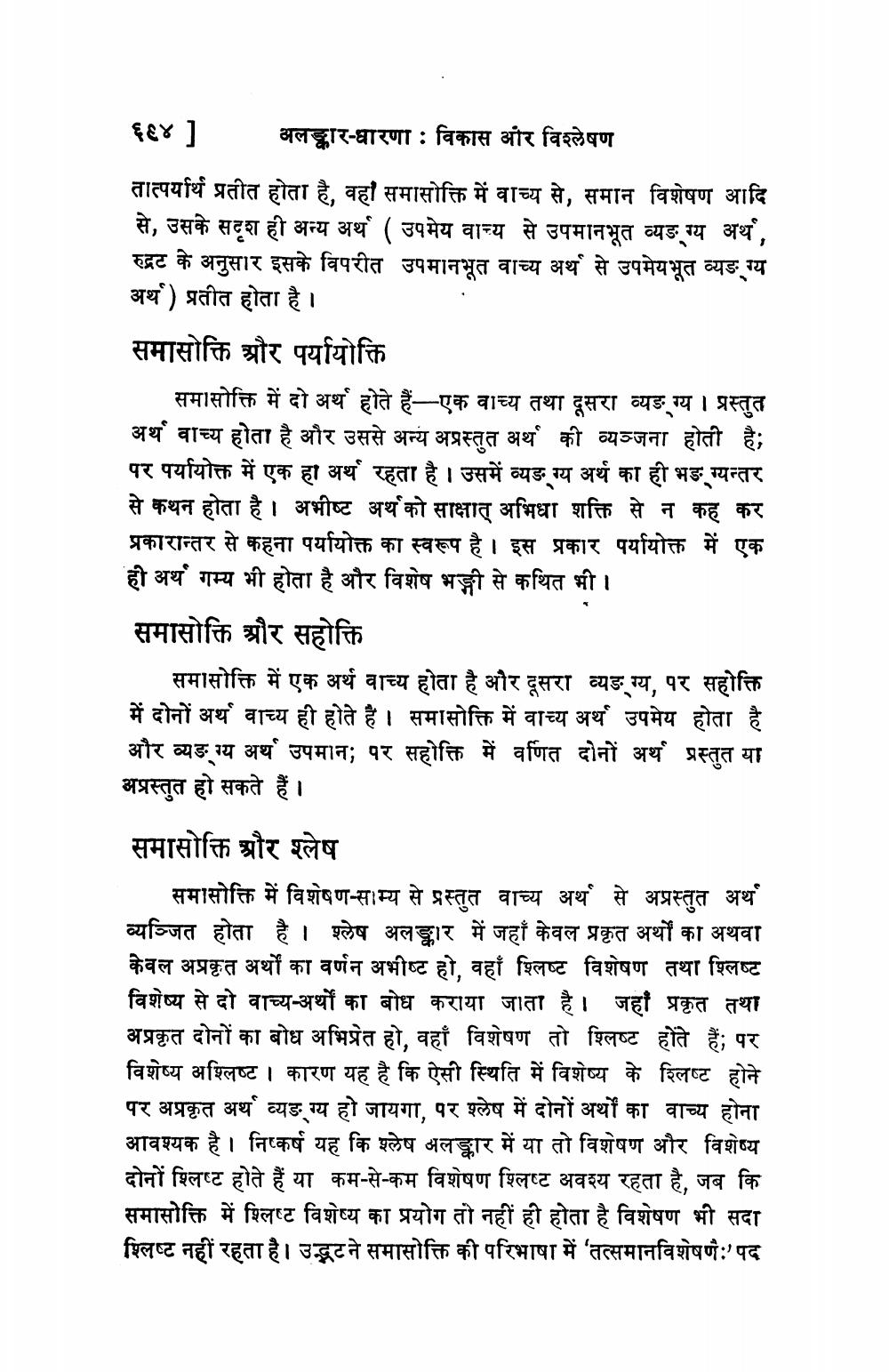________________
६६४ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
तात्पर्यार्थ प्रतीत होता है, वहां समासोक्ति में वाच्य से, समान विशेषण आदि से, उसके सदृश ही अन्य अर्थ ( उपमेय वाच्य से उपमानभूत व्यङग्य अर्थ, रुद्रट के अनुसार इसके विपरीत उपमानभूत वाच्य अर्थ से उपमेयभूत व्यङ ग्य अर्थ) प्रतीत होता है। समासोक्ति और पर्यायोक्ति
समासोक्ति में दो अर्थ होते हैं—एक वाच्य तथा दूसरा व्यङग्य । प्रस्तुत अर्थ वाच्य होता है और उससे अन्य अप्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना होती है; पर पर्यायोक्त में एक हा अर्थ रहता है। उसमें व्यङग्य अर्थ का ही भङ ग्यन्तर से कथन होता है। अभीष्ट अर्थको साक्षात् अभिधा शक्ति से न कह कर प्रकारान्तर से कहना पर्यायोक्त का स्वरूप है। इस प्रकार पर्यायोक्त में एक ही अर्थ गम्य भी होता है और विशेष भङ्गी से कथित भी। समासोक्ति और सहोक्ति
समासोक्ति में एक अर्थ वाच्य होता है और दूसरा व्यङ ग्य, पर सहोक्ति में दोनों अर्थ वाच्य ही होते है। समासोक्ति में वाच्य अर्थ उपमेय होता है और व्यङग्य अर्थ उपमान; पर सहोक्ति में वर्णित दोनों अर्थ प्रस्तुत या अप्रस्तुत हो सकते हैं। समासोक्ति और श्लेष
समासोक्ति में विशेषण-साम्य से प्रस्तुत वाच्य अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ व्यजित होता है। श्लेष अलङ्कार में जहाँ केवल प्रकृत अर्थों का अथवा केवल अप्रकृत अर्थों का वर्णन अभीष्ट हो, वहाँ श्लिष्ट विशेषण तथा श्लिष्ट विशेष्य से दो वाच्य-अर्थों का बोध कराया जाता है। जहाँ प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों का बोध अभिप्रेत हो, वहाँ विशेषण तो श्लिष्ट होते हैं; पर विशेष्य अश्लिष्ट । कारण यह है कि ऐसी स्थिति में विशेष्य के श्लिष्ट होने पर अप्रकृत अर्थ व्यङग्य हो जायगा, पर श्लेष में दोनों अर्थों का वाच्य होना आवश्यक है। निष्कर्ष यह कि श्लेष अलङ्कार में या तो विशेषण और विशेष्य दोनों श्लिष्ट होते हैं या कम-से-कम विशेषण श्लिष्ट अवश्य रहता है, जब कि समासोक्ति में श्लिष्ट विशेष्य का प्रयोग तो नहीं ही होता है विशेषण भी सदा श्लिष्ट नहीं रहता है। उद्भट ने समासोक्ति की परिभाषा में 'तत्समानविशेषणैः' पद