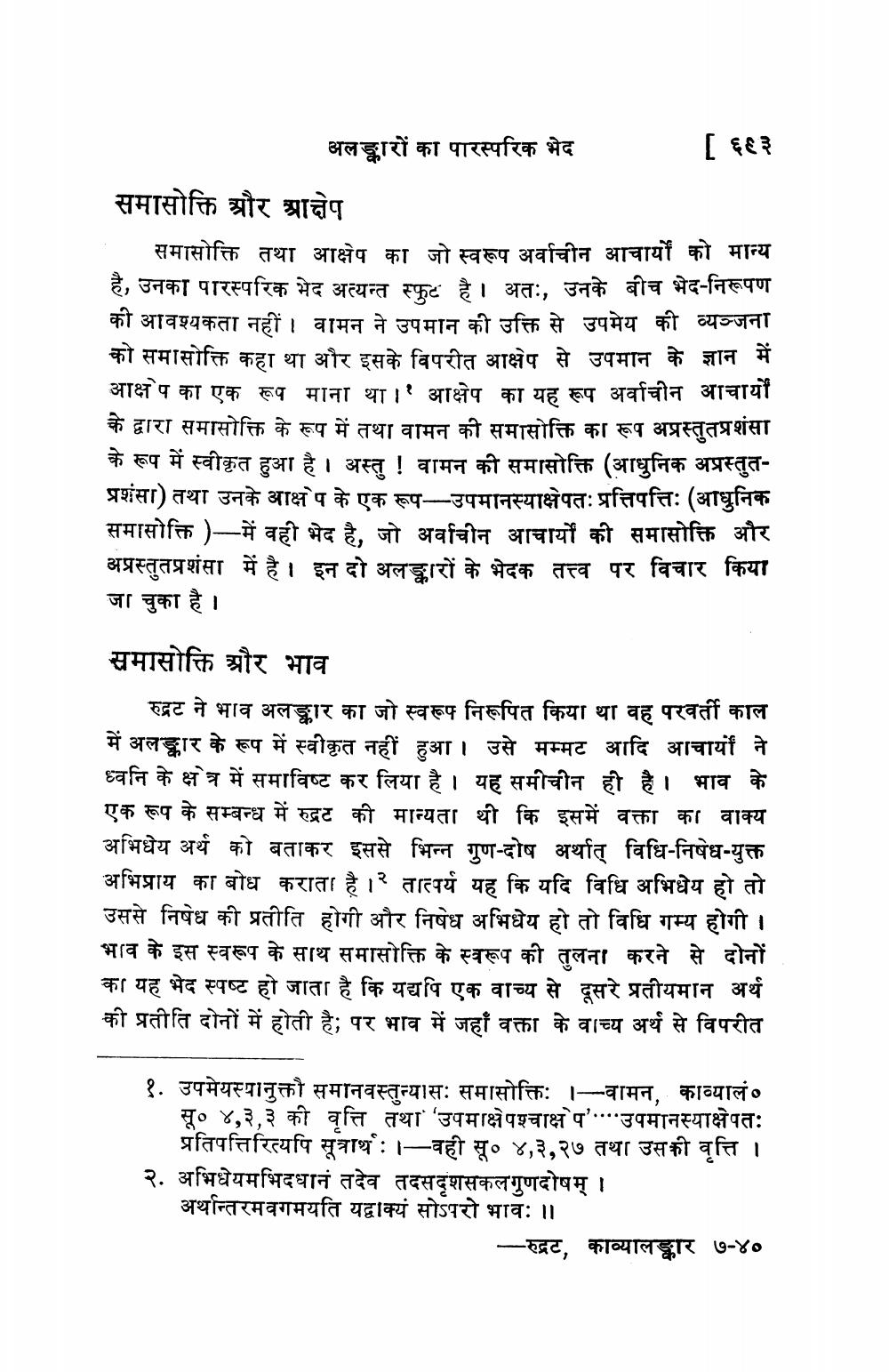________________
अलङ्कारों का पारस्परिक भेद
[ ६९३
समासोक्ति और आक्षेप
समासोक्ति तथा आक्षेप का जो स्वरूप अर्वाचीन आचार्यों को मान्य है, उनका पारस्परिक भेद अत्यन्त स्फुट है । अतः, उनके बीच भेद-निरूपण की आवश्यकता नहीं। वामन ने उपमान की उक्ति से उपमेय की व्यञ्जना को समासोक्ति कहा था और इसके विपरीत आक्षेप से उपमान के ज्ञान में आक्ष ेप का एक रूप माना था । ' आक्षेप का यह रूप अर्वाचीन आचार्यों के द्वारा समासोक्ति के रूप ' तथा वामन की समासोक्ति का रूप अप्रस्तुतप्रशंसा
।
-
के रूप में स्वीकृत हुआ है अस्तु ! वामन की समासोक्ति (आधुनिक अप्रस्तुतप्रशंसा तथा उनके आक्ष ेप के एक रूप — उपमानस्याक्षेपतः प्रत्तिपत्तिः ( आधुनिक समासोक्ति ) – में वही भेद है, जो अर्वाचीन आचार्यों की समासोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसा में है । इन दो अलङ्कारों के भेदक तत्त्व पर विचार किया जा चुका है ।
समासोक्ति और भाव
रुद्रट ने भाव अलङ्कार का जो स्वरूप निरूपित किया था वह परवर्ती काल में अलङ्कार के रूप में स्वीकृत नहीं हुआ। उसे मम्मट आदि आचार्यों ने ध्वनि के क्ष ेत्र में समाविष्ट कर लिया है । यह समीचीन ही है । भाव के एक रूप के सम्बन्ध में रुद्रट की मान्यता थी कि इसमें वक्ता का वाक्य अभिधेय अर्थ को बताकर इससे भिन्न गुण-दोष अर्थात् विधि-निषेध-युक्त अभिप्राय का बोध कराता है। तात्पर्य यह कि यदि विधि अभिधेय हो तो उससे निषेध की प्रतीति होगी और निषेध अभिधेय हो तो विधि गम्य होगी । भाव के इस स्वरूप के साथ समासोक्ति के स्वरूप की तुलना करने से दोनों का यह भेद स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि एक वाच्य से दूसरे प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति दोनों में होती है; पर भाव में जहाँ वक्ता के वाच्य अर्थ से विपरीत
१. उपमेयस्यानुक्तौ समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । वामन, काव्यालं • सू० ४,३, ३ की वृत्ति तथा 'उपमाक्षेपश्चाक्ष ेप' उपमानस्याक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थ: । - वही सू० ४,३, २७ तथा उसकी वृत्ति । २. अभिधेयमभिदधानं तदेव तदसदृशसकलगुणदोषम् ।
अर्थान्तरमवगमयति यद्वाक्यं सोऽपरो भावः ॥
- रुद्रट, काव्यालङ्कार ७-४०