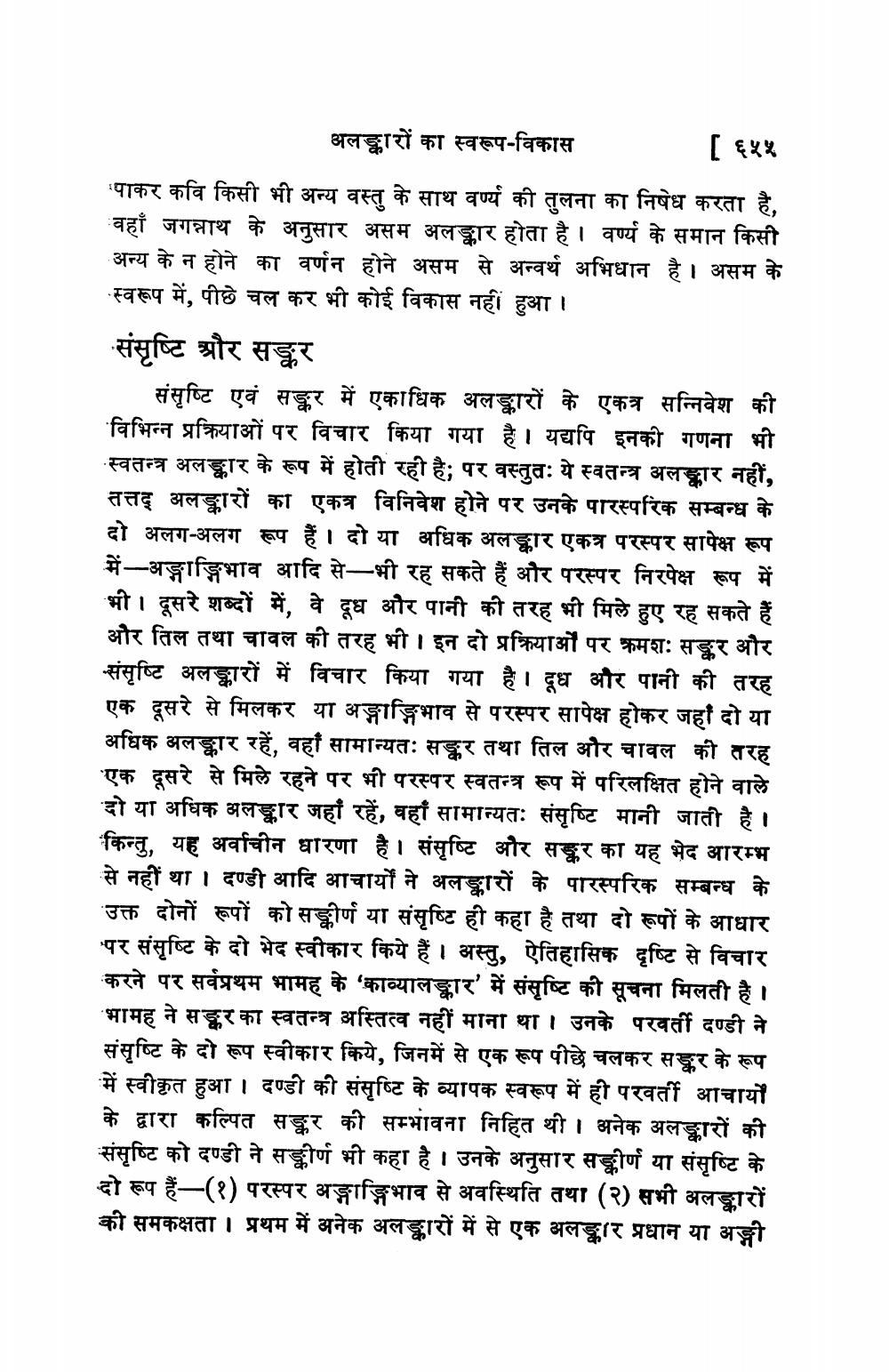________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[६५५
पाकर कवि किसी भी अन्य वस्तु के साथ वर्ण्य की तुलना का निषेध करता है, वहाँ जगन्नाथ के अनुसार असम अलङ्कार होता है। वर्ण्य के समान किसी अन्य के न होने का वर्णन होने असम से अन्वर्थ अभिधान है। असम के स्वरूप में, पीछे चल कर भी कोई विकास नहीं हुआ। संसृष्टि और सङ्कर
संसृष्टि एवं सङ्कर में एकाधिक अलङ्कारों के एकत्र सन्निवेश की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विचार किया गया है। यद्यपि इनकी गणना भी स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में होती रही है; पर वस्तुतः ये स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं, तत्तद् अलङ्कारों का एकत्र विनिवेश होने पर उनके पारस्परिक सम्बन्ध के दो अलग-अलग रूप हैं। दो या अधिक अलङ्कार एकत्र परस्पर सापेक्ष रूप में-अङ्गाङ्गिभाव आदि से भी रह सकते हैं और परस्पर निरपेक्ष रूप में भी। दूसरे शब्दों में, वे दूध और पानी की तरह भी मिले हुए रह सकते हैं और तिल तथा चावल की तरह भी। इन दो प्रक्रियाओं पर क्रमशः सङ्कर और संसृष्टि अलङ्कारों में विचार किया गया है। दूध और पानी की तरह एक दूसरे से मिलकर या अङ्गाङ्गिभाव से परस्पर सापेक्ष होकर जहां दो या अधिक अलङ्कार रहें, वहाँ सामान्यतः सङ्कर तथा तिल और चावल की तरह एक दूसरे से मिले रहने पर भी परस्पर स्वतन्त्र रूप में परिलक्षित होने वाले दो या अधिक अलङ्कार जहाँ रहें, वहां सामान्यतः संसृष्टि मानी जाती है। किन्तु, यह अर्वाचीन धारणा है। संसृष्टि और सङ्कर का यह भेद आरम्भ से नहीं था। दण्डी आदि आचार्यों ने अलङ्कारों के पारस्परिक सम्बन्ध के उक्त दोनों रूपों को सङ्कीर्ण या संसृष्टि ही कहा है तथा दो रूपों के आधार 'पर संसृष्टि के दो भेद स्वीकार किये हैं। अस्तु, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर सर्वप्रथम भामह के 'काव्यालङ्कार' में संसृष्टि की सूचना मिलती है। भामह ने सङ्कर का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं माना था। उनके परवर्ती दण्डी ने संसृष्टि के दो रूप स्वीकार किये, जिनमें से एक रूप पीछे चलकर सङ्कर के रूप में स्वीकृत हुआ। दण्डी की संसृष्टि के व्यापक स्वरूप में ही परवर्ती आचार्यों के द्वारा कल्पित सङ्कर की सम्भावना निहित थी। अनेक अलङ्कारों की संसृष्टि को दण्डी ने सङ्कीर्ण भी कहा है । उनके अनुसार सङ्कीर्ण या संसृष्टि के दो रूप हैं-(१) परस्पर अङ्गाङ्गिभाव से अवस्थिति तथा (२) सभी अलङ्कारों की समकक्षता । प्रथम में अनेक अलङ्कारों में से एक अलङ्कार प्रधान या अङ्गी