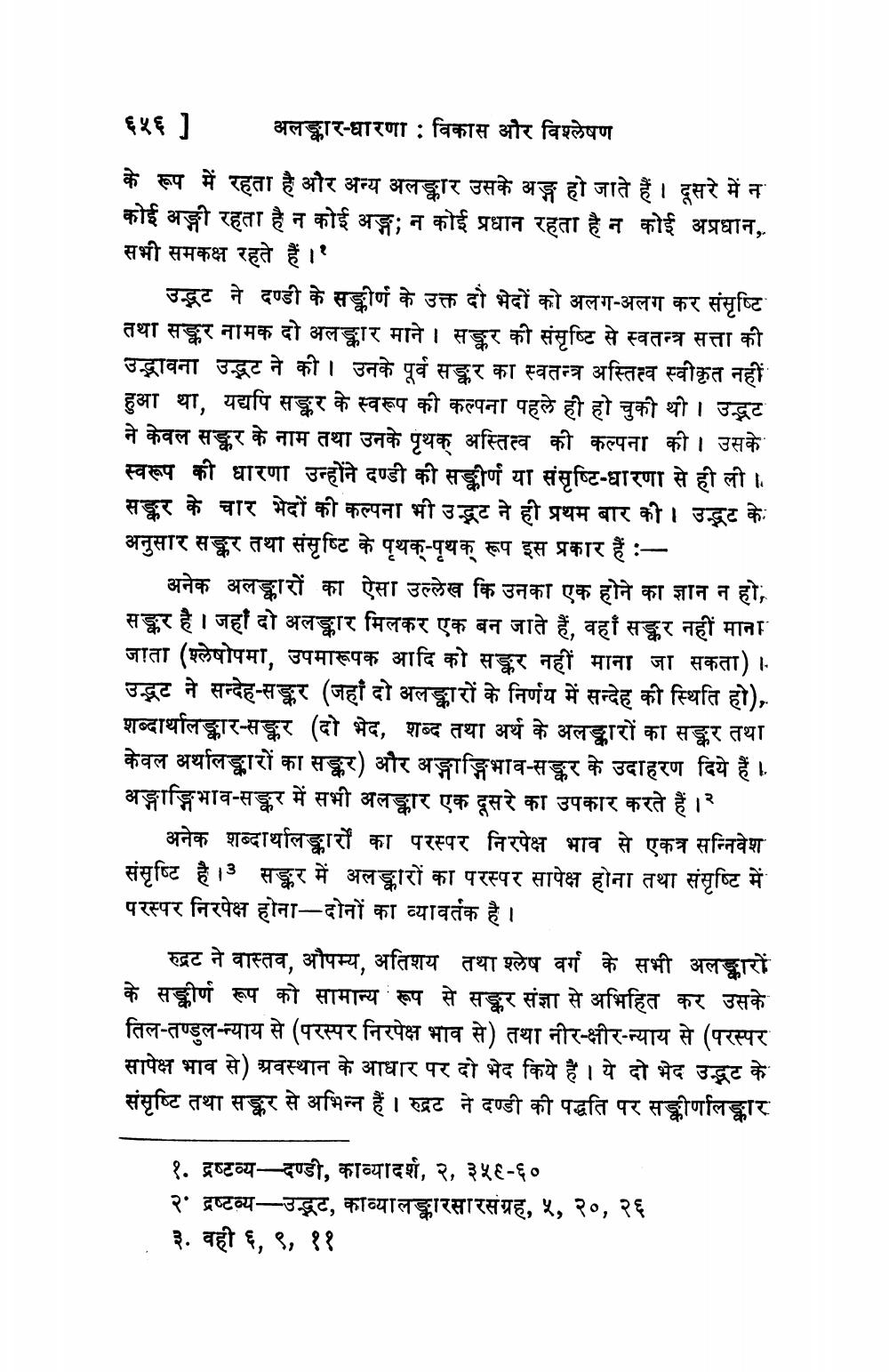________________
६५६ ]
अलङ्कार- धारणा : विकास और विश्लेषण
के रूप में रहता है और अन्य अलङ्कार उसके अङ्ग हो जाते हैं । दूसरे में न कोई अङ्गी रहता है न कोई अङ्ग; न कोई प्रधान रहता है न कोई अप्रधान, सभी समकक्ष रहते हैं । '
उद्भट ने दण्डी के सङ्कीर्ण के उक्त दो भेदों को अलग-अलग कर संसृष्टि तथा सङ्कर नामक दो अलङ्कार माने । सङ्कर की संसृष्टि से स्वतन्त्र सत्ता की उद्भावना उद्भट ने की । उनके पूर्व सङ्कर का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकृत नहीं हुआ था, यद्यपि सङ्कर के स्वरूप की कल्पना पहले ही हो चुकी थी । उद्भट ने केवल सङ्कर के नाम तथा उनके पृथक् अस्तित्व की कल्पना की । उसके स्वरूप की धारणा उन्होंने दण्डी की सङ्कीर्ण या संसृष्टि धारणा से ही ली । सङ्कर के चार भेदों की कल्पना भी उद्भट ने ही प्रथम बार की। उद्भट के अनुसार सङ्कर तथा संसृष्टि के पृथक्-पृथक् रूप इस प्रकार हैं :
——
अनेक अलङ्कारों का ऐसा उल्लेख कि उनका एक होने का ज्ञान न हो, सङ्कर है । जहाँ दो अलङ्कार मिलकर एक बन जाते हैं, वहाँ सङ्कर नहीं माना जाता ( श्लेषोपमा, उपमारूपक आदि को सङ्कर नहीं माना जा सकता ) ।उद्भट ने सन्देह-सङ्कर (जहाँ दो अलङ्कारों के निर्णय में सन्देह की स्थिति हो ), शब्दार्थालङ्कार-सङ्कर (दो भेद, शब्द तथा अर्थ के अलङ्कारों का सङ्कर तथा केवल अर्थालङ्कारों का सङ्कर) और अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर के उदाहरण दिये हैं ।. अङ्गाङ्गिभाव-सङ्कर में सभी अलङ्कार एक दूसरे का उपकार करते हैं ।
अनेक शब्दार्थालङ्कारों का परस्पर निरपेक्ष भाव से एकत्र सन्निवेश संसृष्टि है । 3 सङ्कर में अलङ्कारों का परस्पर सापेक्ष होना तथा संसृष्टि में परस्पर निरपेक्ष होना- दोनों का व्यावर्तक है ।
रुद्रट ने वास्तव, औपम्य, अतिशय तथा श्लेष वर्ग के सभी अलङ्कारों के सङ्कीर्ण रूप को सामान्य रूप से सङ्कर संज्ञा से अभिहित कर उसके तिल - तण्डुल - न्याय से ( परस्पर निरपेक्ष भाव से ) तथा नीर-क्षीर - न्याय से (परस्पर सापेक्ष भाव से) अवस्थान के आधार पर दो भेद किये हैं । ये दो भेद उद्भट के सृष्टि तथा सङ्कर से अभिन्न हैं । रुद्रट ने दण्डी की पद्धति पर सङ्कीर्णालङ्कार
१. द्रष्टव्य दण्डी, काव्यादर्श, २, ३५६-६०
२° द्रष्टव्य – उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह, ५, २०, २६ ३. वही ६, ९, ११