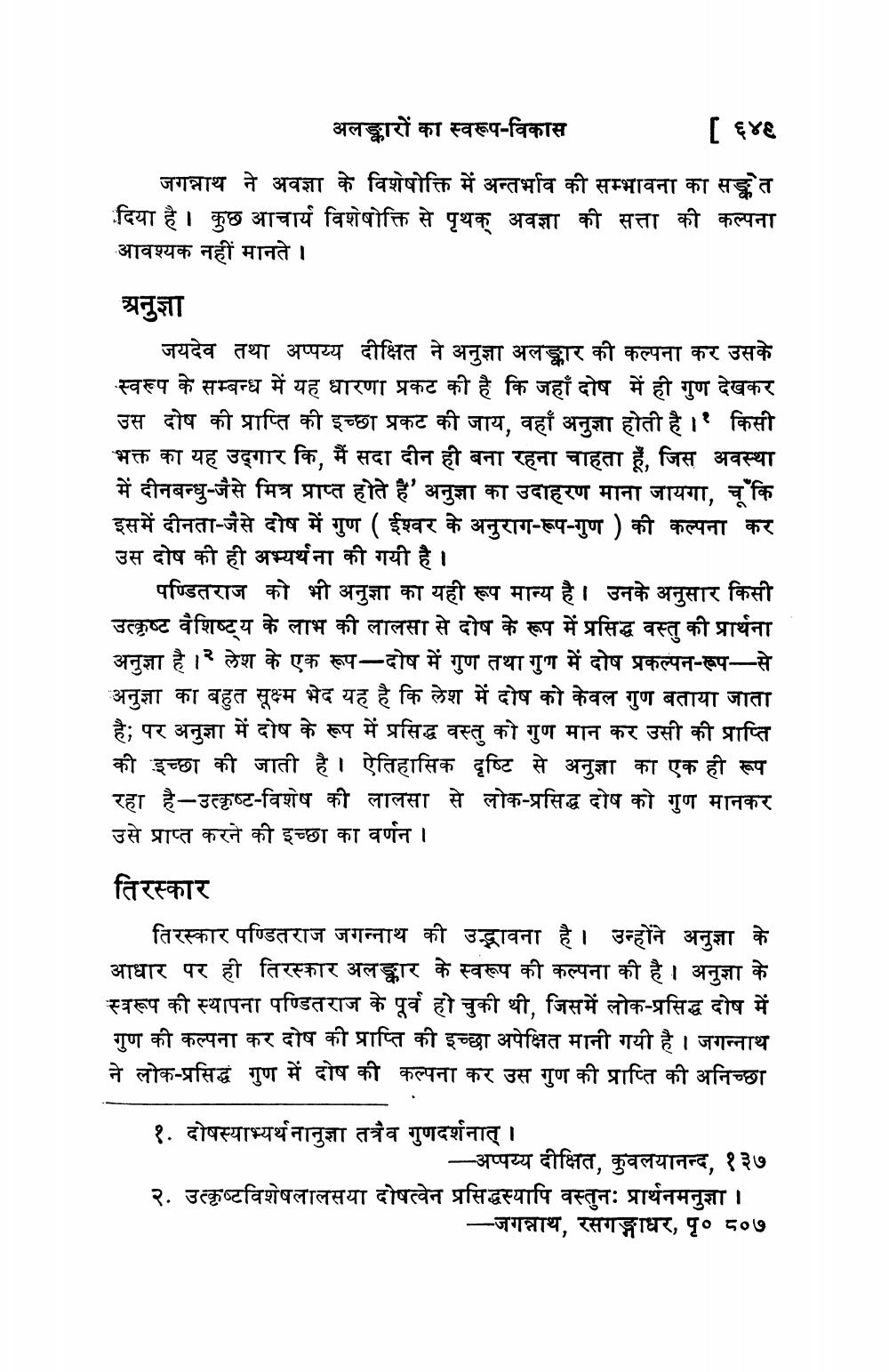________________
अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ६४६
जगन्नाथ ने अवज्ञा के विशेषोक्ति में अन्तर्भाव की सम्भावना का सङ्क ेत दिया है । कुछ आचार्य विशेषोक्ति से पृथक् अवज्ञा की सत्ता की कल्पना आवश्यक नहीं मानते ।
अनुज्ञा
जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने अनुज्ञा अलङ्कार की कल्पना कर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में यह धारणा प्रकट की है कि जहाँ दोष में ही गुण देखकर उस दोष की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की जाय, वहाँ अनुज्ञा होती है । " किसी भक्त का यह उद्गार कि, मैं सदा दीन ही बना रहना चाहता हूँ, जिस अवस्था में दीनबन्धु-जैसे मित्र प्राप्त होते हैं' अनुज्ञा का उदाहरण माना जायगा, चूँकि इसमें दीनता - जैसे दोष में गुण ( ईश्वर के अनुराग - रूप - गुण ) की कल्पना कर उस दोष की ही अभ्यर्थना की गयी है ।
पण्डितराज को भी अनुज्ञा का यही रूप मान्य है । उनके अनुसार किसी उत्कृष्ट वैशिष्ट्य के लाभ की लालसा से दोष के रूप में प्रसिद्ध वस्तु की प्रार्थना अनुज्ञा है । लेश के एक रूप - दोष में गुण तथा गुग में दोष प्रकल्पन-रूप- - से अनुज्ञा का बहुत सूक्ष्म भेद यह है कि लेश में दोष को केवल गुण बताया जाता है; पर अनुज्ञा में दोष के रूप में प्रसिद्ध वस्तु को गुण मान कर उसी की प्राप्ति की इच्छा की जाती है । ऐतिहासिक दृष्टि से अनुज्ञा का एक ही रूप रहा है - उत्कृष्ट - विशेष की लालसा से लोक-प्रसिद्ध दोष को गुण मानकर उसे प्राप्त करने की इच्छा का वर्णन ।
तिरस्कार
तिरस्कार पण्डितराज जगन्नाथ की उद्भावना है। उन्होंने अनुज्ञा के आधार पर ही तिरस्कार अलङ्कार के स्वरूप की कल्पना की है । अनुज्ञा के स्वरूप की स्थापना पण्डितराज के पूर्व हो चुकी थी, जिसमें लोक-प्रसिद्ध दोष में
गुण की कल्पना कर दोष की प्राप्ति की इच्छा अपेक्षित मानी गयी है । जगन्नाथ ने लोक - प्रसिद्ध गुण में दोष की कल्पना कर उस गुण की प्राप्ति की अनिच्छा
१. दोषस्याभ्यर्थनानुज्ञा तत्रैव गुणदर्शनात् । - अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, १३७ २. उत्कृष्टविशेषलालसया दोषत्वेन प्रसिद्धस्यापि वस्तुनः प्रार्थनमनुज्ञा । —जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ८०७