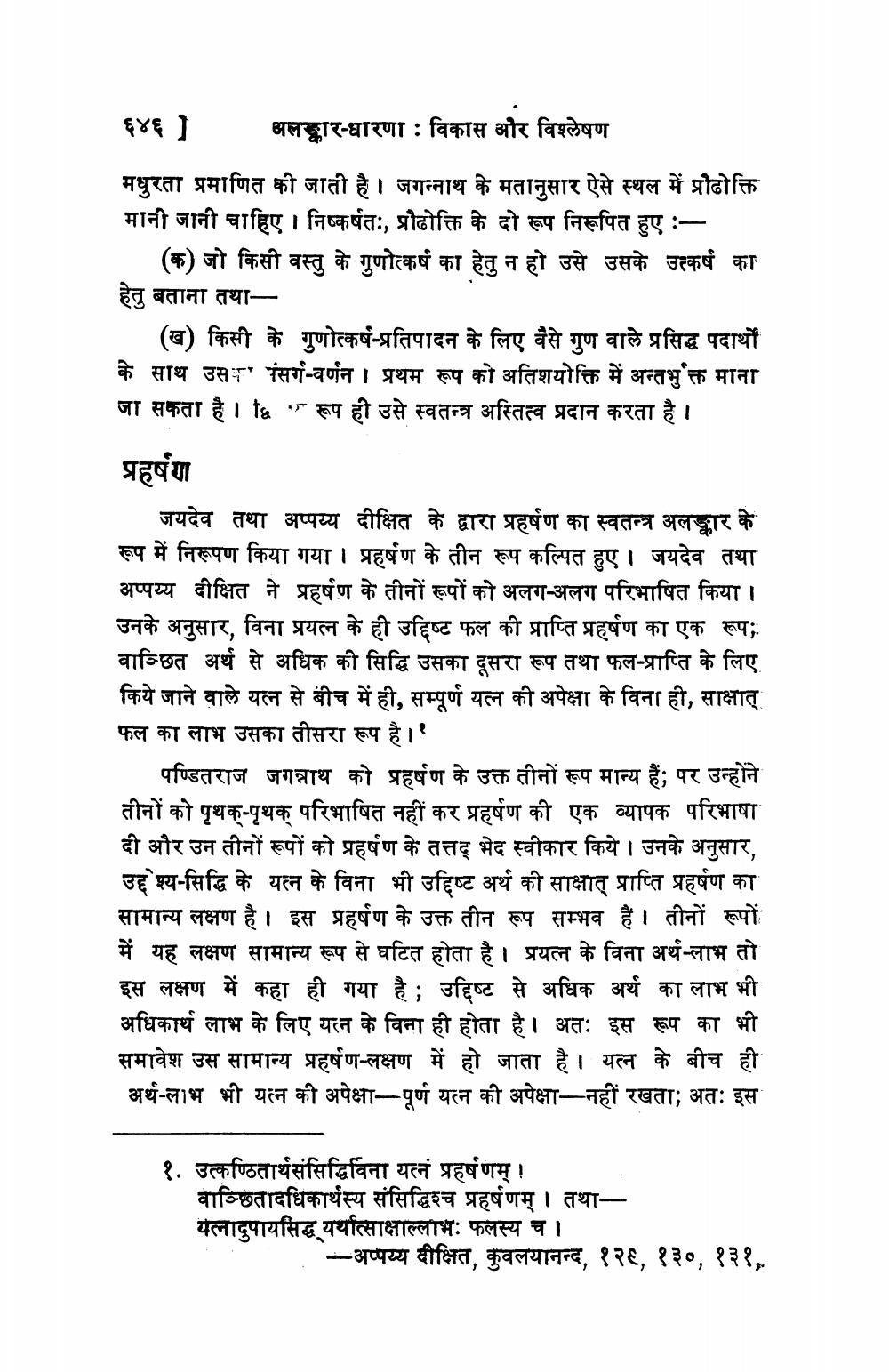________________
६४६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण मधुरता प्रमाणित की जाती है। जगन्नाथ के मतानुसार ऐसे स्थल में प्रौढोक्ति मानी जानी चाहिए । निष्कर्षतः, प्रौढोक्ति के दो रूप निरूपित हुए :
(क) जो किसी वस्तु के गुणोत्कर्ष का हेतु न हो उसे उसके उत्कर्ष का हेतु बताना तथा
(ख) किसी के गुणोत्कर्ष-प्रतिपादन के लिए वैसे गुण वाले प्रसिद्ध पदार्थों के साथ उस संसर्ग-वर्णन । प्रथम रूप को अतिशयोक्ति में अन्तभुक्त माना जा सकता है । ta ., रूप ही उसे स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करता है। प्रहर्षण
जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित के द्वारा प्रहर्षण का स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में निरूपण किया गया। प्रहर्षण के तीन रूप कल्पित हुए। जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने प्रहर्षण के तीनों रूपों को अलग-अलग परिभाषित किया। उनके अनुसार, विना प्रयत्न के ही उद्दिष्ट फल की प्राप्ति प्रहर्षण का एक रूप; वाञ्छित अर्थ से अधिक की सिद्धि उसका दूसरा रूप तथा फल-प्राप्ति के लिए किये जाने वाले यत्न से बीच में ही, सम्पूर्ण यत्न की अपेक्षा के विना ही, साक्षात् फल का लाभ उसका तीसरा रूप है।'
पण्डितराज जगन्नाथ को प्रहर्षण के उक्त तीनों रूप मान्य हैं; पर उन्होंने तीनों को पृथक्-पृथक् परिभाषित नहीं कर प्रहर्षण की एक व्यापक परिभाषा दी और उन तीनों रूपों को प्रहर्षण के तत्तद् भेद स्वीकार किये । उनके अनुसार, उद्देश्य-सिद्धि के यत्न के विना भी उद्दिष्ट अर्थ की साक्षात् प्राप्ति प्रहर्षण का सामान्य लक्षण है। इस प्रहर्षण के उक्त तीन रूप सम्भव है। तीनों रूपों में यह लक्षण सामान्य रूप से घटित होता है। प्रयत्न के विना अर्थ-लाभ तो इस लक्षण में कहा ही गया है ; उद्दिष्ट से अधिक अर्थ का लाभ भी अधिकार्थ लाभ के लिए यत्न के विना ही होता है। अतः इस रूप का भी समावेश उस सामान्य प्रहर्षण-लक्षण में हो जाता है। यत्न के बीच ही अर्थ-लाभ भी यत्न की अपेक्षा-पूर्ण यत्न की अपेक्षा नहीं रखता; अतः इस
१. उत्कण्ठितार्थसंसिद्धिविना यत्नं प्रहर्षणम् ।
वाञ्छितादधिकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम् । तथायत्नादुपायसिद्ध यर्थात्साक्षाल्लाभः फलस्य च ।
.-अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, १२६, १३०, १३१,