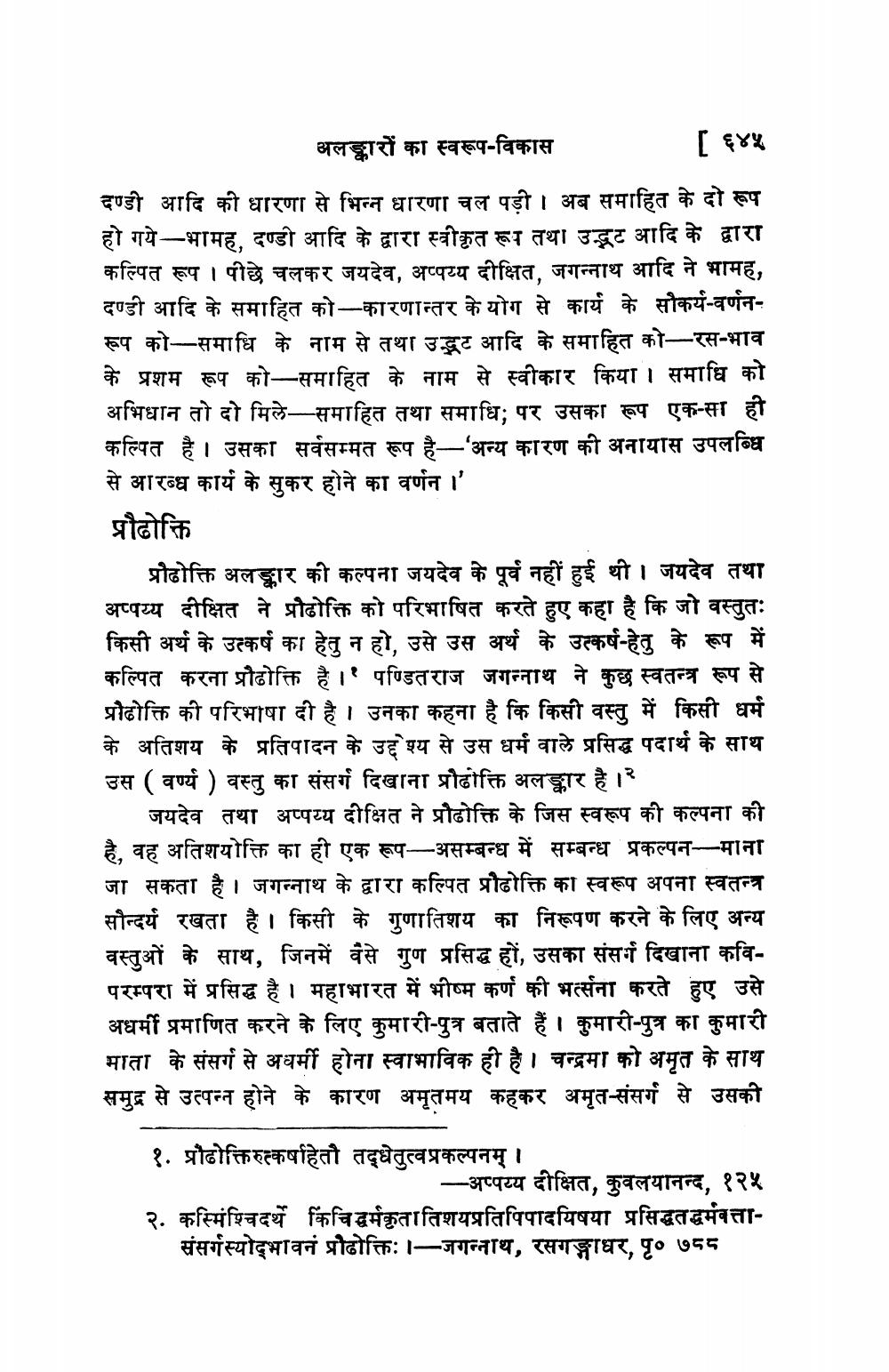________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ६४५
दण्डी आदि की धारणा से भिन्न धारणा चल पड़ी। अब समाहित के दो रूप हो गये-भामह, दण्डी आदि के द्वारा स्वीकृत रूप तथा उद्भट आदि के द्वारा कल्पित रूप । पीछे चलकर जयदेव, अप्पय्य दीक्षित, जगन्नाथ आदि ने भामह, दण्डी आदि के समाहित को-कारणान्तर के योग से कार्य के सौकर्य-वर्णनरूप को-समाधि के नाम से तथा उद्भट आदि के समाहित को-रस-भाव के प्रशम रूप को-समाहित के नाम से स्वीकार किया। समाधि को अभिधान तो दो मिले—समाहित तथा समाधि; पर उसका रूप एक-सा ही कल्पित है। उसका सर्वसम्मत रूप है—'अन्य कारण की अनायास उपलब्धि से आरब्ध कार्य के सुकर होने का वर्णन ।' प्रौढोक्ति
प्रौढोक्ति अलङ्कार की कल्पना जयदेव के पूर्व नहीं हुई थी। जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने प्रौढोक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो वस्तुतः किसी अर्थ के उत्कर्ष का हेतु न हो, उसे उस अर्थ के उत्कर्ष-हेतु के रूप में कल्पित करना प्रौढोक्ति है।' पण्डितराज जगन्नाथ ने कुछ स्वतन्त्र रूप से प्रौढोक्ति की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि किसी वस्तु में किसी धर्म के अतिशय के प्रतिपादन के उद्देश्य से उस धर्म वाले प्रसिद्ध पदार्थ के साथ उस ( वर्ण्य ) वस्तु का संसर्ग दिखाना प्रौढोक्ति अलङ्कार है।
जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने प्रौढोक्ति के जिस स्वरूप की कल्पना की है, वह अतिशयोक्ति का ही एक रूप-असम्बन्ध में सम्बन्ध प्रकल्पन-माना जा सकता है। जगन्नाथ के द्वारा कल्पित प्रौढोक्ति का स्वरूप अपना स्वतन्त्र सौन्दर्य रखता है। किसी के गुणातिशय का निरूपण करने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ, जिनमें वैसे गुण प्रसिद्ध हों, उसका संसर्ग दिखाना कविपरम्परा में प्रसिद्ध है। महाभारत में भीष्म कर्ण की भर्त्सना करते हुए उसे अधर्मी प्रमाणित करने के लिए कुमारी-पुत्र बताते हैं। कुमारी-पुत्र का कुमारी माता के संसर्ग से अधर्मी होना स्वाभाविक ही है। चन्द्रमा को अमृत के साथ समुद्र से उत्पन्न होने के कारण अमृतमय कहकर अमृत-संसर्ग से उसकी
१. प्रौढोक्तिरुत्कर्षाहेतौ तद्धेतृत्वप्रकल्पनम् ।
-अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, १२५ २. कस्मिंश्चिदर्थे किंचिद्धर्मकृतातिशयप्रतिपिपादयिषया प्रसिद्धतद्धर्मवत्ता
संसर्गस्योद्भावनं प्रौढोक्तिः।-जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ७८८