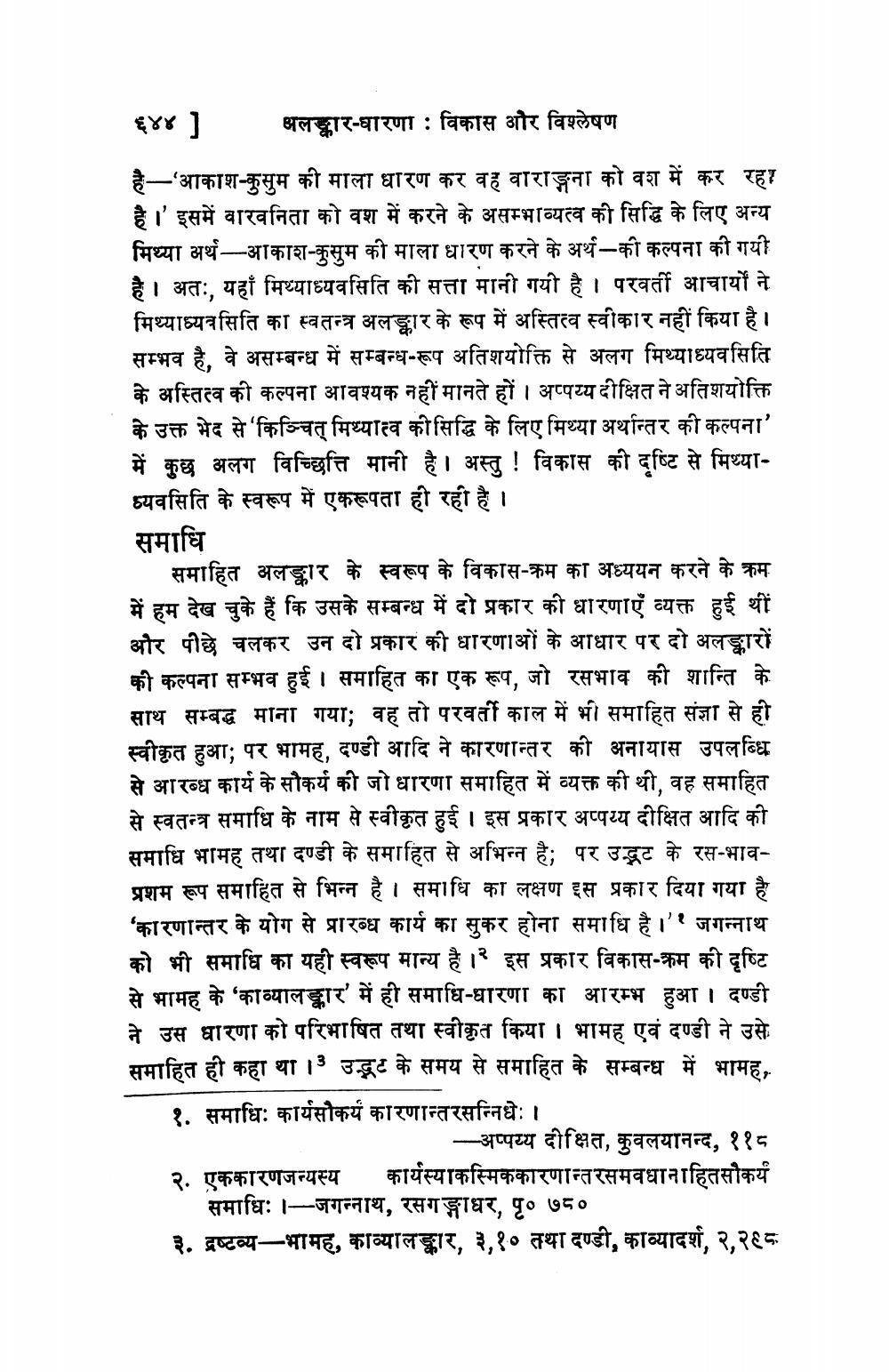________________
६४४ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
है-'आकाश-कुसुम की माला धारण कर वह वाराङ्गना को वश में कर रहा है।' इसमें वारवनिता को वश में करने के असम्भाव्यत्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्या अर्थ-आकाश-कुसुम की माला धारण करने के अर्थ-की कल्पना की गयी है। अतः, यहाँ मिथ्याध्यवसिति की सत्ता मानी गयी है। परवर्ती आचार्यों ने मिथ्याध्यवसिति का स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। सम्भव है, वे असम्बन्ध में सम्बन्ध-रूप अतिशयोक्ति से अलग मिथ्याध्यवसिति के अस्तित्व की कल्पना आवश्यक नहीं मानते हों । अप्पय्य दीक्षित ने अतिशयोक्ति के उक्त भेद से 'किञ्चित् मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए मिथ्या अर्थान्तर की कल्पना' में कुछ अलग विच्छित्ति मानी है। अस्तु ! विकास की दृष्टि से मिथ्याध्यवसिति के स्वरूप में एकरूपता ही रही है । समाधि
समाहित अलङ्कार के स्वरूप के विकास-क्रम का अध्ययन करने के क्रम में हम देख चुके हैं कि उसके सम्बन्ध में दो प्रकार की धारणाएँ व्यक्त हुई थीं और पीछे चलकर उन दो प्रकार की धारणाओं के आधार पर दो अलङ्कारों की कल्पना सम्भव हुई। समाहित का एक रूप, जो रसभाव की शान्ति के साथ सम्बद्ध माना गया; वह तो परवर्ती काल में भी समाहित संज्ञा से ही स्वीकृत हुआ; पर भामह, दण्डी आदि ने कारणान्तर की अनायास उपलब्धि से आरब्ध कार्य के सौकर्य की जो धारणा समाहित में व्यक्त की थी, वह समाहित से स्वतन्त्र समाधि के नाम से स्वीकृत हुई । इस प्रकार अप्पय्य दीक्षित आदि की समाधि भामह तथा दण्डी के समाहित से अभिन्न है; पर उद्भट के रस-भावप्रशम रूप समाहित से भिन्न है। समाधि का लक्षण इस प्रकार दिया गया है 'कारणान्तर के योग से प्रारब्ध कार्य का सुकर होना समाधि है।'' जगन्नाथ को भी समाधि का यही स्वरूप मान्य है। इस प्रकार विकास-क्रम की दृष्टि से भामह के 'काव्यालङ्कार' में ही समाधि-धारणा का आरम्भ हुआ। दण्डी ने उस धारणा को परिभाषित तथा स्वीकृत किया। भामह एवं दण्डी ने उसे समाहित ही कहा था । उद्भट के समय से समाहित के सम्बन्ध में भामह, १. समाधिः कार्यसौकर्य कारणान्तरसन्निधेः ।
-अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, ११८ २. एककारणजन्यस्य कार्यस्याकस्मिककारणान्तरसमवधानाहितसौकर्य
समाधिः । -जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ७८० ३. द्रष्टव्य-भामह, काव्यालङ्कार, ३,१० तथा दण्डी, काव्यादर्श, २,२६८