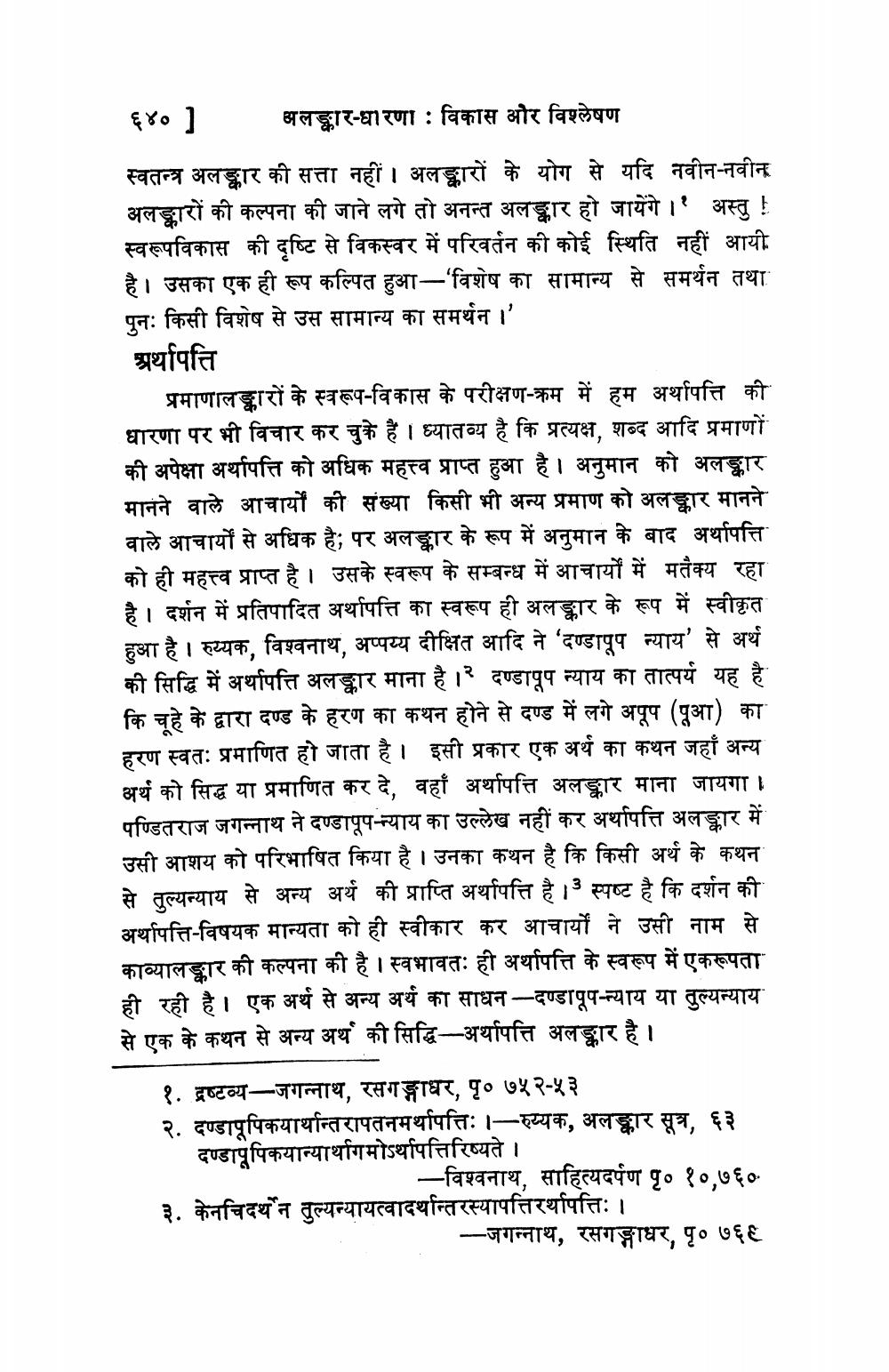________________
६४० ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
स्वतन्त्र अलङ्कार की सत्ता नहीं । अलङ्कारों के योग से यदि नवीन-नवीन अलङ्कारों की कल्पना की जाने लगे तो अनन्त अलङ्कार हो जायेंगे ।' अस्तु ! स्वरूपविकास की दृष्टि से विकस्वर में परिवर्तन की कोई स्थिति नहीं आयी. है । उसका एक ही रूप कल्पित हुआ – 'विशेष का सामान्य से समर्थन तथा पुनः किसी विशेष से उस सामान्य का समर्थन ।'
श्रर्थापत्ति
प्रमाणालङ्कारों के स्वरूप - विकास के परीक्षण क्रम में हम अर्थापत्ति की धारणा पर भी विचार कर चुके हैं। ध्यातव्य है कि प्रत्यक्ष, शब्द आदि प्रमाणों की अपेक्षा अर्थापत्ति को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है । अनुमान को अलङ्कार मानने वाले आचार्यों की संख्या किसी भी अन्य प्रमाण को अलङ्कार मानने वाले आचार्यों से अधिक है; पर अलङ्कार के रूप में अनुमान के बाद अर्थापत्ति
ही महत्त्व प्राप्त है । उसके स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्यों में मतैक्य रहा है । दर्शन में प्रतिपादित अर्थापत्ति का स्वरूप ही अलङ्कार के रूप में स्वीकृत हुआ है । रुय्यक, विश्वनाथ, अप्पय्य दीक्षित आदि ने 'दण्डापूप न्याय' से अर्थ की सिद्धि में अर्थापत्ति अलङ्कार माना है । २ दण्डापूप न्याय का तात्पर्य यह है कि चूहे के द्वारा दण्ड के हरण का कथन होने से दण्ड में लगे अपूप ( आ ) का हरण स्वतः प्रमाणित हो जाता है । इसी प्रकार एक अर्थ का कथन जहाँ अन्य अर्थ को सिद्ध या प्रमाणित कर दे, वहाँ अर्थापत्ति अलङ्कार माना जायगा । में पण्डितराज जगन्नाथ ने दण्डापूप- न्याय का उल्लेख नहीं कर अर्थापत्ति अलङ्कार उसी आशय को परिभाषित किया है। उनका कथन है कि किसी अर्थ के कथन से तुल्यन्याय से अन्य अर्थ की प्राप्ति अर्थापत्ति है । 3 स्पष्ट है कि दर्शन की अर्थापत्ति-विषयक मान्यता को ही स्वीकार कर आचार्यों ने उसी नाम से काव्यालङ्कार की कल्पना की है । स्वभावतः ही अर्थापत्ति के स्वरूप में एकरूपता ही रही है । एक अर्थ से अन्य अर्थ का साधन - दण्डापूपन्याय या तुल्यन्याय से एक के कथन से अन्य अर्थ की सिद्धि - अर्थापत्ति अलङ्कार है ।
१. द्रष्टव्य — जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ७५२-५३
२. दण्डापूपिकयार्थान्तरापतनमर्थापत्तिः । - रुय्यक, अलङ्कार सूत्र, ६३ दण्डापूपिकयान्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते ।
- विश्वनाथ, साहित्यदर्पण पृ० १०,७६०३. केनचिदर्थेन तुल्यन्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिः ।
—जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ७६६