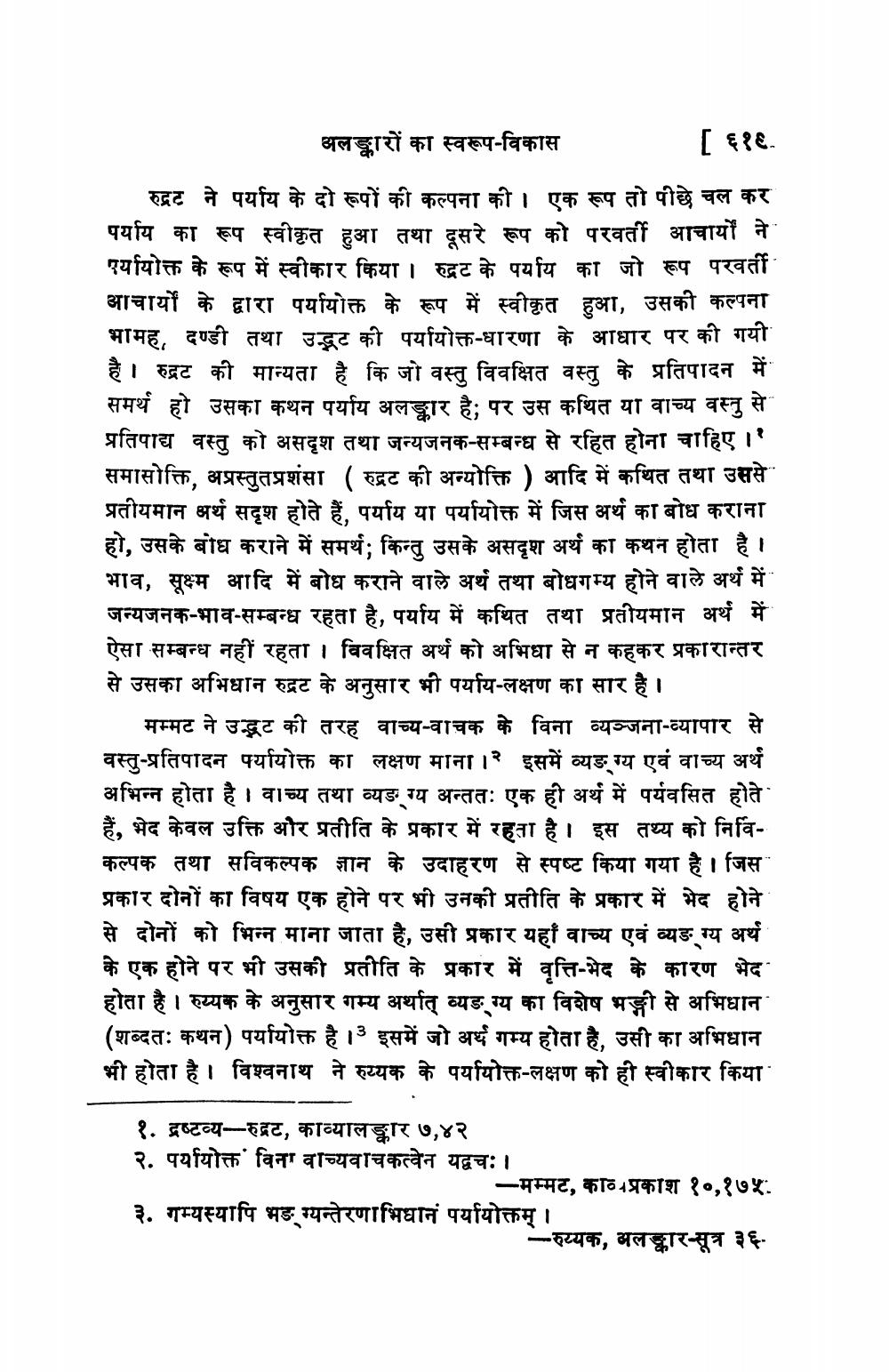________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ६१६.
रुद्रट ने पर्याय के दो रूपों की कल्पना की। एक रूप तो पीछे चल कर पर्याय का रूप स्वीकृत हुआ तथा दूसरे रूप को परवर्ती आचार्यों ने एर्यायोक्त के रूप में स्वीकार किया। रुद्रट के पर्याय का जो रूप परवर्ती आचार्यों के द्वारा पर्यायोक्त के रूप में स्वीकृत हुआ, उसकी कल्पना भामह, दण्डी तथा उद्भट की पर्यायोक्त-धारणा के आधार पर की गयी है। रुद्रट की मान्यता है कि जो वस्तु विवक्षित वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ हो उसका कथन पर्याय अलङ्कार है; पर उस कथित या वाच्य वस्तु से प्रतिपाद्य वस्तु को असदृश तथा जन्यजनक-सम्बन्ध से रहित होना चाहिए।' समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा ( रुद्रट की अन्योक्ति ) आदि में कथित तथा उससे प्रतीयमान अर्थ सदृश होते हैं, पर्याय या पर्यायोक्त में जिस अर्थ का बोध कराना हो, उसके बोध कराने में समर्थ; किन्तु उसके असदृश अर्थ का कथन होता है। भाव, सूक्ष्म आदि में बोध कराने वाले अर्थ तथा बोधगम्य होने वाले अर्थ में जन्यजनक-भाव-सम्बन्ध रहता है, पर्याय में कथित तथा प्रतीयमान अर्थ में ऐसा सम्बन्ध नहीं रहता। विवक्षित अर्थ को अभिधा से न कहकर प्रकारान्तर से उसका अभिधान रुद्रट के अनुसार भी पर्याय-लक्षण का सार है।
मम्मट ने उद्भट की तरह वाच्य-वाचक के विना व्यञ्जना-व्यापार से वस्तु-प्रतिपादन पर्यायोक्त का लक्षण माना।२ इसमें व्यङ्ग्य एवं वाच्य अर्थ अभिन्न होता है । वाच्य तथा व्यङग्य अन्ततः एक ही अर्थ में पर्यवसित होते हैं, भेद केवल उक्ति और प्रतीति के प्रकार में रहता है। इस तथ्य को निर्विकल्पक तथा सविकल्पक ज्ञान के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है । जिस प्रकार दोनों का विषय एक होने पर भी उनकी प्रतीति के प्रकार में भेद होने से दोनों को भिन्न माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ वाच्य एवं व्यङग्य अर्थ के एक होने पर भी उसकी प्रतीति के प्रकार में वृत्ति-भेद के कारण भेद होता है । रुय्यक के अनुसार गम्य अर्थात् व्यङग्य का विशेष भङ्गी से अभिधान (शब्दतः कथन) पर्यायोक्त है। इसमें जो अर्थ गम्य होता है, उसी का अभिधान भी होता है। विश्वनाथ ने रुय्यक के पर्यायोक्त-लक्षण को ही स्वीकार किया
१. द्रष्टव्य-रुद्रट, काव्यालङ्कार ७,४२ २. पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः ।
-मम्मट, काव्यप्रकाश १०,१७५. ३. गम्यस्यापि भङ ग्यन्तेरणाभिधानं पर्यायोक्तम् ।
-रुय्यक, अलङ्कार-सूत्र ३६.