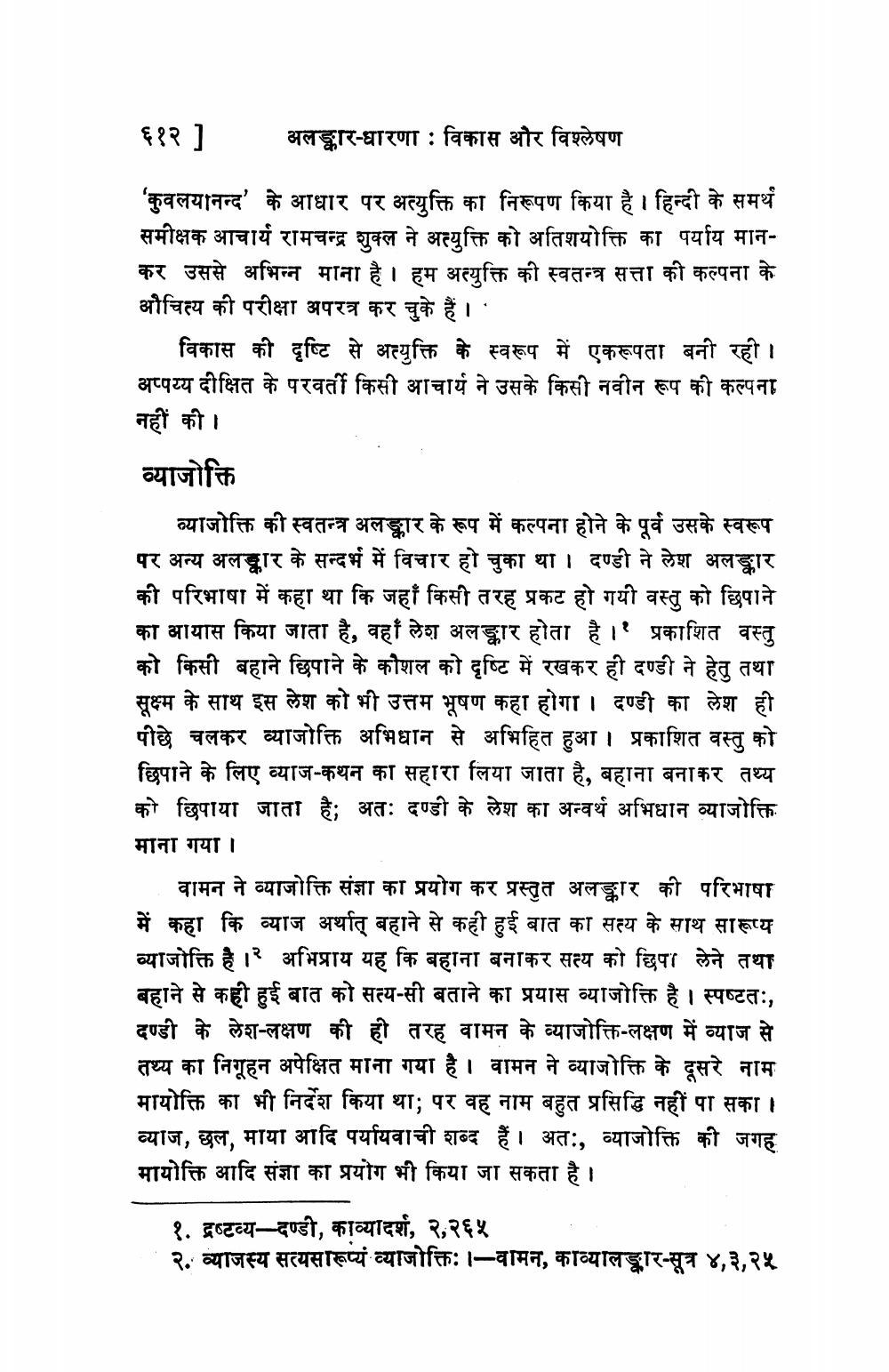________________
६१२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
'कुवलयानन्द' के आधार पर अत्युक्ति का निरूपण किया है। हिन्दी के समर्थ समीक्षक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अत्युक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानकर उससे अभिन्न माना है। हम अत्युक्ति की स्वतन्त्र सत्ता की कल्पना के औचित्य की परीक्षा अपरत्र कर चुके हैं।
विकास की दृष्टि से अत्युक्ति के स्वरूप में एकरूपता बनी रही। अप्पय्य दीक्षित के परवर्ती किसी आचार्य ने उसके किसी नवीन रूप की कल्पना नहीं की। व्याजोक्ति
व्याजोक्ति की स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में कल्पना होने के पूर्व उसके स्वरूप पर अन्य अलङ्कार के सन्दर्भ में विचार हो चुका था। दण्डी ने लेश अलङ्कार की परिभाषा में कहा था कि जहाँ किसी तरह प्रकट हो गयी वस्तु को छिपाने का आयास किया जाता है, वहाँ लेश अलङ्कार होता है।' प्रकाशित वस्तु को किसी बहाने छिपाने के कौशल को दृष्टि में रखकर ही दण्डी ने हेतु तथा सूक्ष्म के साथ इस लेश को भी उत्तम भूषण कहा होगा। दण्डी का लेश ही पीछे चलकर व्याजोक्ति अभिधान से अभिहित हुआ। प्रकाशित वस्तु को छिपाने के लिए व्याज-कथन का सहारा लिया जाता है, बहाना बनाकर तथ्य को छिपाया जाता है; अतः दण्डी के लेश का अन्वर्थ अभिधान व्याजोक्ति माना गया। ____ वामन ने व्याजोक्ति संज्ञा का प्रयोग कर प्रस्तुत अलङ्कार की परिभाषा में कहा कि व्याज अर्थात् बहाने से कही हुई बात का सत्य के साथ सारूप्य व्याजोक्ति है ।२ अभिप्राय यह कि बहाना बनाकर सत्य को छिपा लेने तथा बहाने से कही हुई बात को सत्य-सी बताने का प्रयास व्याजोक्ति है। स्पष्टतः, दण्डी के लेश-लक्षण की ही तरह वामन के व्याजोक्ति-लक्षण में व्याज से तथ्य का निगहन अपेक्षित माना गया है। वामन ने व्याजोक्ति के दूसरे नाम मायोक्ति का भी निर्देश किया था; पर वह नाम बहुत प्रसिद्धि नहीं पा सका। व्याज, छल, माया आदि पर्यायवाची शब्द हैं। अत:, व्याजोक्ति की जगह मायोक्ति आदि संज्ञा का प्रयोग भी किया जा सकता है।
१. द्रष्टव्य-दण्डी, काव्यादर्श, २,२६५ २. व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्तिः।-वामन, काव्यालङ्कार-सूत्र ४,३,२५