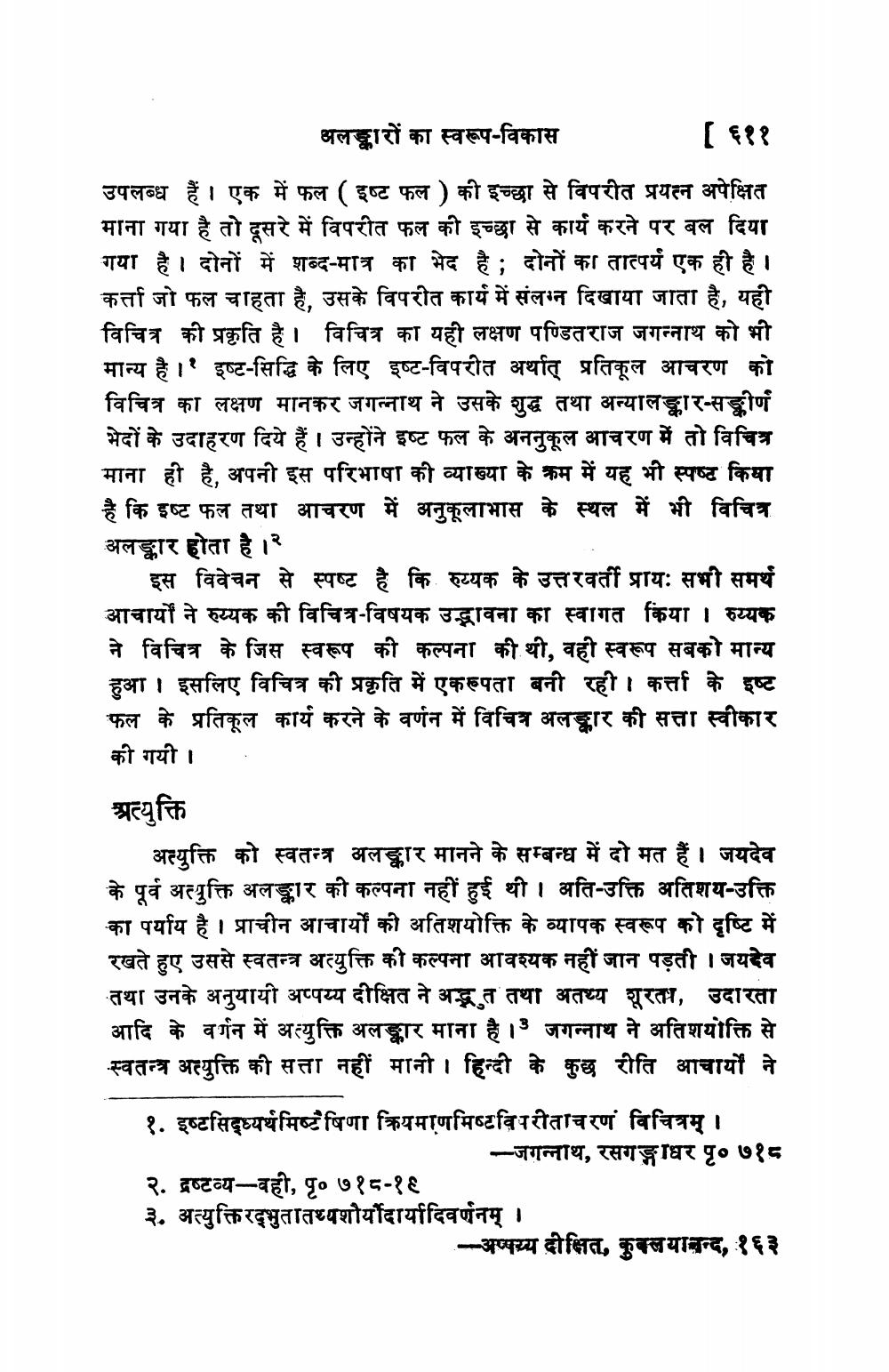________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[६११
उपलब्ध हैं। एक में फल ( इष्ट फल ) की इच्छा से विपरीत प्रयत्न अपेक्षित माना गया है तो दूसरे में विपरीत फल की इच्छा से कार्य करने पर बल दिया गया है। दोनों में शब्द-मात्र का भेद है; दोनों का तात्पर्य एक ही है। कर्ता जो फल चाहता है, उसके विपरीत कार्य में संलग्न दिखाया जाता है, यही विचित्र की प्रकृति है। विचित्र का यही लक्षण पण्डितराज जगन्नाथ को भी मान्य है।' इष्ट-सिद्धि के लिए इष्ट-विपरीत अर्थात् प्रतिकूल आचरण को विचित्र का लक्षण मानकर जगन्नाथ ने उसके शुद्ध तथा अन्यालङ्कार-सङ्कीर्ण भेदों के उदाहरण दिये हैं। उन्होंने इष्ट फल के अननुकूल आचरण में तो विचित्र माना ही है, अपनी इस परिभाषा की व्याख्या के क्रम में यह भी स्पष्ट किया है कि इष्ट फल तथा आचरण में अनुकूलाभास के स्थल में भी विचित्र अलङ्कार होता है।
इस विवेचन से स्पष्ट है कि रुय्यक के उत्तरवर्ती प्रायः सभी समर्थ आचार्यों ने रुय्यक की विचित्र-विषयक उद्भावना का स्वागत किया । रुय्यक ने विचित्र के जिस स्वरूप की कल्पना की थी, वही स्वरूप सबको मान्य हुआ। इसलिए विचित्र की प्रकृति में एकरूपता बनी रही। कर्ता के इष्ट फल के प्रतिकूल कार्य करने के वर्णन में विचित्र अलङ्कार की सत्ता स्वीकार की गयी। अत्युक्ति
अत्युक्ति को स्वतन्त्र अलङ्कार मानने के सम्बन्ध में दो मत हैं। जयदेव के पूर्व अत्युक्ति अलङ्कार की कल्पना नहीं हुई थी। अति-उक्ति अतिशय-उक्ति का पर्याय है । प्राचीन आचार्यों की अतिशयोक्ति के व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए उससे स्वतन्त्र अत्युक्ति की कल्पना आवश्यक नहीं जान पड़ती । जयदेव तथा उनके अनुयायी अप्पय्य दीक्षित ने अद्भत तथा अतथ्य शूरता, उदारता आदि के वर्गन में अत्युक्ति अलङ्कार माना है। जगन्नाथ ने अतिशयोक्ति से स्वतन्त्र अत्युक्ति की सत्ता नहीं मानी। हिन्दी के कुछ रीति आचार्यों ने १. इष्टसिद्ध्यर्थमिष्टषिणा क्रियमाणमिष्टविपरीताचरणं विचित्रम् ।
-जगन्नाथ, रसगङ्गाधर पृ०७१८ २. द्रष्टव्य-वही, पृ० ७१८-१९ ३. अत्युक्तिरद्भुतातथ्यशौर्यौदार्यादिवर्णनम् ।
-अप्पय्य दीक्षित, कुवलयानन्द, १६३