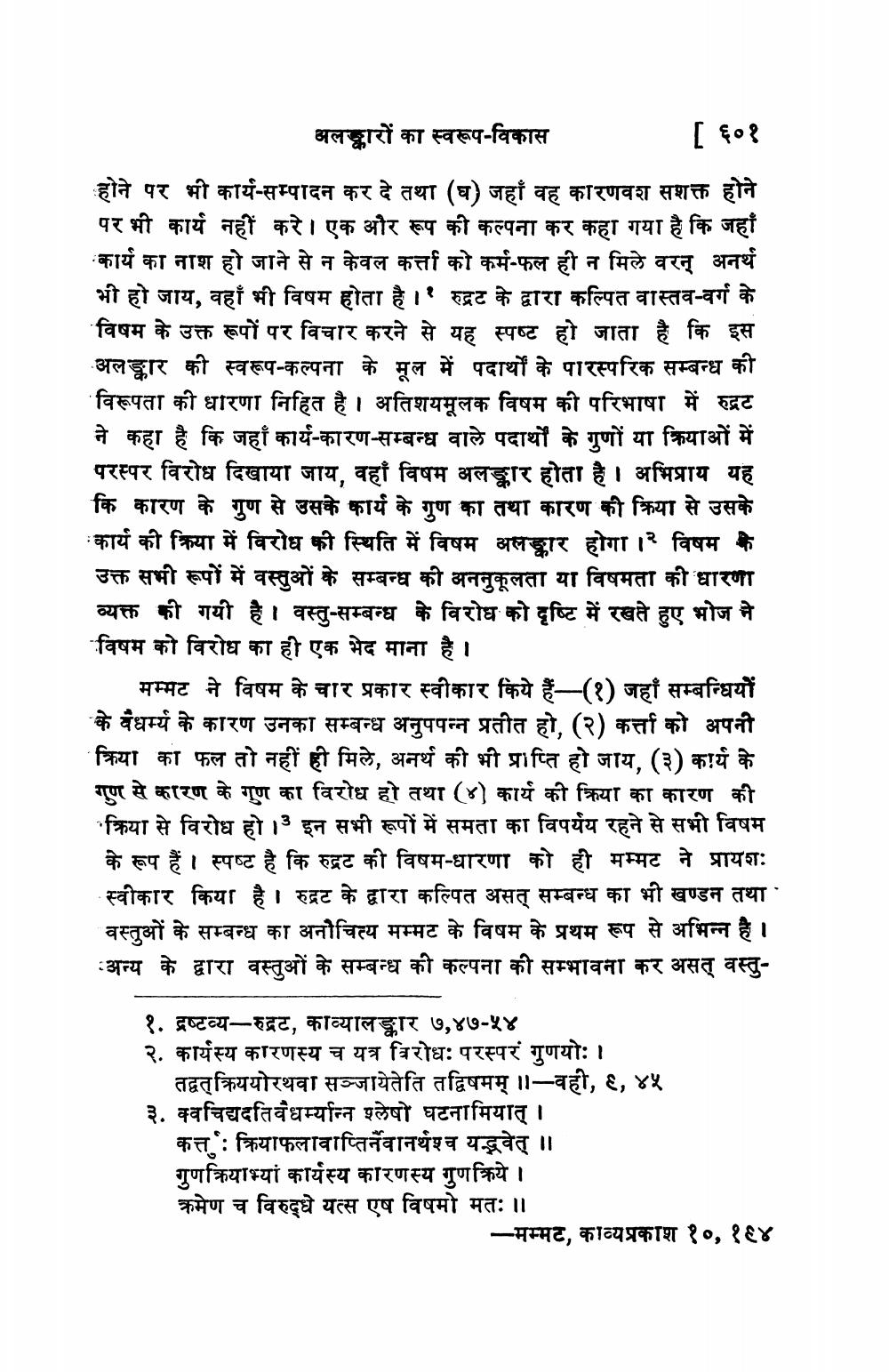________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ६०१ होने पर भी कार्य सम्पादन कर दे तथा (घ) जहाँ वह कारणवश सशक्त होने पर भी कार्य नहीं करे। एक और रूप की कल्पना कर कहा गया है कि जहाँ कार्य का नाश हो जाने से न केवल कर्त्ता को कर्म-फल ही न मिले वरन् अनर्थ भी हो जाय, वहाँ भी विषम होता है । रुद्रट के द्वारा कल्पित वास्तव-वर्ग के विषम के उक्त रूपों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अलङ्कार की स्वरूप - कल्पना के मूल में पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध की विरूपता की धारणा निहित है । अतिशयमूलक विषम की परिभाषा में रुद्रट ने कहा है कि जहाँ कार्य-कारण-सम्बन्ध वाले पदार्थों के गुणों या क्रियाओं में परस्पर विरोध दिखाया जाय, वहाँ विषम अलङ्कार होता है । अभिप्राय यह कि कारण के गुण से उसके कार्य के गुण का तथा कारण की क्रिया से उसके कार्य की क्रिया में विरोध की स्थिति में विषम अलङ्कार होगा । विषम के उक्त सभी रूपों में वस्तुओं के सम्बन्ध की अननुकूलता या विषमता की धारणा व्यक्त की गयी है । वस्तु सम्बन्ध के विरोध को दृष्टि में रखते हुए भोज ने विषम को विरोध का ही एक भेद माना है ।
मम्मट ने विषम के चार प्रकार स्वीकार किये हैं- (१) जहाँ सम्बन्धियों के वैधर्म्य के कारण उनका सम्बन्ध अनुपपन्न प्रतीत हो, (२) कर्त्ता को अपनी क्रिया का फल तो नहीं ही मिले, अनर्थ की भी प्राप्ति हो जाय, (३) कार्य के गुण से कारण के गुण का विरोध हो तथा (४) कार्य की क्रिया का कारण की "क्रिया से विरोध हो । 3 इन सभी रूपों में समता का विपर्यय रहने से सभी विषम के रूप हैं । स्पष्ट है कि रुद्रट की विषम-धारणा को ही मम्मट ने प्रायशः स्वीकार किया है । रुद्रट के द्वारा कल्पित असत् सम्बन्ध का भी खण्डन तथा वस्तुओं के सम्बन्ध का अनौचित्य मम्मट के विषम के प्रथम रूप से अभिन्न है । - अन्य के द्वारा वस्तुओं के सम्बन्ध की कल्पना की सम्भावना कर असत् वस्तु
१. द्रष्टव्य - रुद्रट, काव्यालङ्कार ७, ४७-५४
२. कार्यस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्परं गुणयोः ।
तद्वत्क्रिययोरथवा सञ्जायेतेति तद्विषमम् ॥ - वही, ६, ४५
३. क्वचिद्यदति वैधर्म्यान्न श्लेषो घटनामियात् । कत्त: क्रियाफलावाप्तिर्नैवानर्थश्च यद्भवेत् ॥ गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये क्रमेण च विरुद्धे यत्स एष विषमो मतः ॥
- मम्मट, काव्यप्रकाश १०, १९४