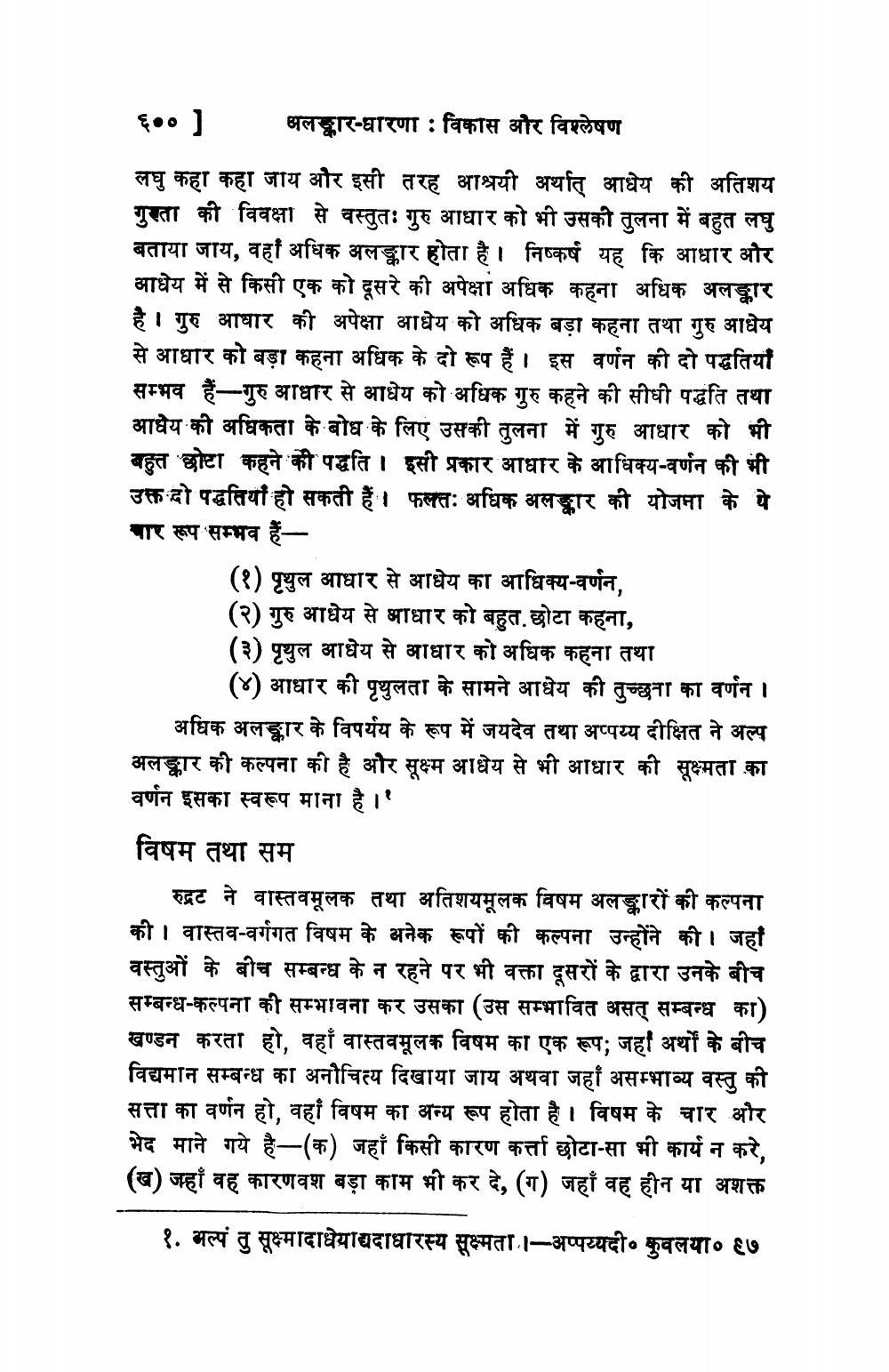________________
६..]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
लघु कहा कहा जाय और इसी तरह आश्रयी अर्थात् आधेय की अतिशय गुरुता की विवक्षा से वस्तुतः गुरु आधार को भी उसकी तुलना में बहुत लघु बताया जाय, वहाँ अधिक अलङ्कार होता है। निष्कर्ष यह कि आधार और आधेय में से किसी एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक कहना अधिक अलङ्कार है। गुरु आधार की अपेक्षा आधेय को अधिक बड़ा कहना तथा गुरु आधेय से आधार को बड़ा कहना अधिक के दो रूप हैं। इस वर्णन की दो पद्धतियां सम्भव हैं-गुरु आधार से आधेय को अधिक गुरु कहने की सीधी पद्धति तथा आधेय की अधिकता के बोध के लिए उसकी तुलना में गुरु आधार को भी बहुत छोटा कहने की पद्धति । इसी प्रकार आधार के आधिक्य-वर्णन की भी उक्त दो पद्धतियां हो सकती हैं। फलतः अधिक अलङ्कार की योजना के ये चार रूप सम्भव हैं
(१) पृथुल आधार से आधेय का आधिक्य-वर्णन, (२) गुरु आधेय से आधार को बहुत.छोटा कहना, (३) पृथुल आधेय से आधार को अधिक कहना तथा
(४) आधार की पृथुलता के सामने आधेय की तुच्छता का वर्णन । अधिक अलङ्कार के विपर्यय के रूप में जयदेव तथा अप्पय्य दीक्षित ने अल्प अलङ्कार की कल्पना की है और सूक्ष्म आधेय से भी आधार की सूक्ष्मता का वर्णन इसका स्वरूप माना है।' विषम तथा सम ___ रुद्रट ने वास्तवमूलक तथा अतिशयमूलक विषम अलङ्कारों की कल्पना की। वास्तव-वर्गगत विषम के अनेक रूपों की कल्पना उन्होंने की। जहाँ वस्तुओं के बीच सम्बन्ध के न रहने पर भी वक्ता दूसरों के द्वारा उनके बीच सम्बन्ध-कल्पना की सम्भावना कर उसका (उस सम्भावित असत् सम्बन्ध का) खण्डन करता हो, वहाँ वास्तवमूलक विषम का एक रूप; जहाँ अर्थों के बीच विद्यमान सम्बन्ध का अनौचित्य दिखाया जाय अथवा जहाँ असम्भाव्य वस्तु की सत्ता का वर्णन हो, वहां विषम का अन्य रूप होता है। विषम के चार और भेद माने गये है-(क) जहाँ किसी कारण कर्ता छोटा-सा भी कार्य न करे, (ख) जहाँ वह कारणवश बड़ा काम भी कर दे, (ग) जहाँ वह हीन या अशक्त
१. भल्पं तु सूक्ष्मादाधेयाद्यदाधारस्य सूक्ष्मता।-अप्पय्यदी• कुवलया० ६७